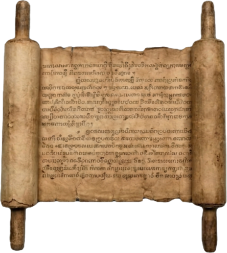
स्मृतिप्रस्थान
सूत्र परिचय
यह सूत्र दीघनिकाय २२ के समान ही है; दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी, इसे दीर्घ के साथ-साथ मध्यम निकाय में भी सम्मिलित क्यों किया गया, इसका निश्चित कारण हमें ज्ञात नहीं है। संभव है कि, चूँकि मध्यम निकाय मुख्यतः साधना-संबंधी सूत्रों का संग्रह है, इसलिए इसकी यहाँ उपस्थिति को भी आवश्यक समझा गया हो।
बहरहाल, यह सूत्र साधना करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। भगवान ने स्वयं (मज्झिमनिकाय १२ में) कहा हैं कि स्मृतिप्रस्थान की साधना इतनी व्यापक और गहरी है कि यदि वे उसे लगातार सौ वर्षों तक बिना रुके बताते रहे, तब भी उसका विवरण खत्म नहीं होगा। चलिए, जानते हैं कि ये ‘सति’ या ‘स्मृति’ क्या है?
आजकल लोग ‘सति’ का अर्थ तरह-तरह से निकालते हैं। कुछ लोग इसे “निष्क्रिय जागरूकता” समझते हैं, अर्थात जो कुछ भी हो रहा है, उसे होने दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस जागरूक बने देखते रहो। लेकिन भगवान ने सति को निष्क्रियता से नहीं, बल्कि सक्रियता से जोड़ा है, और जागरूकता को स्मृति के साथ।
भगवान की दी गयी उपमा बड़ी सरल और लाजवाब है—
“जैसे किसी राजसी गढ़ पर भीतरी प्रजा की रक्षा के लिए, और बाहरी शक्तियों को दूर रखने के लिए एक चतुर, समर्थ और होशियार द्वारपाल होता है, जो संदेहास्पद लोगों को बाहर रखता है, और परिचित भले लोगों को भीतर प्रवेश देता है। उसी तरह, कोई स्मृतिमान होता है, याददाश्त में बहुत तेज़! पूर्वकाल में किया गया कर्म, पूर्वकाल में कहा गया वचन भी स्मरण रखता है, और अनुस्मरण कर पाता है।
और, तब वह लोक के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाकर—
- काया को काया देखते हुए रहता है
- वेदना को वेदना देखते हुए रहता है
- चित्त को चित्त देखते हुए रहता है
- स्वभाव को स्वभाव देखते हुए रहता है
—तत्पर, सचेत और स्मृतिमान।
तब, ऐसी द्वारपाल-रूपी स्मृति स्थापित कर, कोई अकुशल का त्याग करता है, और कुशलता को बढ़ाता है, पाप का त्याग करता है, और निष्पापता को बढ़ाता है। और, स्वयं का परिशुद्धतापूर्वक ख्याल रखता है। इस तरह, कोई स्मृतिसंपन्न रहता है।”
—अंगुत्तरनिकाय ७:६३
इस तरह, भगवान ने सति का वर्णन द्वारपाल की स्मृति के साथ जोड़कर किया है। यह सति कोई निष्क्रिय और मौन रहने वाले मॉल के द्वारपाल जैसी नहीं है, जो किसी पुतले की तरह लोगों को आते-जाते हुए देखकर, बिना किसी उद्देश्य के मुस्कुराता हुआ, बस खड़े रहने का वेतन लेता है।
इसके बजाय, यह सति उस चतुर, सक्षम और होशियार सैनिक की तरह है, जो राजसी क़िले के सबसे महत्वपूर्ण द्वार पर तैनात होता है। आजकल की भाषा में कहें, तो देश की सीमा-द्वार पर तैनात फौजी। वह जानता है कि उसकी एक भी गलती, एक भी चूक, उस क़िले या देश को संकट में डाल सकती है। इसलिए वह अपने द्वार-स्थल पर अत्यधिक चौकस और सक्रिय रहता है, बड़ी सतर्कता से आने-जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेता है, उनकी बारीक हरकतों और सूक्ष्म हाव-भावों का निरीक्षण करता है। और वह सुनिश्चित करता है कि केवल विश्वसनीय लोग ही भीतर प्रवेश कर सकें, जबकि संदेहास्पद या आतंकवादी को वह प्रवेश करने से रोकता है।
ठीक उसी तरह, सति की साधना करता हुआ कोई, बहुत ही सचेत, तत्पर और “याददाश्त में तेज़” बने रहता है। वह केवल अच्छे और कुशल गुणों को ही भीतर आने की अनुमति देता है, जबकि अकुशल या नकारात्मक गुणों को बाहर ही रोक देता है। लेकिन सचेत (“सम्पजञ्ञ”) होना वाकई क्या है? भगवान अन्य सूत्र में निर्देश देते हैं—
“कोई साधक ‘सचेत’ कैसे होता है?
- उसे वेदना (=अनुभूति) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।
- उसे विचारों (“वितक्क”) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।
- उसे संज्ञा (=नजरिया) का उत्पन्न होना, स्थित होना, और व्यय होना पता चलता हैं।
—इस तरह, कोई साधक सचेत होता है।”
—संयुत्तनिकाय ४७:३५
इस तरह, सचेत या जागरूक होने का अर्थ है—अपनी वेदना, विचारों और संज्ञाओं को तीन चरणों में जानना—उनके उत्पन्न होते हुए, कुछ समय तक टिके रहते, और फिर लुप्त होते हुए। इन ‘उदय-ठहराव-व्यय’ की निरंतर सजगता साधक को ‘अनित्य, दुःख और अनात्म’ के प्रत्यक्ष दर्शन तक ले जाती है।
साथ ही, सति का आतापी से जुड़ा रहना अनिवार्य है। “आतापी” का अर्थ, दरअसल, आर्य अष्टांगिक मार्ग के छठे-अंग “सम्यक प्रयास” से संबंधित है। एक ऐसी भावना, जो बिना रुके और बिना थके, सद्गुणों के संरक्षण और अवगुणों की रोकथाम में लगी रहती है—
“और, कोई आतापी [=तत्पर, चुस्त, मुस्तैद, वीर्यवान, परिश्रमी, मेहनती] कैसे होता है? कोई सोचता है—
- ‘यदि अनुत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव उत्पन्न होंगे, तो अनर्थ होगा’
- ‘यदि उत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव त्यागे न गए, तो अनर्थ होगा’
- ‘यदि अनुत्पन्न कुशल स्वभाव उत्पन्न न हुए, तो अनर्थ होगा’
- ‘यदि उत्पन्न कुशल स्वभाव खत्म हुए, तो अनर्थ होगा’
—और तब, वह तत्परता जगाता है।
इस तरह कोई “आतापी” होता है।”
—संयुत्तनिकाय १६:२
कल्पना करें कि किसी साधक के भीतर कोई पाप या अकुशल स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उसे होने देना चाहिए? भगवान के अनुसार, बिलकुल नहीं! हमें स्मृति की साधना इधर-उधर भटकते हुए दिशाहीन रूप से नहीं करनी हैं। बल्कि, हमें एक निर्धारित लक्ष्य के साथ, एक विशिष्ट मार्ग को चुनकर उसी दिशा में आगे बढ़ना हैं। यही मार्ग हमें अन्तर्ज्ञान की उस परिज्ञा या अंतिम-सीमा तक ले जाएगा, जहाँ सभी तरह के दुःख हमेशा के लिए पीछे छुट जाते हैं।
जैसे हमें धम्मानुपस्सना, अर्थात, “स्वभाव को स्वभाव देखने की साधना” में यह जानना हैं कि हमारे भीतर कोई विकार (नीवरण) तो नहीं है। फिर, अगले चरण में हमें यह समझना हैं कि वह विकार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। पाली के शब्दों में “उदय” और “समुदय” में महत्वपूर्ण अंतर है। उदय का अर्थ है, किसी बात का केवल प्रकट होना। जबकि समुदय का अर्थ है, किसी बात का “किसी अन्य के प्रभाव या कारण से” प्रकट होना। इसलिए, मैंने इसे “उत्पत्ति-स्वभाव” के रूप में अनुवादित किया है, जो यह दर्शाता है कि कोई स्वभाव आपोआप यूँ ही “उदय” नहीं होता, बल्कि उसका किसी कारण या प्रभाव से “समुदय” होता है। इस प्रकार, हमें उन स्वभावों की उत्पत्ति और व्यय के कारण का पता लगाकर, उन पर नियंत्रित रूप से कार्य करना हैं।
उदाहरण के तौर पर, हमें यह समझना है कि किसी बात की उत्पत्ति या शुरुआत कैसे और किसके साथ हुई। मसलन, किसी नीवरण के जागने से ठीक पहले क्या हुआ था? कौन-से इंद्रिय पर क्या घटना घटित हुई? वेदना क्या हुई? चित्त कैसे बदला? मन में क्या विचार आया? संज्ञा कैसे बदला? और अंततः, उसी क्षण में वह नीवरण उत्पन्न हुआ। अर्थात, यह इदप्पच्चयता [=कारण-कार्य भाव] और पटिच्च समुप्पाद [अर्थात, किसी बात का आधार लेकर उसके साथ सह-उत्पन्न होना] की ओर इशारा करता है। इस तरह, सतिपट्ठान के अगले चरण में धम्म के गहरे सिद्धान्त शामिल होते हैं—
- जब यह है, तब वह है।
- इसके उत्पन्न होने से, वह उत्पन्न होने लगता है।
- जब यह नहीं है, तब वह भी नहीं है।
- इसके अन्त होने से, उसका भी अन्त होने लगता है।
—अंगुत्तरनिकाय १०:९२ : वेर सुत्त
दूसरी ओर, हमें हर स्वभाव के बारे में बिलकुल अलग-अलग जानकारी प्राप्त करनी है। उदाहरण के लिए, हमें एक स्वभाव (नीवरण) के बारे में यह समझना है कि उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे रोकी जा सकती है। दूसरे स्वभाव (संबोधि-अंग) के बारे में यह जानना है कि वह कैसे विकसित होकर परिपक्व हो सकता है। तीसरे स्वभाव (आयतन) के बारे में, हमें उसके बंधन (संयोजन) को समझना है—कैसे वह बंधन उत्पन्न होता है और कैसे उसे छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार, सतिपट्ठान की साधना में हमें अलग-अलग स्वभावों के प्रति अलग-अलग रवैय्या, अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने हैं, और यह सब बहुत सक्रियता के साथ करना हैं।
सतिपट्ठान की साधना में तीन चरण होते हैं। आगे आने वाले प्रत्येक पर्व के अंतिम पैराग्राफ पर गौर करें—
(१) लोक के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाते हुए, “भीतरी और बाहरी” बातों पर गौर करना।
(२) “समुदय और व्यय स्वभाव” देखकर, “इदप्पच्चयता” पता लगाना।
(३) स्मृति स्थापित हो जाने पर, “अनाश्रित होकर रहना, दुनिया का आधार नहीं लेना”। इस तीसरे चरण को “अतम्मयता” कहते हैं।
अर्थात, जब पहले दोनों चरण पूरे हो जाते हैं और हम किसी अमुक स्वभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं, तब एक समय आता है, जिसमें अमुक स्वभाव के रहने पर, “यह अमुक स्वभाव है”—ऐसी विशेष प्रकार की स्मृति उपेक्षा के साथ स्थापित हो जाती है। उसमें “मैं” या “मेरा” का कोई भाव नहीं होता, और व्यक्ति उस समय पाँच आधार-स्कंधों या कहें तो, दुनिया का आधार छोड़कर, अनाश्रित रूप से स्थित होता है। कुछ समय तक इसी अवस्था में रहने के बाद, अंततः चित्त विमुक्त हो जाता है और आर्यफल की प्राप्ति होती है।
आईयें, अब भगवान के शब्दों में जानें कि चारों स्मृतिप्रस्थान की साधना कैसे की जाती है:
हिन्दी
ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान कुरु देश में कम्मासधम्म नामक कुरु निगम में विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, “भिक्षुओं!”
“भदन्त!” भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया।
भगवान ने कहा, “भिक्षुओं, यह चार स्मृतिप्रस्थान एक-तरफ़ा 1 मार्ग है—सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक और विलाप को लाँघने के लिए, दर्द और व्यथा को विलुप्त करने के लिए, सही तरीक़ा पाने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए। कौन-से चार?
यहाँ, भिक्षुओं, कोई भिक्षु लोक के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाकर, काया को काया देखते हुए रहता है—तत्पर, सचेत और स्मृतिमान। वह लोक के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाकर, वेदना को वेदना देखते हुए रहता है—तत्पर, सचेत और स्मृतिमान। वह लोक के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाकर, चित्त को चित्त देखते हुए रहता है—तत्पर, सचेत और स्मृतिमान। वह लोक के प्रति लालसा या नाराज़ी हटाकर, स्वभाव को स्वभाव देखते हुए रहता है—तत्पर, सचेत और स्मृतिमान।
१. काया को देखना
भिक्षुओं, कोई भिक्षू जंगल में, या पेड़ के तले, या निर्जन ध्यानस्थल में जाकर पालथी मारकर, शरीर को सीधा रखते हुए बैठता है, और स्मृति को अपने सामने उपस्थित करता है। वह स्मृतिपूर्वक श्वास लेता है, और स्मृतिपूर्वक श्वास छोड़ता है।
- लंबी श्वास लेते हुए जानता है, ‘लंबी श्वास ले रहा हूँ।’ लंबी श्वास छोड़ते हुए जानता है, ‘लंबी श्वास छोड़ रहा हूँ।’
- छोटी श्वास लेते हुए जानता है, ‘छोटी श्वास ले रहा हूँ।’ छोटी श्वास छोड़ते हुए जानता है, ‘छोटी श्वास छोड़ रहा हूँ।’
- पूरी काया महसूस करते हुए श्वास लेना सीखता है। पूरी काया महसूस करते हुए श्वास छोड़ना सीखता है।
- काया के संस्कार को शान्त करते हुए श्वास लेना सीखता है। काया के संस्कार को शान्त करते हुए श्वास छोड़ना सीखता है। 2
जैसे, भिक्षुओं, निपुण बढ़ई को औजार लंबा घुमाते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबा घुमा रहा हूँ।’ और, उसे छोटा घुमाते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटा घुमा रहा हूँ।’ उसी तरह, भिक्षुओं, भिक्षु को लंबी-साँस लेते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबी-साँस ले रहा हूँ।’ और, उसे लंबी-साँस छोड़ते हुए पता चलता है कि ‘मैं लंबी-साँस छोड़ रहा हूँ।’ उसे छोटी-साँस लेते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटी-साँस ले रहा हूँ।’ और उसे छोटी-साँस छोड़ते हुए पता चलता है कि ‘मैं छोटी-साँस छोड़ रहा हूँ।’ वह संपूर्ण शरीर महसूस करते हुए साँस लेना सीखता है; वह संपूर्ण शरीर महसूस करते हुए साँस छोड़ना सीखता है। वह कायिक-संस्कार को शान्त करते हुए साँस लेना सीखता है; वह कायिक-संस्कार को शान्त करते हुए साँस छोड़ना सीखता है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को [मात्र] काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी [हर जगह] काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव [“समुदय-धम्म”] देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित [=स्वतंत्र] होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, उस भिक्षु को—
- चलते हुए पता चलता है कि ‘चल रहा हूँ।’
- खड़े हुए पता चलता है कि ‘खड़ा हूँ।’
- बैठे हुए पता चलता है कि ‘बैठा हूँ।’
- लेटे हुए पता चलता है कि ‘लेटा हूँ।’
- जिस-जिस तरह उसकी काया अवस्था लेती है, उस-उस तरह उसे पता चलता है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु—
- आगे बढ़ते और लौट आते सचेत रहता है।
- नज़र टिकाते और नज़र हटाते सचेत रहता है।
- [अंग को] सिकोड़ते और पसारते हुए सचेत रहता है।
- संघाटि, पात्र और चीवर धारण करते हुए सचेत रहता है।
- खाते, पीते, चबाते, स्वाद लेते हुए सचेत रहता है।
- पेशाब और शौच करते हुए सचेत रहता है।
- चलते, खड़े रहते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, मौन होते हुए सचेत रहता है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु अपनी काया को पैर तल से ऊपर, माथे के केश से नीचे, त्वचा से ढ़की हुई, नाना प्रकार की गंदगियों से भरी हुई मनन करता है—‘मेरी इस काया में हैं—केश, लोम, नाखून, दाँत, त्वचा; माँस, नसें, हड्डी, हड्डीमज्जा, तिल्ली; हृदय, कलेजा, झिल्ली, गुर्दा, फेफड़ा; आँत, छोटी-आँत, उदर, टट्टी, मस्तिष्क; पित्त, कफ, पीब, रक्त, पसीना, चर्बी; आँसू, तेल, थूक, बलगम, जोड़ो में तरल, मूत्र।’
जैसे, किसी खुली बोरी में चावल, गेहूँ, मूँग, राजमा, तिल, कनकी आदि नाना-प्रकार का अनाज भरा हो। तब, कोई अच्छी आँखोंवाला पुरुष उसे नीचे उड़ेलकर पता करें—‘यह चावल है, यह गेहूँ है, यह मूँग है, यह राजमा है, यह तिल है, यह कनकी है।’ उसी तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु अपनी काया को पैर तल से ऊपर, माथे के केश से नीचे, त्वचा से ढ़की हुई, नाना प्रकार की गंदगियों से भरी हुई मनन करता है—‘मेरी इस काया में हैं—केश, लोम, नाखून, दाँत, त्वचा; माँस, नसें, हड्डी, हड्डीमज्जा, तिल्ली; हृदय, कलेजा, झिल्ली, गुर्दा, फेफड़ा; आँत, छोटी-आँत, उदर, टट्टी, मस्तिष्क; पित्त, कफ, पीब, रक्त, पसीना, चर्बी; आँसू, तेल, थूक, बलगम, जोड़ो में तरल, मूत्र।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु इस काया को, चाहे जिस अवस्था, जिस परिस्थिति में हो, धातु के अनुसार मनन करता है—‘इस काया में—
- पृथ्वीधातु है;
- जलधातु है;
- अग्निधातु है;
- वायुधातु है।’
जैसे, कोई कसाई गाय को काटकर उसे चौराहे पर अलग-अलग ढ़ेर बनाकर बैठता है। उसी तरह, वह भिक्षु इस काया को, चाहे जिस अवस्था, जिस परिस्थिति में हो, धातु के अनुसार मनन करता है—‘इस काया में पृथ्वीधातु है; जलधातु है; अग्निधातु है; वायुधातु है।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
(१) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—एक दिन पुरानी, दो दिन पुरानी, तीन दिन पुरानी—फूल चुकी, नीली पड़ चुकी, पीब रिसती हुई। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है—‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
(२) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—कौवों द्वारा नोची जाती, चीलों द्वारा नोची जाती, गिद्धों द्वारा नोची जाती, बगुलों द्वारा नोची जाती, कुत्तों द्वारा चबाई जाती, बाघ द्वारा चबाई जाती, तेंदुए द्वारा चबाई जाती, सियार द्वारा चबाई जाती, अथवा विविध जंतुओं द्वारा खायी जाती। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है—‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
(३) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—माँस से युक्त, रक्त से सनी, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…
(४) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—माँस के बिना, रक्त से सनी, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…
(५) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—माँस के बिना, रक्त के बिना, नसों से बँधी, हड्डी-कंकालवाली…
(६) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—माँस के बिना, रक्त के बिना, नसों से बिना बँधी, हड्डियाँ जहाँ-वहाँ बिखरी हुई—कही हाथ की हड्डी; कही पैर की; कही टखने की हड्डी; कही जाँघ की; कही कुल्हे की हड्डी; कही कमर की; कही पसली; कही पीठ की हड्डी; कही कंधे की हड्डी; कही गर्दन की; कही ठोड़ी की हड्डी; कही दाँत; कही खोपड़ी। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है—‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
(७) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—हड्डियाँ शंख जैसे सफ़ेद हो चुकी…
(८) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—वर्षोंपश्चात, जब हड्डियों का ढ़ेर लगा हो…
(९) आगे, भिक्षुओं, वह भिक्षु श्मशान में पड़ी लाश देखता है—जब हड्डियाँ सड़कर चूर्ण बन चुकी हो। तब वह उसे अपनी काया से तुलना करता है—‘मेरी काया भी इसी स्वभाव की है। आगे यही होना है। यह टाला नहीं जा सकता।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी काया को काया देखते हुए रहता है। अथवा, वह काया का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा काया का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह काया है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है।
२. वेदना देखना
और, आगे भिक्षुओं, कैसे कोई भिक्षु वेदना को वेदना देखते हुए रहता है? यहाँ भिक्षु को सुख महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं सुख महसूस कर रहा हूँ।’ दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ।’ नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ।’
उसे भौतिक सुख [“सामिस सुख”] महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक सुख महसूस कर रहा हूँ।’ उसे आध्यात्मिक सुख [“निरामिस सुख”] महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक सुख महसूस कर रहा हूँ।’ उसे भौतिक दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक दर्द महसूस कर रहा हूँ।’ उसे आध्यात्मिक दर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक दर्द महसूस कर रहा हूँ।’ उसे भौतिक नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं भौतिक नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ।’ उसे आध्यात्मिक नसुख-नदर्द महसूस करते हुए पता चलता है कि ‘मैं आध्यात्मिक नसुख-नदर्द महसूस कर रहा हूँ।’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी वेदना को वेदना देखते हुए रहता है; अथवा, बाहरी वेदना को वेदना देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी वेदना को वेदना देखते हुए रहता है। अथवा, वह वेदना का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा वेदना का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा वेदना का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह वेदना है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु वेदना को वेदना देखते हुए रहता है।
३. चित्त देखना
और, आगे भिक्षुओं, कैसे भिक्षु चित्त को चित्त देखते हुए रहता है? यहाँ भिक्षु को—
- रागपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह रागपूर्ण चित्त है’
- वीतराग चित्त पता चलता है कि ‘यह वीतराग चित्त है’
- द्वेषपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह द्वेषपूर्ण चित्त है’
- द्वेषविहीन चित्त पता चलता है कि ‘यह द्वेषविहीन चित्त है’
- मोहपूर्ण चित्त पता चलता है कि ‘यह मोहपूर्ण चित्त है’
- मोहविहीन चित्त पता चलता है कि ‘यह मोहविहीन चित्त है’
- संकुचित [“सङखित्त”] चित्त पता चलता है कि ‘संकुचित चित्त है’
- बिखरा [“विक्खित्त”] चित्त पता चलता है कि ‘बिखरा चित्त है’
- बढ़ा हुआ [“महग्गत”] चित्त पता चलता है कि ‘यह विस्तारित चित्त है’
- न बढ़ा [“अमहग्गत”] चित्त पता चलता है कि ‘यह अविस्तारित चित्त है’
- बेहतर [“उत्तर”] चित्त पता चलता है कि ‘यह बेहतर चित्त है’
- सर्वोत्तर [“अनुत्तर”] चित्त पता चलता है कि ‘यह सर्वोत्तर चित्त है’
- समाहित चित्त पता चलता है कि ‘यह समाहित चित्त है’
- असमाहित चित्त पता चलता है कि ‘यह असमाहित चित्त है’
- विमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘यह विमुक्त चित्त है’
- अविमुक्त चित्त पता चलता है कि ‘यह अविमुक्त चित्त है!’
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी चित्त को चित्त देखते हुए रहता है। अथवा, वह चित्त का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा चित्त का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा चित्त का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह चित्त है।’ और जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु चित्त को चित्त देखते हुए रहता है।
४. धम्म देखना
और, भिक्षुओं, कैसे कोई भिक्षु स्वभाव [“धम्म” = मन में चल रही बात] को स्वभाव देखते हुए रहता है? यहाँ कोई भिक्षु पाँच व्यवधान [“पञ्च नीवरण”] स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई भिक्षु पाँच व्यवधान स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?
• यहाँ किसी भिक्षु को भीतर कामेच्छा होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर कामेच्छा है।” अथवा कामेच्छा न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर कामेच्छा नहीं है।” उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न कामेच्छा की उत्पत्ति होती है। उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न कामेच्छा खत्म होती है। और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई कामेच्छा की दुबारा उत्पत्ति न होगी।
• उसे भीतर दुर्भावना होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर दुर्भावना है।” अथवा दुर्भावना न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर दुर्भावना नहीं है।” उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न दुर्भावना की उत्पत्ति होती है। उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न दुर्भावना खत्म होती है। और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई दुर्भावना की दुबारा उत्पत्ति न होगी।
• उसे भीतर सुस्ती और तंद्रा होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर सुस्ती और तंद्रा है।” अथवा सुस्ती और तंद्रा न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर सुस्ती और तंद्रा नहीं है।” उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न सुस्ती और तंद्रा की उत्पत्ति होती है। उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न सुस्ती और तंद्रा खत्म होती है। और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई सुस्ती और तंद्रा की दुबारा उत्पत्ति न होगी।
• उसे भीतर बेचैनी और पश्चाताप होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर बेचैनी और पश्चाताप है”। अथवा बेचैनी और पश्चाताप न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर बेचैनी और पश्चाताप नहीं है।” उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न बेचैनी और पश्चाताप की उत्पत्ति होती है। उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न बेचैनी और पश्चाताप खत्म होती है। और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई बेचैनी और पश्चाताप की दुबारा उत्पत्ति न होगी।
• उसे भीतर अनिश्चितता [=संदेह] होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर अनिश्चितता है।” अथवा अनिश्चितता न होने पर पता चलता है कि “मेरे भीतर अनिश्चितता नहीं है।” उसे पता चलता है कि कैसे अनुत्पन्न अनिश्चितता की उत्पत्ति होती है। उसे पता चलता है कि कैसे उत्पन्न अनिश्चितता खत्म होती है। और, उसे पता चलता है कि कैसे खत्म हुई अनिश्चितता की दुबारा उत्पत्ति न होगी।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु पाँच व्यवधान स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।
और, आगे भिक्षुओं, कोई भिक्षु पाँच आधार-संग्रह [“पञ्च उपादानक्खन्ध”] स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई भिक्षु पाँच आधार-संग्रह स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?
कोई भिक्षु पता करता है—‘यह रूप है; यह रूप की उत्पत्ति है; यह रूप की विलुप्ती है। यह वेदना है; यह वेदना की उत्पत्ति है; यह वेदना की विलुप्ती है। यह संज्ञा है; यह संज्ञा की उत्पत्ति है; यह संज्ञा की विलुप्ती है। यह संस्कार है; यह संस्कार की उत्पत्ति है; यह संस्कार की विलुप्ती है। यह विज्ञान है; यह विज्ञान की उत्पत्ति है; यह विज्ञान की विलुप्ती है।’3
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु पाँच आधार-संग्रह स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, कोई भिक्षु छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई भिक्षु छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?
• यहाँ कोई भिक्षु आँख पता करता है; रूप पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन [“संयोजन”] पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
• वह कान पता करता है; आवाज़ पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
• वह नाक पता करता है; गंध पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
• वह जीभ पता करता है; स्वाद पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
• वह काया पता करता है; संस्पर्श पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
• वह मन पता करता है; स्वभाव पता करता है; उन दोनों पर आधार पर जो बंधन पैदा होता है, उसे पता करता है। अनुत्पन्न बंधन कैसे उत्पन्न होता है, वह पता करता है। उत्पन्न बंधन कैसे छोड़ा जाता है, वह पता करता है। और, छूटा बंधन कैसे दुबारा न उत्पन्न हो, वह पता करता है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु छह भीतरी-बाहरी आयाम स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।
और, आगे, भिक्षुओं, कोई भिक्षु सात संबोधि-अंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई भिक्षु सात संबोधि-अंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?
• यहाँ किसी भिक्षु में भीतर स्मृति (“सति”) संबोधिअंग हो, तो उसे पता चलता है कि ‘मेरे भीतर स्मृति संबोधिअंग है।’ अथवा भीतर स्मृति संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि ‘मेरे भीतर स्मृति संबोधिअंग नहीं है।’ उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न स्मृति संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ स्मृति संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर धम्म-विचय (“धम्मविचय”) संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर धम्म-विचय संबोधिअंग है।” अथवा भीतर धम्म-विचय संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर धम्म-विचय संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न धम्म-विचय संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ धम्म-विचय संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर वीर्य (“वीरिय”) संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर वीर्य संबोधिअंग है।” अथवा भीतर वीर्य संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर वीर्य संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न वीर्य संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ वीर्य संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर प्रीति (“पीति”) संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रीति संबोधिअंग है।” अथवा भीतर प्रीति संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रीति संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न प्रीति संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ प्रीति संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर प्रश्रब्धि (“पस्सद्धि”) संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रश्रब्धि संबोधिअंग है।” अथवा भीतर प्रश्रब्धि संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर प्रश्रब्धि संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न प्रश्रब्धि संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ प्रश्रब्धि संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर समाधि संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर समाधि संबोधिअंग है।” अथवा भीतर समाधि संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर समाधि संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न समाधि संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ समाधि संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
• उसे भीतर उपेक्षा (“उपेक्खा”) संबोधिअंग हो, तो पता चलता है कि “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधिअंग है।” अथवा भीतर उपेक्षा संबोधिअंग न हो, तो उसे पता चलता है कि “मेरे भीतर उपेक्षा संबोधिअंग नहीं है।” उसे पता चलता है कि अनुत्पन्न उपेक्षा संबोधिअंग कैसे उत्पन्न होता है। और, उसे पता चलता है कि उत्पन्न हुआ उपेक्षा संबोधिअंग विकसित होकर परिपूर्ण कैसे होता है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु सात संबोधिअंग स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।
आगे, भिक्षुओं, कोई भिक्षु चार आर्यसत्य स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। कैसे कोई भिक्षु चार आर्यसत्य स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है?
यहाँ कोई भिक्षु ‘यह दुःख है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘यह दुःख की उत्पत्ति है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘यह दुःख का निरोध है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है। ‘यह दुःख का निरोध-मार्ग है’, उसे यथास्वरूप पता चलता है।
भिक्षुओं, यह दुःख आर्यसत्य क्या है?
जन्म कष्टपूर्ण [=दुःख] है, बुढ़ापा कष्टपूर्ण है, मौत कष्टपूर्ण है। शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, और निराशा कष्टपूर्ण है। अप्रिय से जुड़ाव कष्टपूर्ण है। प्रिय से अलगाव कष्टपूर्ण है। इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है। संक्षिप्त में, पाँच आधार-संग्रह कष्टपूर्ण है।
जन्म क्या है? भिन्न-भिन्न सत्वों का भिन्न-भिन्न समूह में जन्म होना, जन्म लेना, उत्पत्ति होना, उद्भव होना, [पाँच आधार] संग्रह का प्रादुर्भाव होना, [छह] आयामों का प्राप्त होना—यह जन्म कहलाता है।
बुढ़ापा क्या है? भिन्न-भिन्न सत्वों का भिन्न-भिन्न समूह में बूढ़ा होना, जीर्ण होना, [दाँत] टूटना, [केश] सफ़ेद होना, [त्वचा पर] झुर्रियां पड़ना, प्राण-ऊर्जा [“आयु”] में कमी आना, इंद्रियाँ कमज़ोर होना—यह बुढ़ापा कहलाता है।
मौत क्या है? भिन्न-भिन्न सत्वों का भिन्न-भिन्न समूह से च्युति होना, गुज़र जाना, अलगाव होना, अंतर्धान होना, मृत्यु होना, निधन होना, समयावधि समाप्त [“कालकिरिया”] होना, संग्रह का बिखरना, शरीर त्यागना, जीवित-इंद्रिय रुक जाना—यह मौत कहलाती है।
शोक क्या है? भिन्न-भिन्न दुर्भाग्यों से पीड़ित, भिन्न-भिन्न दर्द-स्वभावों से संस्पर्शित [छूते] सत्वों का शोक, खेद, अफ़सोस; स्वयं को लेकर खेद होना, स्वयं को लेकर अफ़सोस होना—यह शोक कहलाता है।
विलाप [“परिदेव”] क्या है? भिन्न-भिन्न दुर्भाग्यों से पीड़ित, भिन्न-भिन्न दर्द-स्वभावों से संस्पर्शित सत्वों का रोना, बिलखना, विलाप करना, क्रंदन करना, आँसू बहाना, मातम करना—यह विलाप कहलाता है।
दर्द क्या है? शारीरिक पीड़ा, शारीरिक परेशानी, काया से छूने पर पीड़ा और परेशानी महसूस होना—यह दर्द कहलाता है।
व्यथा क्या है? मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी, मन से छूने पर पीड़ा और परेशानी महसूस होना—यह व्यथा कहलाती है।
निराशा [“उपायास”] क्या है? भिन्न-भिन्न दुर्भाग्यों से पीड़ित, भिन्न-भिन्न दर्द-स्वभावों से संस्पर्शित सत्वों का हताश होना, निराश होना, उदास होना, मायूस होना—यह निराशा कहलाती है।
अप्रिय से जुड़ाव क्या है? यहाँ किसी के इच्छाविरुद्ध, नापसंद अनाकर्षक रूप, आवाज़, गन्ध, स्वाद, संस्पर्श और स्वभाव—अथवा अनर्थ चाहने वाले, अहित चाहने वाले, असुविधा चाहने वाले, योगबन्धन से राहत न चाहने वाले—के साथ संगति होना, भेट होना, साथ जुड़ना, मेलमिलाप होना—यह कहलाता है ‘अप्रिय से जुड़ाव कष्टपूर्ण है’।
प्रिय से अलगाव क्या है? यहाँ किसी की इच्छानुसार, पसंदीदा आकर्षक रूप, आवाज़, गन्ध, स्वाद, संस्पर्श और स्वभाव—अथवा भला चाहने वाले, हित चाहने वाले, सुविधा चाहने वाले, योगबन्धन से राहत चाहने वाले माता, पिता, बहन, भाई, मित्र, साथी, रक्तसंबंधी रिश्तेदार—के साथ संगति न होना, भेट न होना, साथ न जुड़ना, मेलमिलाप न होना—यह कहलाता है ‘प्रिय से अलगाव कष्टपूर्ण है’।
इच्छापूर्ति न होना क्या है? जन्म-स्वभाव वाले सत्वों को [कभी] ऐसी इच्छा प्रकट होती हैं—‘अरे! हम जन्म-स्वभाव वाले न होते! काश, हमारा जन्म न होता!’ किंतु वह [मात्र] इच्छा करने से नहीं मिलता—यह कहलाता है ‘इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है’।
बुढ़ापा-स्वभाव वाले सत्वों को ऐसी इच्छा प्रकट होती हैं—‘अरे! हम बुढ़ापा-स्वभाव वाले न होते! काश, हम बूढ़े न होते!’ किंतु वह इच्छा करने से नहीं मिलता—यह कहलाता है ‘इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है’।
रोग-स्वभाववाले सत्वों को ऐसी इच्छा प्रकट होती हैं—‘अरे! हम रोग-स्वभाव वाले न होते! काश, हमें रोग ही न होता!’ किंतु वह इच्छा करने से नहीं मिलता—यह कहलाता है ‘इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है’।
मौत-स्वभाववाले सत्वों को ऐसी इच्छा प्रकट होती हैं—‘अरे! हम मौत-स्वभाव वाले न होते! काश, हमारी मौत न होती!’ किंतु वह इच्छा करने से नहीं मिलता—यह कहलाता है ‘इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है’।
शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, और निराशा—स्वभाव वाले सत्वों को ऐसी इच्छा प्रकट होती हैं—‘अरे! हम शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, और निराशा—स्वभाव वाले न होते! काश, हमें शोक, विलाप, दर्द, व्यथा, और निराशा न होती!’ किंतु वह इच्छा करने से नहीं मिलता—यह कहलाता है ‘इच्छापूर्ति न होना कष्टपूर्ण है’।
संक्षिप्त में, पाँच आधार-संग्रह क्या है? यही, जैसे कि रूप आधार-संग्रह, वेदना आधार-संग्रह, संज्ञा आधार-संग्रह, संस्कार आधार-संग्रह, विज्ञान आधार-संग्रह—यह कहलाता है ‘संक्षिप्त में, पाँच आधार-संग्रह कष्टपूर्ण है’।
और, भिक्षुओं, दुःख उत्पत्ति आर्यसत्य क्या है?
यह जो तृष्णा है—पुनः अस्तित्व बनाने वाली, मज़ा और दिलचस्पी के साथ आने वाली, यहाँ-वहाँ लुत्फ़ उठाने वाली—अर्थात [छह इंद्रियसुख पाने की] काम तृष्णा, अस्तित्व [बनाने की] तृष्णा, और अस्तित्व मिटाने की तृष्णा।
किन्तु, भिक्षुओं, यह तृष्णा जागनी हो तो कहाँ जागती [पैदा होती] है, बसनी हो तो कहाँ बसती [निवास करती] है? इस दुनिया में जो प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में क्या प्रिय होता है, अच्छा लगता है? इस दुनिया में आँख प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है। इस दुनिया में कान… नाक… जीभ… काया… मन प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप… आवाज़… गंध… स्वाद… संस्पर्श… स्वभाव प्रिय होते हैं, अच्छे लगते हैं—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में आँख विज्ञान… कान विज्ञान… नाक विज्ञान… जीभ विज्ञान… काया विज्ञान… मन विज्ञान प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में आँख का संपर्क… कान का संपर्क… नाक का संपर्क… जीभ का संपर्क… काया का संपर्क… मन का संपर्क प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में आँख संपर्क से जागी वेदना… कान संपर्क से जागी वेदना… नाक संपर्क से जागी वेदना… जीभ संपर्क से जागी वेदना… काया संपर्क से जागी वेदना… मन संपर्क से जागी वेदना प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति संज्ञा… आवाज़ के प्रति संज्ञा… गंध के प्रति संज्ञा… स्वाद के प्रति संज्ञा… संस्पर्श के प्रति संज्ञा… स्वभाव के प्रति संज्ञा प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति इरादा [“संचेतना”]… आवाज़ के प्रति इरादा… गंध के प्रति इरादा… स्वाद के प्रति इरादा… संस्पर्श के प्रति इरादा… स्वभाव के प्रति इरादा प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति तृष्णा… आवाज़ के प्रति तृष्णा… गंध के प्रति तृष्णा… स्वाद के प्रति तृष्णा… संस्पर्श के प्रति तृष्णा… स्वभाव के प्रति तृष्णा प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति वितर्क [“वितक्क”]… आवाज़ के प्रति वितर्क… गंध के प्रति वितर्क… स्वाद के प्रति वितर्क… संस्पर्श के प्रति वितर्क… स्वभाव के प्रति वितर्क प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति विचार… आवाज़ के प्रति विचार… गंध के प्रति विचार… स्वाद के प्रति विचार… संस्पर्श के प्रति विचार… स्वभाव के प्रति विचार प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा जागनी हो तो यही जागती है, बसनी हो तो यही बसती है।
भिक्षुओं, यह कहलाता है दुःख-उत्पत्ति आर्यसत्य।
और, भिक्षुओं, दुःख-निरोध आर्यसत्य क्या है?
उसी तृष्णा का, बिना अवशेष रहे वैराग्य होना, निरोध होना, त्याग दिया जाना, संन्यास ले लेना, मुक्ति होना, आश्रय छूट जाना।
भिक्षुओं, यह तृष्णा छोड़नी हो तो कहाँ छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो कहाँ ख़त्म होती है? इस दुनिया में जो प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में क्या प्रिय होता है, अच्छा लगता है? इस दुनिया में आँख प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है। इस दुनिया में कान… नाक… जीभ… काया… मन प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप… आवाज़… गंध… स्वाद… संस्पर्श… स्वभाव प्रिय होते है, अच्छे लगते है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में आँख विज्ञान… कान विज्ञान… नाक विज्ञान… जीभ विज्ञान… काया विज्ञान… मन विज्ञान प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में आँख का संपर्क… कान का संपर्क… नाक का संपर्क… जीभ का संपर्क… काया का संपर्क… मन का संपर्क प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में आँख संपर्क से जागी वेदना… कान संपर्क से जागी वेदना… नाक संपर्क से जागी वेदना… जीभ संपर्क से जागी वेदना… काया संपर्क से जागी वेदना… मन संपर्क से जागी वेदना प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति संज्ञा… आवाज़ के प्रति संज्ञा… गंध के प्रति संज्ञा… स्वाद के प्रति संज्ञा… संस्पर्श के प्रति संज्ञा… स्वभाव के प्रति संज्ञा प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति इरादा… आवाज़ के प्रति इरादा… गंध के प्रति इरादा… स्वाद के प्रति इरादा… संस्पर्श के प्रति इरादा… स्वभाव के प्रति इरादा प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति तृष्णा… आवाज़ के प्रति तृष्णा… गंध के प्रति तृष्णा… स्वाद के प्रति तृष्णा… संस्पर्श के प्रति तृष्णा… स्वभाव के प्रति तृष्णा प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति वितर्क… आवाज़ के प्रति वितर्क… गंध के प्रति वितर्क… स्वाद के प्रति वितर्क… संस्पर्श के प्रति वितर्क… स्वभाव के प्रति वितर्क प्रिय होती है, अच्छी लगती है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
इस दुनिया में रूप के प्रति विचार… आवाज़ के प्रति विचार… गंध के प्रति विचार… स्वाद के प्रति विचार… संस्पर्श के प्रति विचार… स्वभाव के प्रति विचार प्रिय होता है, अच्छा लगता है—तृष्णा छोड़नी हो तो यही छोड़ी जाती है, खत्म करनी हो तो यही खत्म होती है।
भिक्षुओं, यह कहलाता है दुःख-निरोध आर्यसत्य।
और, भिक्षुओं, यह दुःख-निरोध मार्ग आर्यसत्य क्या है?
बस यही, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अर्थात, सम्यक-दृष्टि, सम्यक-संकल्प, सम्यक-वचन, सम्यक-कर्मांत, सम्यक-जीविका, सम्यक-प्रयास, सम्यक-स्मृति, और सम्यक-समाधि।
भिक्षुओं, यह सम्यक-दृष्टि क्या है? दुःख का ज्ञान, दुःख उत्पत्ति का ज्ञान, दुःख निरोध का ज्ञान, और दुःख निरोध-मार्ग का ज्ञान। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-दृष्टि।
और, भिक्षुओं, सम्यक-संकल्प क्या है? निष्काम का संकल्प, दुर्भावनाविहीन संकल्प, और अहिंसात्मक संकल्प। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-संकल्प।
और, भिक्षुओं, सम्यक-वचन क्या है? असत्य वचन से विरत रहना, फूट डालनेवाले वचन से विरत रहना, कटु वचन से विरत रहना, व्यर्थ वचन से विरत रहना। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-वचन।
और, भिक्षुओं, सम्यक-कर्मांत क्या है? जीवहत्या से विरत रहना, चुराने से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-कर्मांत।
और, भिक्षुओं, सम्यक-जीविका क्या है? यहाँ, भिक्षुओं, कोई भिक्षु मिथ्या-जीविका त्यागता है, और सम्यक जीविका से जीवन चलाता है। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-जीविका।
और, भिक्षुओं, सम्यक-प्रयास क्या है? यहाँ, भिक्षुओं, कोई भिक्षु अनुत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव उत्पन्न न हो—उसके लिए भिक्षु चाह पैदा करता है, मेहनत करता है, ज़ोर लगाता है, इरादा बनाकर जुटता है। वह उत्पन्न पाप, अकुशल स्वभाव छोड़ने के लिए चाह पैदा करता है, मेहनत करता है, ज़ोर लगाता है, इरादा बनाकर जुटता है। वह अनुत्पन्न कुशल स्वभाव उत्पन्न करने के लिए चाह पैदा करता है, मेहनत करता है, ज़ोर लगाता है, इरादा बनाकर जुटता है। वह उत्पन्न कुशल स्वभाव टिकाए रखने, आगे लाने, वृद्धि करने, प्रचुरता लाने, विकसित कर परिपूर्ण करने के लिए चाह पैदा करता है, मेहनत करता है, ज़ोर लगाता है, इरादा बनाकर जुटता है। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-प्रयास।
और, भिक्षुओं, सम्यक-स्मृति क्या है? कोई भिक्षु काया को काया देखते हुए रहता है—तत्पर सचेत और स्मृतिमान, लोक के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाते हुए। वेदना को वेदना देखते हुए रहता है—तत्पर सचेत और स्मृतिमान, लोक के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाते हुए। चित्त को चित्त देखते हुए रहता है—तत्पर सचेत और स्मृतिमान, लोक के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाते हुए। स्वभाव को स्वभाव देखते हुए रहता है—तत्पर सचेत और स्मृतिमान, लोक के प्रति लालसा और नाराज़ी हटाते हुए। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-स्मृति।
और, भिक्षुओं, सम्यक-समाधि क्या है? यहाँ भिक्षुओं, कोई भिक्षु कामुकता से निर्लिप्त, अकुशल स्वभाव से निर्लिप्त—वितर्क और विचार सहित, निर्लिप्तता से जन्मे प्रीति और सुख वाले प्रथम-ध्यान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है। आगे, वितर्क और विचार थमने पर भीतर आश्वस्त हुआ मानस एकरस होकर बिना-वितर्क बिना-विचार, समाधि से जन्मे प्रीति और सुख वाले द्वितीय-ध्यान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है। तब, आगे वह प्रीति से विरक्ति ले, स्मृति और सचेतता के साथ उपेक्षा धारण कर शरीर से सुख महसूस करता है। जिसे आर्यजन ‘उपेक्षक, स्मृतिमान, सुखविहारी’ कहते हैं—वह उस तृतीय-ध्यान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है। आगे, वह सुख और दुःख के परित्याग से, तथा पूर्व के सौमनस्य और दौमनस्य के विलुप्त होने से—न सुख, न दुःख; उपेक्षा और स्मृति की परिशुद्धता के साथ चतुर्थ-ध्यान में प्रवेश पाकर उसमें विहार करता है। यही है, भिक्षुओं, सम्यक-समाधि।
और, भिक्षुओं, यही दुःख निरोध-मार्ग आर्यसत्य है।
इस तरह, भिक्षुओं, वह भिक्षु भीतरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा भीतरी और बाहरी स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, वह स्वभाव का उत्पत्ति-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है; अथवा स्वभाव का उत्पत्ति और व्यय-स्वभाव देखते हुए रहता है। अथवा, उसकी स्मृति स्थापित हो जाती है—‘यह स्वभाव है।’ और, जब तक यह ज्ञान, यह याद बनी रहती है, वह अनाश्रित होकर रहता है; दुनिया का आधार नहीं लेता। इस तरह, भिक्षुओं, कोई भिक्षु चार आर्यसत्य स्वभावों को स्वभाव देखते हुए रहता है।
अब, भिक्षुओं, जो इस तरह चार स्मृतिप्रस्थान की साधना ७ वर्षों तक करें, उसे दो में से एक फ़ल अपेक्षित है—अभी यही परमज्ञान, अथवा आधार शेष बचने पर अनागामिता।
छोड़ो, भिक्षुओं, ७ वर्ष ! जो इस तरह चार स्मृतिप्रस्थान की साधना ६ वर्षों तक… ५ वर्षों तक… ४ वर्षों तक… ३ वर्षों तक… २ वर्षों तक… १ वर्ष तक… ७ महीने तक करें, उसे दो में से एक फ़ल अपेक्षित है—अभी यही परमज्ञान, अथवा आधार शेष बचने पर अनागामिता।
छोड़ो, भिक्षुओं, ७ वर्ष ! जो इस तरह चार स्मृतिप्रस्थान की साधना ६ महीने तक… ५ महीने तक… ४ महीने तक… ३ महीने तक… २ महीने तक… १ महीने तक… आधे महीने तक… मात्र ७ दिनों तक अभ्यास करें, उसे दो में से एक फ़ल अपेक्षित है—अभी यही परमज्ञान, अथवा आधार शेष बचने पर अनागामिता।
भिक्षुओं, यह चार स्मृतिप्रस्थान एकतरफ़ा मार्ग है—सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक और विलाप लाँघने के लिए, दर्द और व्यथा को विलुप्त करने के लिए, सही तरीक़ा पाने के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए। मैंने जो कहा था, इसलिए कहा था।”
भगवान ने ऐसा कहा। संतुष्ट हुए भिक्षुओं ने भगवान के कथन का अनुमोदन किया।
सुत्र समाप्त।
-
दशकों तक एकायनो मग्गो का अनुवाद होता था, ‘इकलौता मार्ग’। किंतु, भन्ते ञाणमोली के पश्चात, अनुवादकों ने उसके पूर्व संदर्भ की ओर गौर किया, और पाया कि दरअसल उसका अर्थ वन वे होता है। अर्थात, ऐसा एक-तरफा रास्ता, जो एक ही दिशा में आगे बढ़े, और एक ही मंज़िल पर ले जाए, दुसरे रास्तें न खुले। ↩︎
-
मज्झिमनिकाय ४४ के अनुसार आश्वास-प्रश्वास, अर्थात, आती-जाती साँस ही कायिक-संस्कार है। हम भिन्न-भिन्न तरह से साँस लेकर भिन्न-भिन्न तरह से काया महसूस करते है, और उसे बनाते है। ↩︎
-
रूप की उत्पत्ति क्या है?
कोई व्यक्ति [भौतिक] रूप से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है। जब वह रूप से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है, तब उसे मज़ा आता है। रूप का किसी भी तरह मज़ा लेना आधार बनाता है। आधार के कारण अस्तित्व पनपता है। अस्तित्व के कारण जन्म होता है। जन्म के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला चल पड़ता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह की उत्पत्ति होती है।
वेदना…नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता की उत्पत्ति क्या है?
कोई व्यक्ति वेदना… नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है। जब वह वेदना… नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता से आनंदित होता है, स्वीकार करता है, जुड़ जाता है, तब उसे मज़ा आता है। वेदना… नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता का किसी भी तरह मज़ा लेना आधार बनाता है। आधार के कारण अस्तित्व पनपता है। अस्तित्व के कारण जन्म होता है। जन्म के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला चल पड़ता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह की उत्पत्ति होती है।
और रूप का विलुप्त होना क्या है?
कोई व्यक्ति रूप से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता। जब वह रूप से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता, तब उसे मज़ा नहीं आता। रूप का किसी भी तरह मज़ा न लेना आधार ख़त्म करता है। आधार ख़त्म होने के कारण अस्तित्व नहीं पनपता। अस्तित्व न होने के कारण जन्म नहीं होता। जन्म न होने के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला रुक जाता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह विलुप्त हो जाता है।
वेदना…नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता का विलुप्त होना क्या है?
कोई व्यक्ति वेदना…नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता। जब वह वेदना…नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता से आनंदित नहीं होता, स्वीकार नहीं करता, जुड़ नहीं जाता, तब उसे मज़ा नहीं आता। वेदना…नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता का किसी भी तरह मज़ा न लेना आधार ख़त्म करता है। आधार ख़त्म होने के कारण अस्तित्व नहीं पनपता। अस्तित्व न होने के कारण जन्म नहीं होता। जन्म न होने के कारण बुढ़ापा मौत शोक विलाप दर्द व्यथा निराशा का सिलसिला रुक जाता है। इस तरह समस्त दुःख संग्रह विलुप्त हो जाता है।
इस तरह भिक्षुओं, रूप की उत्पत्ति व विलुप्ति होती है। वेदना… नज़रिए… संस्कार… विज्ञानता की उत्पत्ति व विलुप्ति होती है, जिसे समाधि में लीन भिक्षु जैसे हो, वैसे सही पता करता है। इसलिए समाधि विकसित करो, भिक्षुओं। समाधि में लीन भिक्षु जैसे हो, वैसे सही पता करता है।
["सं.नि.२२:५"] ↩︎
पालि
१०५. एवं मे सुतं – एकं समयं भगवा कुरूसु विहरति कम्मासधम्मं नाम कुरूनं निगमो। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि – ‘‘भिक्खवो’’ति। ‘‘भदन्ते’’ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच –
उद्देसो
१०६. ‘‘एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिदेवानं परिद्दवानं (सी॰ पी॰) समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्थङ्गमाय, ञायस्स अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना।
‘‘कतमे चत्तारो? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।
उद्देसो निट्ठितो।
कायानुपस्सना आनापानपब्बं
१०७. ‘‘कथञ्च, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरञ्ञगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्ञागारगतो वा निसीदति, पल्लङ्कं आभुजित्वा, उजुं कायं पणिधाय, परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा। सो सतोव अस्ससति, सतोव सतो (सी॰ स्या॰) पस्ससति। दीघं वा अस्ससन्तो ‘दीघं अस्ससामी’ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो ‘दीघं पस्ससामी’ति पजानाति, रस्सं वा अस्ससन्तो ‘रस्सं अस्ससामी’ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो ‘रस्सं पस्ससामी’ति पजानाति, ‘सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी’ति सिक्खति, ‘सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी’ति सिक्खति , ‘पस्सम्भयं कायसङ्खारं अस्ससिस्सामी’ति सिक्खति, ‘पस्सम्भयं कायसङ्खारं पस्ससिस्सामी’ति सिक्खति।
‘‘सेय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा दीघं वा अञ्छन्तो ‘दीघं अञ्छामी’ति पजानाति, रस्सं वा अञ्छन्तो ‘रस्सं अञ्छामी’ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघं वा अस्ससन्तो ‘दीघं अस्ससामी’ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो ‘दीघं पस्ससामी’ति पजानाति, रस्सं वा अस्ससन्तो ‘रस्सं अस्ससामी’ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो ‘रस्सं पस्ससामी’ति पजानाति; ‘सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी’ति सिक्खति, ‘सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी’ति सिक्खति; ‘पस्सम्भयं कायसङ्खारं अस्ससिस्सामी’ति सिक्खति, ‘पस्सम्भयं कायसङ्खारं पस्ससिस्सामी’ति सिक्खति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति। ‘अत्थि कायो’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो एवम्पि (सी॰ स्या॰ पी॰), भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
आनापानपब्बं निट्ठितं।
कायानुपस्सना इरियापथपब्बं
१०८. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु गच्छन्तो वा ‘गच्छामी’ति पजानाति, ठितो वा ‘ठितोम्ही’ति पजानाति, निसिन्नो वा ‘निसिन्नोम्ही’ति पजानाति, सयानो वा ‘सयानोम्ही’ति पजानाति। यथा यथा वा पनस्स कायो पणिहितो होति तथा तथा नं पजानाति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति। ‘अत्थि कायो’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
इरियापथपब्बं निट्ठितं।
कायानुपस्सना सम्पजानपब्बं
१०९. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
सम्पजानपब्बं निट्ठितं।
कायानुपस्सना पटिकूलमनसिकारपब्बं
११०. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, अधो केसमत्थका, तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति – ‘अत्थि इमस्मिं काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु नहारु (सी॰ स्या॰ पी॰) अट्ठि अट्ठिमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लसिका मुत्त’न्ति मुत्तं मत्थलुङ्गन्ति (क॰)।
‘‘सेय्यथापि, भिक्खवे, उभतोमुखा पुतोळि मूतोळी (सी॰ स्या॰ पी॰) पूरा नानाविहितस्स धञ्ञस्स, सेय्यथिदं – सालीनं वीहीनं मुग्गानं मासानं तिलानं तण्डुलानं। तमेनं चक्खुमा पुरिसो मुञ्चित्वा पच्चवेक्खेय्य – ‘इमे साली इमे वीही इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डुला’ति। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं उद्धं पादतला, अधो केसमत्थका, तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति – ‘अत्थि इमस्मिं काये केसा लोमा…पे॰… मुत्त’न्ति।
‘‘इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
पटिकूलमनसिकारपब्बं निट्ठितं।
कायानुपस्सना धातुमनसिकारपब्बं
१११. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति – ‘अत्थि इमस्मिं काये पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातू’ति।
‘‘सेय्यथापि , भिक्खवे, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गाविं वधित्वा चतुमहापथे चातुम्महापथे (सी॰ स्या॰ पी॰) बिलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्स। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पच्चवेक्खति – ‘अत्थि इमस्मिं काये पथवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातू’ति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे , भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
धातुमनसिकारपब्बं निट्ठितं।
कायानुपस्सना नवसिवथिकपब्बं
११२. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड्डितं एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धुमातकं विनीलकं विपुब्बकजातं। सो इममेव कायं उपसंहरति – ‘अयम्पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो’ति एतं अनतीतोति (सी॰ पी॰)। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड्डितं काकेहि वा खज्जमानं कुललेहि वा खज्जमानं गिज्झेहि वा खज्जमानं कङ्केहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमानं ब्यग्घेहि वा खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिङ्गालेहि वा गिज्झेहि वा खज्जमानं, सुवानेहि वा खज्जमानं, सिगालेहि वा (स्या॰ पी॰) खज्जमानं विविधेहि वा पाणकजातेहि खज्जमानं। सो इममेव कायं उपसंहरति – ‘अयम्पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो’ति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड्डितं अट्ठिकसङ्खलिकं समंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं…पे॰… अट्ठिकसङ्खलिकं निमंसलोहितमक्खितं न्हारुसम्बन्धं…पे॰… अट्ठिकसङ्खलिकं अपगतमंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं…पे॰… अट्ठिकानि अपगतसम्बन्धानि अपगतन्हारुसम्बन्धानि (स्या॰) दिसा विदिसा विक्खित्तानि, अञ्ञेन हत्थट्ठिकं अञ्ञेन पादट्ठिकं अञ्ञेन गोप्फकट्ठिकं ‘‘अञ्ञेन गोप्फकट्ठिक’’न्ति इदं सी॰ स्या॰ पी॰ पोत्थकेसु नत्थि अञ्ञेन जङ्घट्ठिकं अञ्ञेन ऊरुट्ठिकं अञ्ञेन कटिट्ठिकं अञ्ञेन कटट्ठिकं अञ्ञेन पिट्ठट्ठिकं अञ्ञेन कण्टकट्ठिकं अञ्ञेन फासुकट्ठिकं अञ्ञेन उरट्ठिकं अञ्ञेन अंसट्ठिकं अञ्ञेन बाहुट्ठिकं (स्या॰) अञ्ञेन फासुकट्ठिकं अञ्ञेन पिट्ठिट्ठिकं अञ्ञेन खन्धट्ठिकं अञ्ञेन कटट्ठिकं अञ्ञेन पिट्ठट्ठिकं अञ्ञेन कण्टकट्ठिकं अञ्ञेन फासुकट्ठिकं अञ्ञेन उरट्ठिकं अञ्ञेन अंसट्ठिकं अञ्ञेन बाहुट्ठिकं (स्या॰) अञ्ञेन गीवट्ठिकं अञ्ञेन हनुकट्ठिकं अञ्ञेन दन्तट्ठिकं अञ्ञेन सीसकटाहं। सो इममेव कायं उपसंहरति – ‘अयम्पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो’ति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति…पे॰… एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छड्डितं, अट्ठिकानि सेतानि सङ्खवण्णपटिभागानि सङ्खवण्णूपनिभानि (सी॰ स्या॰ पी॰) …पे॰… अट्ठिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि…पे॰… अट्ठिकानि पूतीनि चुण्णकजातानि । सो इममेव कायं उपसंहरति – ‘अयम्पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो’ति। इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति। ‘अत्थि कायो’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति।
नवसिवथिकपब्बं निट्ठितं।
चुद्दसकायानुपस्सना निट्ठिता।
वेदनानुपस्सना
११३. ‘‘कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुखं वा सुखं, दुक्खं, अदुक्खमसुखं (सी॰ स्या॰ पी॰ क॰) वेदनं वेदयमानो ‘सुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; दुक्खं वा सुखं, दुक्खं अदुक्खमसुखं (सी॰ स्या॰ पी॰ क॰) वेदनं वेदयमानो ‘दुक्खं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; अदुक्खमसुखं वा वेदनं वेदयमानो ‘अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो ‘सामिसं सुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो ‘निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; सामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो ‘सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; निरामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो ‘निरामिसं दुक्खं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; सामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो ‘सामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; निरामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो ‘निरामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामी’ति पजानाति; इति अज्झत्तं वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। ‘अत्थि वेदना’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति , न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति।
वेदनानुपस्सना निट्ठिता।
चित्तानुपस्सना
११४. ‘‘कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति? इध, भिक्खवे, भिक्खु सरागं वा चित्तं ‘सरागं चित्त’न्ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं ‘वीतरागं चित्त’न्ति पजानाति; सदोसं वा चित्तं ‘सदोसं चित्त’न्ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं ‘वीतदोसं चित्त’न्ति पजानाति; समोहं वा चित्तं ‘समोहं चित्त’न्ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं ‘वीतमोहं चित्त’न्ति पजानाति; संखित्तं वा चित्तं ‘संखित्तं चित्त’न्ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं ‘विक्खित्तं चित्त’न्ति पजानाति; महग्गतं वा चित्तं ‘महग्गतं चित्त’न्ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं ‘अमहग्गतं चित्त’न्ति पजानाति; सउत्तरं वा चित्तं ‘सउत्तरं चित्त’न्ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं ‘अनुत्तरं चित्त’न्ति पजानाति; समाहितं वा चित्तं ‘समाहितं चित्त’न्ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं ‘असमाहितं चित्त’न्ति पजानाति; विमुत्तं वा चित्तं ‘विमुत्तं चित्त’न्ति पजानाति, अविमुत्तं वा चित्तं ‘अविमुत्तं चित्त’न्ति पजानाति। इति अज्झत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिं विहरति। ‘अत्थि चित्त’न्ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति।
चित्तानुपस्सना निट्ठिता।
धम्मानुपस्सना नीवरणपब्बं
११५. ‘‘कथञ्च, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति? इध, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु। कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु?
‘‘इध , भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं ‘अत्थि मे अज्झत्तं कामच्छन्दो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं ‘नत्थि मे अज्झत्तं कामच्छन्दो’ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं ब्यापादं ‘अत्थि मे अज्झत्तं ब्यापादो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं ब्यापादं ‘नत्थि मे अज्झत्तं ब्यापादो’ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स ब्यापादस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स ब्यापादस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स ब्यापादस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं थीनमिद्धं ‘अत्थि मे अज्झत्तं थीनमिद्ध’न्ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं थीनमिद्धं ‘नत्थि मे अज्झत्तं थीनमिद्ध’न्ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं ‘अत्थि मे अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च’न्ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं ‘नत्थि मे अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्च’न्ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छं ‘अत्थि मे अज्झत्तं विचिकिच्छा’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छं ‘नत्थि मे अज्झत्तं विचिकिच्छा’ति पजानाति; यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति , समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। ‘अत्थि धम्मा’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नीवरणेसु।
नीवरणपब्बं निट्ठितं।
धम्मानुपस्सना खन्धपब्बं
११६. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु। कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु? इध, भिक्खवे, भिक्खु – ‘इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो; इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अत्थङ्गमो; इति सञ्ञा, इति सञ्ञाय समुदयो, इति सञ्ञाय अत्थङ्गमो; इति सङ्खारा, इति सङ्खारानं समुदयो, इति सङ्खारानं अत्थङ्गमो; इति विञ्ञाणं, इति विञ्ञाणस्स समुदयो, इति विञ्ञाणस्स अत्थङ्गमो’ति; इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। ‘अत्थि धम्मा’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु।
खन्धपब्बं निट्ठितं।
धम्मानुपस्सना आयतनपब्बं
११७. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु। कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु?
‘‘इध , भिक्खवे, भिक्खु चक्खुञ्च पजानाति, रूपे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘सोतञ्च पजानाति, सद्दे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘घानञ्च पजानाति, गन्धे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘जिव्हञ्च पजानाति, रसे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘कायञ्च पजानाति, फोट्ठब्बे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘मनञ्च पजानाति, धम्मे च पजानाति, यञ्च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तञ्च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयतिं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।
‘‘इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। ‘अत्थि धम्मा’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्झत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु।
आयतनपब्बं निट्ठितं।
धम्मानुपस्सना बोज्झङ्गपब्बं
११८. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्झङ्गेसु। कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्झङ्गेसु? इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अज्झत्तं सतिसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं सतिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं सतिसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं सतिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं धम्मविचयसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं धम्मविचयसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं वीरियसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं वीरियसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं वीरियसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं वीरियसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स वीरियसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स वीरियसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति , यथा च अनुप्पन्नस्स पीतिसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं समाधिसम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति।
‘‘सन्तं वा अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गं ‘अत्थि मे अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गं ‘नत्थि मे अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गो’ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति ।
‘‘इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। ‘अत्थि धम्मा’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज्झङ्गेसु।
बोज्झङ्गपब्बं निट्ठितं बोज्झङ्गपब्बं निट्ठितं। पठमभाणवारं (स्या॰)।
धम्मानुपस्सना सच्चपब्बं
११९. ‘‘पुन चपरं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु अरियसच्चेसु। कथञ्च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु अरियसच्चेसु? इध, भिक्खवे, भिक्खु ‘इदं दुक्ख’न्ति यथाभूतं पजानाति, ‘अयं दुक्खसमुदयो’ति यथाभूतं पजानाति, ‘अयं दुक्खनिरोधो’ति यथाभूतं पजानाति, ‘अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा’ति यथाभूतं पजानाति।
पठमभाणवारो निट्ठितो।
दुक्खसच्चनिद्देसो
१२०. ‘‘कतमञ्च , भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं? जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, मरणम्पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासापि दुक्खा, अप्पियेहि सम्पयोगोपि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगोपि दुक्खो ‘‘अप्पियेहि…पे॰… विप्पयोगोपि दुक्खो’’ति पाठो चेव तंनिद्देसो च सी॰ पी॰ पोत्थकेसु न दिस्सति, सुमङ्गलविलासिनियंपि तंसंवण्णना नत्थि, यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा पञ्चुपादानक्खन्धापि (क॰) दुक्खा।
१२१. ‘‘कतमा च, भिक्खवे, जाति? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति ओक्कन्ति अभिनिब्बत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिलाभो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, जाति।
१२२. ‘‘कतमा च, भिक्खवे, जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको, अयं वुच्चति, भिक्खवे, जरा।
१२३. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, मरणं? यं सुमङ्गलविलासिनी ओलोकेतब्बा तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालङ्किरिया खन्धानं भेदो कळेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो, इदं वुच्चति, भिक्खवे, मरणं।
१२४. ‘‘कतमो च, भिक्खवे, सोको? यो खो, भिक्खवे, अञ्ञतरञ्ञतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्ञतरञ्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स सोको सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको, अयं वुच्चति, भिक्खवे, सोको।
१२५. ‘‘कतमो च, भिक्खवे, परिदेवो? यो खो, भिक्खवे, अञ्ञतरञ्ञतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्ञतरञ्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं, अयं वुच्चति, भिक्खवे, परिदेवो।
१२६. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, दुक्खं? यं खो, भिक्खवे, कायिकं दुक्खं कायिकं असातं कायसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं, इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं।
१२७. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, दोमनस्सं? यं खो, भिक्खवे, चेतसिकं दुक्खं चेतसिकं असातं मनोसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं, इदं वुच्चति, भिक्खवे, दोमनस्सं।
१२८. ‘‘कतमो च, भिक्खवे, उपायासो? यो खो, भिक्खवे, अञ्ञतरञ्ञतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्ञतरञ्ञतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स आयासो उपायासो आयासितत्तं उपायासितत्तं, अयं वुच्चति, भिक्खवे, उपायासो।
१२९. ‘‘कतमो च, भिक्खवे, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो? इध यस्स ते होन्ति अनिट्ठा अकन्ता अमनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अनत्थकामा अहितकामा अफासुककामा अयोगक्खेमकामा, या तेहि सद्धिं सङ्गति समागमो समोधानं मिस्सीभावो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो।
१३०. ‘‘कतमो च, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो? इध यस्स ते होन्ति इट्ठा कन्ता मनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा मित्ता वा अमच्चा वा ञातिसालोहिता वा, या तेहि सद्धिं असङ्गति असमागमो असमोधानं अमिस्सीभावो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो।
१३१. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं? जातिधम्मानं, भिक्खवे , सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति – ‘अहो वत मयं न जातिधम्मा अस्साम, न च वत नो जाति आगच्छेय्या’ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं, इदम्पि यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं। जराधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति – ‘अहो वत मयं न जराधम्मा अस्साम, न च वत नो जरा आगच्छेय्या’ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं, इदम्पि यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं। ब्याधिधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति – ‘अहो वत मयं न ब्याधिधम्मा अस्साम, न च वत नो ब्याधि आगच्छेय्या’ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं, इदम्पि यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं। मरणधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति – ‘अहो वत मयं न मरणधम्मा अस्साम, न च वत नो मरणं आगच्छेय्या’ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं, इदम्पि यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं। सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मानं, भिक्खवे, सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जति – ‘अहो वत मयं न सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा अस्साम, न च वत नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा आगच्छेय्यु’न्ति। न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं, इदम्पि यम्पिच्छं न लभति तम्पि दुक्खं।
१३२. ‘‘कतमे च, भिक्खवे, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा? सेय्यथिदं – रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सङ्खारुपादानक्खन्धो, विञ्ञाणुपादानक्खन्धो। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं।
समुदयसच्चनिद्देसो
१३३. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं दुक्खसमुदयो (स्या॰) अरियसच्चं? यायं तण्हा पोनोब्भविका पोनोभविका (सी॰ पी॰) नन्दीरागसहगता नन्दिरागसहगता (सी॰ स्या॰ पी॰) तत्रतत्राभिनन्दिनी। सेय्यथिदं – कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा।
‘‘सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कत्थ उप्पज्जमाना उप्पज्जति, कत्थ निविसमाना निविसति? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं? चक्खु लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति। सोतं लोके…पे॰… घानं लोके… जिव्हा लोके… कायो लोके… मनो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपा लोके… सद्दा लोके… गन्धा लोके… रसा लोके… फोट्ठब्बा लोके… धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘चक्खुविञ्ञाणं लोके… सोतविञ्ञाणं लोके… घानविञ्ञाणं लोके… जिव्हाविञ्ञाणं लोके… कायविञ्ञाणं लोके… मनोविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘चक्खुसम्फस्सो लोके… सोतसम्फस्सो लोके… घानसम्फस्सो लोके… जिव्हासम्फस्सो लोके… कायसम्फस्सो लोके… मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके… सोतसम्फस्सजा वेदना लोके… घानसम्फस्सजा वेदना लोके… जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके… कायसम्फस्सजा वेदना लोके… मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपसञ्ञा लोके… सद्दसञ्ञा लोके… गन्धसञ्ञा लोके… रससञ्ञा लोके… फोट्ठब्बसञ्ञा लोके… धम्मसञ्ञा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपसञ्चेतना लोके… सद्दसञ्चेतना लोके… गन्धसञ्चेतना लोके… रससञ्चेतना लोके… फोट्ठब्बसञ्चेतना लोके… धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपतण्हा लोके… सद्दतण्हा लोके… गन्धतण्हा लोके… रसतण्हा लोके… फोट्ठब्बतण्हा लोके… धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपवितक्को लोके… सद्दवितक्को लोके… गन्धवितक्को लोके… रसवितक्को लोके… फोट्ठब्बवितक्को लोके… धम्मवितक्को लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति।
‘‘रूपविचारो लोके… सद्दविचारो लोके… गन्धविचारो लोके… रसविचारो लोके… फोट्ठब्बविचारो लोके… धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं।
निरोधसच्चनिद्देसो
१३४. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधं दुक्खनिरोधो (स्या॰) अरियसच्चं? यो तस्सायेव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो।
‘‘सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं? चक्खु लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति। सोतं लोके…पे॰… घानं लोके… जिव्हा लोके… कायो लोके… मनो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपा लोके… सद्दा लोके… गन्धा लोके… रसा लोके… फोट्ठब्बा लोके… धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘चक्खुविञ्ञाणं लोके… सोतविञ्ञाणं लोके… घानविञ्ञाणं लोके… जिव्हाविञ्ञाणं लोके… कायविञ्ञाणं लोके… मनोविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘चक्खुसम्फस्सो लोके… सोतसम्फस्सो लोके… घानसम्फस्सो लोके… जिव्हासम्फस्सो लोके… कायसम्फस्सो लोके… मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके… सोतसम्फस्सजा वेदना लोके… घानसम्फस्सजा वेदना लोके… जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके… कायसम्फस्सजा वेदना लोके… मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपसञ्ञा लोके… सद्दसञ्ञा लोके… गन्धसञ्ञा लोके… रससञ्ञा लोके… फोट्ठब्बसञ्ञा लोके… धम्मसञ्ञा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपसञ्चेतना लोके… सद्दसञ्चेतना लोके… गन्धसञ्चेतना लोके… रससञ्चेतना लोके… फोट्ठब्बसञ्चेतना लोके… धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपतण्हा लोके… सद्दतण्हा लोके… गन्धतण्हा लोके… रसतण्हा लोके… फोट्ठब्बतण्हा लोके… धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपवितक्को लोके… सद्दवितक्को लोके… गन्धवितक्को लोके… रसवितक्को लोके… फोट्ठब्बवितक्को लोके… धम्मवितक्को लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।
‘‘रूपविचारो लोके… सद्दविचारो लोके… गन्धविचारो लोके… रसविचारो लोके… फोट्ठब्बविचारो लोके… धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झामाना निरुज्झति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खनिरोधं अरियसच्चं।
मग्गसच्चनिद्देसो
१३५. ‘‘कतमञ्च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं? अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो सेय्यथिदं – सम्मादिट्ठि सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि।
‘‘कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि? यं खो, भिक्खवे, दुक्खे ञाणं, दुक्खसमुदये ञाणं, दुक्खनिरोधे ञाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि।
‘‘कतमो च, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो? नेक्खम्मसङ्कप्पो अब्यापादसङ्कप्पो अविहिंसासङ्कप्पो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो।
‘‘कतमा च, भिक्खवे, सम्मावाचा? मुसावादा वेरमणी वेरमणि (क॰), पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी । अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावाचा।
‘‘कतमो च, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो।
‘‘कतमो च, भिक्खवे, सम्माआजीवो? इध, भिक्खवे, अरियसावको मिच्छाआजीवं पहाय सम्माआजीवेन जीवितं कप्पेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्माआजीवो।
‘‘कतमो च, भिक्खवे, सम्मावायामो? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति वीरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति वीरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति वीरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति वीरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावायामो।
‘‘कतमा च, भिक्खवे, सम्मासति? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासति।
‘‘कतमो च, भिक्खवे, सम्मासमाधि? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति ‘उपेक्खको सतिमा सुखविहारी’ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासमाधि। इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं।
१३६. ‘‘इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति; समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति। ‘अत्थि धम्मा’ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति। यावदेव ञाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति। एवम्पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु अरियसच्चेसु।
सच्चपब्बं निट्ठितं।
धम्मानुपस्सना निट्ठिता।
१३७. ‘‘यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य सत्त वस्सानि, तस्स द्विन्नं फलानं अञ्ञतरं फलं पाटिकङ्खं दिट्ठेव धम्मे अञ्ञा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता।
‘‘तिट्ठन्तु, भिक्खवे, सत्त वस्सानि। यो हि कोचि , भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य छ वस्सानि…पे॰… पञ्च वस्सानि… चत्तारि वस्सानि… तीणि वस्सानि… द्वे वस्सानि… एकं वस्सं… तिट्ठतु, भिक्खवे, एकं वस्सं। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य सत्त मासानि, तस्स द्विन्नं फलानं अञ्ञतरं फलं पाटिकङ्खं दिट्ठेव धम्मे अञ्ञा; सति वा उपादिसेसे अनागामिता। तिट्ठन्तु, भिक्खवे, सत्त मासानि। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य छ मासानि…पे॰… पञ्च मासानि… चत्तारि मासानि… तीणि मासानि… द्वे मासानि… एकं मासं… अड्ढमासं… तिट्ठतु, भिक्खवे, अड्ढमासो। यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भावेय्य सत्ताहं, तस्स द्विन्नं फलानं अञ्ञतरं फलं पाटिकङ्खं दिट्ठेव धम्मे अञ्ञा सति वा उपादिसेसे अनागामिता’’ति।
१३८. ‘‘‘एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समतिक्कमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्थङ्गमाय ञायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना’ति। इति यं तं वुत्तं, इदमेतं पटिच्च वुत्त’’न्ति।
इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुन्ति।
महासतिपट्ठानसुत्तं निट्ठितं दसमं।
मूलपरियायवग्गो निट्ठितो पठमो।