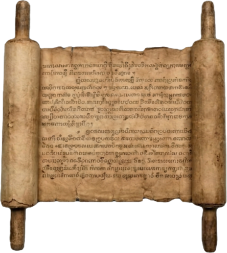
पुर्णिमा की रात
हिन्दी
ऐसा मैंने सुना — एक समय भगवान श्रावस्ती में मिगारमाता के विहार 1 पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान उपोसथ की पंचदशी पुर्णिमा की रात को भिक्षुसंघ से घिरकर खुले आकाश के नीचे बैठे थे।
तब कोई भिक्षु अपने आसन से उठा, और चीवर को एक कंधे पर कर, भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, भगवान से कहा, “भन्ते, मैं भगवान से कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि भगवान मुझे मौका देकर प्रश्न पर उत्तर दें।” 2
“ठीक है, भिक्षु। अपने आसन पर बैठकर, जो शंका हो पूछो।”
पञ्चुपादानक्खन्ध
“भन्ते, क्या पाँच आसक्ति संग्रह (“उपादानक्खन्ध”) ये हैं—रूप आसक्ति संग्रह, वेदना (“वेदना”) आसक्ति संग्रह, संज्ञा आसक्ति संग्रह, संस्कार (=संस्कार) आसक्ति संग्रह, विज्ञान आसक्ति संग्रह?”
“हाँ, भिक्षु। ये ही पाँच आसक्ति संग्रह हैं—रूप आसक्ति संग्रह, वेदना आसक्ति संग्रह, संज्ञा आसक्ति संग्रह, संस्कार आसक्ति संग्रह, विज्ञान आसक्ति संग्रह।”
“साधु (=बहुत अच्छा), भन्ते।” कहते हुए हर्षित हुए भिक्षु ने भगवान के कहे का अभिनंदन किया, और फिर भगवान से अगला प्रश्न पूछा 3—
मूल
“किन्तु, भन्ते, इन पाँच आसक्ति संग्रह की जड़ (“मूल”) क्या है?”
“भिक्षु, इन पाँच आसक्ति संग्रह की जड़ चाहत (“छन्द” =कामना) है”
“किन्तु, भन्ते, क्या आसक्ति ही पाँच आसक्ति संग्रह है, अथवा पाँच आसक्ति संग्रह अलग है, और आसक्ति अलग?”
“(दोनों ही) नहीं, भिक्षु। न आसक्ति ही ‘पाँच आसक्ति संग्रह’ है, न ‘पाँच आसक्ति संग्रह’ अलग और आसक्ति अलग हैं। बल्कि, पाँच आसक्ति संग्रह के प्रति जो चाहत और दिलचस्पी (“छन्दराग”) है, वही आसक्ति है।”
विविधता
“किन्तु, भन्ते, क्या पाँच आसक्ति संग्रह के प्रति चाहत और दिलचस्पी में भिन्नता (या विविधता) हो सकती हैं?”
“हो सकती है, भिक्षु।” भगवान ने कहा। “जब किसी भिक्षु को लगता है कि ‘भविष्य में मेरा ऐसा रूप हो जाए, ऐसी वेदना हो जाए, ऐसी संज्ञा हो जाए, ऐसी संस्कार हो जाए, ऐसा विज्ञान हो जाए!’ इस प्रकार, भिक्षु, पाँच आसक्ति संग्रह के प्रति चाहत और दिलचस्पी में भिन्नता हो सकती है।”
संग्रह की परिभाषा
“भन्ते, यह ‘संग्रह’ (“खन्ध”) शब्द किस हद तक उपयोग होता है?”
- “भिक्षु, जो भी रूप हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप के—वे रूप संग्रह हैं।
- जो भी वेदना हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप की—वे वेदना संग्रह हैं।
- जो भी संज्ञा हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप की—वे संज्ञा संग्रह हैं।
- जो भी संस्कार हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप की—वे संस्कार संग्रह हैं।
- जो भी विज्ञान हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का—वे विज्ञान संग्रह हैं।
—इस हद तक, भिक्षु, ‘संग्रह’ शब्द उपयोग होता है।”
हेतु पच्चय
“भन्ते, किस कारण, किस परिस्थिति में रूप संग्रह प्रकट होता है? और, भन्ते, किस कारण, किस परिस्थिति में वेदना संग्रह… संज्ञा संग्रह… संस्कार संग्रह… विज्ञान संग्रह प्रकट होते हैं?”
- “चार महाभूत के कारण, भिक्षु, चार महाभूत की परिस्थिती में रूप संग्रह विद्यमान होता है।
- (इंद्रिय) संपर्क के कारण, संपर्क की परिस्थिति में वेदना संग्रह प्रकट होता है।
- संपर्क के (ही) कारण, संपर्क की परिस्थिति में संज्ञा संग्रह (भी) प्रकट होता है।
- संपर्क के (ही) कारण, संपर्क की परिस्थिति में संस्कार संग्रह (भी) प्रकट होता है। 4
- नाम-रूप के कारण, भिक्षु, नाम-रूप की परिस्थिति में विज्ञान संग्रह प्रकट होता है। 5”
सक्कायदिट्ठी
“भन्ते, यह स्व-धारणा दृष्टि क्या है?”
“भिक्षु, कोई धम्म न सुना, आम आदमी हो, जो आर्यजनों के दर्शन से वंचित, आर्य-धम्म से अपरिचित, आर्य-धम्म में अनुशासित न हो; या सत्पुरुषों के दर्शन से वंचित, सत्पुरूष-धम्म से अपरिचित, सत्पुरूष-धम्म में अनुशासित न हो—
- वह रूप को आत्मा मानता है, या आत्मा को रूपवान मानता है, या आत्मा में रूप देखता है, या रूप में आत्मा देखता है।
- वह वेदना को आत्मा मानता है…
- वह संज्ञा को आत्मा मानता है…
- वह संस्कार को आत्मा मानता है…
- वह विज्ञान को आत्मा मानता है, या आत्मा को विज्ञानवान मानता है, या आत्मा में विज्ञान देखता है, या विज्ञान में आत्मा देखता है।
—इस तरह, भिक्षु, स्व-धारणा दृष्टि होती है।”
“किन्तु, भगवान, स्व-धारणा दृष्टि कैसे नहीं होती?”
“भिक्षु, कोई धम्म सुना आर्यश्रावक हो, जो आर्यजनों के दर्शन से लाभान्वित, आर्य-धम्म से परिचित, आर्य-धम्म में अनुशासित हो; या सत्पुरुषों के दर्शन से लाभान्वित, सत्पुरूष-धम्म से परिचित, सत्पुरूष-धम्म में अनुशासित हो—
- वह रूप को आत्मा नहीं मानता है, या आत्मा को रूपवान नहीं मानता है, या आत्मा में रूप नहीं देखता है, या रूप में आत्मा नहीं देखता है।
- वह वेदना को आत्मा नहीं मानता है…
- वह संज्ञा को आत्मा नहीं मानता है…
- वह संस्कार को आत्मा नहीं मानता है…
- वह विज्ञान को आत्मा नहीं मानता है, या आत्मा को विज्ञानवान नहीं मानता है, या आत्मा में विज्ञान नहीं देखता है, या विज्ञान में आत्मा नहीं देखता है।
—इस तरह, भिक्षु, स्व-धारणा दृष्टि नहीं होती है।”
अस्साद आदीनव निस्सरण
“भन्ते, रूप का प्रलोभन (या आकर्षण) क्या है, खामी (या दुष्परिणाम) क्या है, निकलने का मार्ग क्या है? और, भन्ते, वेदना… संज्ञा… संस्कार… विज्ञान का प्रलोभन क्या है, खामी क्या है, निकलने का मार्ग क्या है?”
- “रूप के आधार पर, भिक्षु, जो भी सुख और खुशी उत्पन्न होती है, वही रूप का प्रलोभन है।
- रूप अनित्य, दुःखदायी, और परिवर्तनशील है, वही रूप की खामी है।
- रूप के प्रति चाहत व दिलचस्पी हटाना, चाहत व दिलचस्पी त्यागना, वही रूप से निकलने का मार्ग है।
- वेदना के आधार पर जो भी सुख और खुशी…
- …
- संज्ञा के आधार पर…
- …
- संस्कार के आधार पर…
- …
- विज्ञान के आधार पर जो भी सुख और खुशी उत्पन्न होती है, वही विज्ञान का प्रलोभन है।
- विज्ञान अनित्य, दुःखदायी, और परिवर्तनशील है, वही विज्ञान की खामी है।
- विज्ञान के प्रति चाहत व दिलचस्पी हटाना, चाहत व दिलचस्पी त्यागना, वही विज्ञान से निकलने का मार्ग है।”
मैं/मेरा
“भन्ते, कोई किस प्रकार जानता है, किस प्रकार देखता है, ताकि इस विज्ञानपूर्ण काया और बाहरी सभी छवियों (“निमित्त”) के प्रति मैं/मेरे (“अहङ्कारममङ्कार”) का अहंभाव अनुशय 6 न हो?”
“भिक्षु, जो भी रूप हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का। सभी रूपों को यह ‘मेरे नहीं हैं, मेरा आत्म नहीं हैं, मैं यह नहीं हूँ’, इस तरह, सम्यक अन्तर्ज्ञान से यथास्वरूप देखना है।
जो भी वेदना हो… जो भी संज्ञा हो… जो भी संस्कार हो… जो भी विज्ञान हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का। सभी विज्ञान को यह ‘मेरे नहीं हैं, मेरा आत्म नहीं हैं, मैं यह नहीं हूँ’, इस तरह, सम्यक अन्तर्ज्ञान से यथास्वरूप देखना है।
इस प्रकार, भिक्षु, कोई जानता है, इस प्रकार देखता है, ताकि इस विज्ञानपूर्ण काया और बाहरी सभी छवियों के प्रति मैं/मेरे का अहंभाव अनुशय नहीं होता।”
बहके मन के विचार
तभी किसी दूसरे भिक्षु के मानस में ऐसे विचार उत्पन्न हुए, “तो लगता है, श्रीमान, रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, संस्कार अनात्म है, विज्ञान अनात्म है। तब अनात्म के किए कर्म किस आत्मा को छूते हैं?”
तब भगवान ने उस भिक्षु के मानस में चल रहे विचारों को अपने मानस से जानकर, उस भिक्षु को आमंत्रित किया, “ऐसा संभव है, भिक्षुओं, कि यहाँ किसी न जानने वाले, अविद्या में पड़े, तृष्णा से अभिभूत चित्त के निकम्मे पुरुष को ऐसा लगे कि वह शास्ता के शासन (शिक्षा) को मात दी जा सकती है, ‘तो लगता है, श्रीमान, रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, संज्ञा अनात्म है, संस्कार अनात्म है, विज्ञान अनात्म है। तब अनात्म के किए कर्म किस आत्मा को छूते हैं?’
भिक्षुओं, मैंने तुम्हें उन-उन धम्मों में (प्रतिप्रश्न करने का) प्रशिक्षण दिया हैं। क्या लगता है, भिक्षुओं, रूप नित्य है या अनित्य?”
“अनित्य, भन्ते।”
“जो नित्य नहीं, वह कष्टदायी है या सुखदायी?”
“कष्टदायी, भन्ते।”
“जो नित्य नहीं, कष्टदायी है, परिवर्तनशील है, क्या उसे इस तरह देखना योग्य है कि ‘यह मेरा है, यह मेरा आत्म है, यही तो मैं हूँ’?”
“नहीं, भन्ते।”
“वेदना नित्य है या अनित्य?… संज्ञा नित्य है या अनित्य?… संस्कार नित्य है या अनित्य?… विज्ञान नित्य है या अनित्य?”
“अनित्य, भन्ते।”
“जो नित्य नहीं, वह कष्टदायी है या सुखदायी?”
“कष्टदायी, भन्ते।”
“जो नित्य नहीं, कष्टदायी है, परिवर्तनशील है, क्या उसे इस तरह देखना योग्य है कि ‘यह मेरा है, यह मेरा आत्म है, यही तो मैं हूँ’?”
“नहीं, भन्ते।”
“इसलिए, भिक्षुओं, जो भी रूप हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का। सभी रूपों को यह ‘मेरे नहीं हैं, मेरा आत्म नहीं हैं, मैं यह नहीं हूँ’, इस तरह, सम्यक अन्तर्ज्ञान से यथास्वरूप देखना है।
जो भी वेदना हो… जो भी संज्ञा हो… जो भी संस्कार हो… जो भी विज्ञान हो—भूत, भविष्य या वर्तमान के, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या उत्तम, दूर या समीप का। सभी विज्ञान को यह ‘मेरे नहीं हैं, मेरा आत्म नहीं हैं, मैं यह नहीं हूँ’, इस तरह, सम्यक अन्तर्ज्ञान से यथास्वरूप देखना है।
भिक्षुओं, इस तरह देखने से धम्म-सुने आर्यश्रावक का रूप के प्रति मोहभंग होता है, वेदना के प्रति मोहभंग होता है, संज्ञा के प्रति मोहभंग होता है, संस्कार के प्रति मोहभंग होता है, विज्ञान के प्रति मोहभंग होता है।
मोहभंग होने से विराग होता है। विराग होने से विमुक्त होता है। विमुक्ति से ज्ञात होता है, ‘विमुक्त हुआ!’ और पता चलता है, ‘जन्म समाप्त हुए! ब्रह्मचर्य परिपूर्ण हुआ! काम पुरा हुआ! अभी यहाँ करने के लिए कुछ बचा नहीं!’”
भगवान ने ऐसा कहा। हर्षित होकर भिक्षुओं ने भगवान की बात का अभिनंदन किया। और जब यह स्पष्टीकरण बोला जा रहा था, तब साठ भिक्षुओं का चित्त अनासक्त होकर आस्रवों से विमुक्त हुआ।
सुत्र समाप्त।
-
जेतवन के पश्चात् श्रावस्ती का दूसरा सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विहार पूर्वाराम था, जिसे “मिगारमातुपसाद”, अर्थात मिगारमाता का महल, भी कहा जाता था। यह विहार जेतवन के मुख्य द्वार से पूर्व दिशा में, लगभग २ किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। शांत वातावरण में स्थित यह स्थान बुद्ध के निवास और उपदेश के लिए उपयुक्त था, जहाँ उन्होंने कई बार वर्षावास भी किया।
इस विहार का निर्माण महाउपासिका विशाखा ने कराया था, जो बुद्धकाल की महानतम दायकों में मानी जाती हैं। विशाखा को “मिगार की माँ” के नाम से जाना जाता है। यह नामकरण साधारण नहीं था—मिगार, जो उसका ससुर था, उसे विशाखा ने धम्म में प्रवृत्त किया और उसे उपासक बनाया। इस धार्मिक उत्थान के कारण, यद्यपि वह सांसारिक दृष्टि से उसकी बहू थी, धम्म की दृष्टि से वह उसकी ‘माँ’ बन गई। ↩︎
-
अट्ठकथा के अनुसार, यह भिक्षु वास्तव में अपने अनेक शिष्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से ये प्रश्न पूछ रहा था। संभव है कि यह संदर्भ सही हो, क्योंकि उसके प्रश्न अत्यंत सधे हुए और स्पष्ट रूप से ध्येयपूर्ण प्रतीत होते हैं। ↩︎
-
आगे इस प्रतिक्रियात्मक वाक्य को छोड़ दिया गया है। किंतु इस सूत्र के सभी समानांतर रूपों में यह भगवान के प्रत्येक उत्तर के पश्चात दोहराया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वह भिक्षु भगवान के हर उत्तर पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता है और तत्पश्चात अगला प्रश्न दागता है। ↩︎
-
वेदना और संज्ञा आपस में बहुत क़रीबी तौर पर जुड़ी होती हैं। हम जैसा महसूस करते हैं, प्रायः उसी ढंग से उसे पहचानते और समझते हैं। जैसे ही कोई इंद्रिय-संपर्क होता है, वैसे ही वेदना जन्म लेती है और साथ-साथ संज्ञा भी उभर आती है। इसके बाद हम उस पर संस्कार, यानी “संस्कार”, के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी पेड़ से बेर तोड़कर “चखते” हैं। उसके बेहद कड़वे स्वाद से जीभ का “संपर्क” होता है, अनुभव “अप्रिय” लगता है; तुरंत ही हम उसे “बेकार” मान लेते हैं (संज्ञा), और फिर उसे “थूक” देने का चुनाव करते हैं (संस्कार)। ↩︎
-
नाम-रूप के बारे में जानने के लिए हमारी शब्दावली पढ़ें। ↩︎
-
अनुशय के बारे में जानने के लिए हमारी शब्दावली अवश्य पढ़ें। ↩︎
पालि
८५. एवं मे सुतं – एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे पन्नरसे पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया भिक्खुसङ्घपरिवुतो अब्भोकासे निसिन्नो होति। अथ खो अञ्ञतरो भिक्खु उट्ठायासना एकंसं चीवरं कत्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच –
‘‘पुच्छेय्याहं, भन्ते, भगवन्तं किञ्चिदेव देसं, सचे मे भगवा ओकासं करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया’’ति। ‘‘तेन हि त्वं, भिक्खु, सके आसने निसीदित्वा पुच्छ यदाकङ्खसी’’ति।
८६. अथ खो सो भिक्खु सके आसने निसीदित्वा भगवन्तं एतदवोच – ‘‘इमे नु खो, भन्ते, पञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथिदं – रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सङ्खारुपादानक्खन्धो, विञ्ञाणुपादानक्खन्धो’’ति? ‘‘इमे खो, भिक्खु, पञ्चुपादानक्खन्धा, सेय्यथिदं – रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्ञुपादानक्खन्धो, सङ्खारुपादानक्खन्धो, विञ्ञाणुपादानक्खन्धो’’ति।
‘‘साधु, भन्ते’’ति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरिं पञ्हं पुच्छि – ‘‘इमे पन, भन्ते, पञ्चुपादानक्खन्धा किंमूलका’’ति? ‘‘इमे खो, भिक्खु, पञ्चुपादानक्खन्धा छन्दमूलका’’ति। ‘‘तंयेव नु खो, भन्ते, उपादानं ते पञ्चुपादानक्खन्धा, उदाहु अञ्ञत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादान’’न्ति? ‘‘न खो, भिक्खु, तंयेव उपादानं ते पञ्चुपादानक्खन्धा, नापि अञ्ञत्र पञ्चहुपादानक्खन्धेहि उपादानं। यो खो, भिक्खु, पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरागो तं तत्थ उपादान’’न्ति।
‘‘सिया पन, भन्ते, पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरागवेमत्तता’’ति? ‘‘सिया भिक्खू’’ति भगवा अवोच ‘‘इध, भिक्खु, एकच्चस्स एवं होति – ‘एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं , एवंवेदनो सियं अनागतमद्धानं, एवंसञ्ञो सियं अनागतमद्धानं, एवंसङ्खारो सियं अनागतमद्धानं, एवंविञ्ञाणो सियं अनागतमद्धान’न्ति। एवं खो, भिक्खु, सिया पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु छन्दरागवेमत्तता’’ति।
‘‘कित्तावता पन, भन्ते, खन्धानं खन्धाधिवचनं होती’’ति? ‘‘यं किञ्चि, भिक्खु, रूपं – अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, ओळारिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वा, यं दूरे सन्तिके वा – अयं रूपक्खन्धो। या काचि वेदना – अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, ओळारिका वा सुखुमा वा, हीना वा पणीता वा, या दूरे सन्तिके वा – अयं वेदनाक्खन्धो। या काचि सञ्ञा – अतीतानागतपच्चुप्पन्ना…पे॰… या दूरे सन्तिके वा – अयं सञ्ञाक्खन्धो। ये केचि सङ्खारा – अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, ओळारिका वा सुखुमा वा, हीना वा पणीता वा, ये दूरे सन्तिके वा – अयं सङ्खारक्खन्धो। यं किञ्चि विञ्ञाणं – अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा, ओळारिकं वा सुखुमं वा, हीनं वा पणीतं वा, यं दूरे सन्तिके वा – अयं विञ्ञाणक्खन्धो। एत्तावता खो, भिक्खु, खन्धानं खन्धाधिवचनं होती’’ति।
‘‘को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो रूपक्खन्धस्स पञ्ञापनाय? को हेतु को पच्चयो वेदनाक्खन्धस्स पञ्ञापनाय? को हेतु को पच्चयो सञ्ञाक्खन्धस्स पञ्ञापनाय? को हेतु को पच्चयो सङ्खारक्खन्धस्स पञ्ञापनाय? को हेतु को पच्चयो विञ्ञाणक्खन्धस्स पञ्ञापनाया’’ति?
‘‘चत्तारो खो, भिक्खु, महाभूता हेतु, चत्तारो महाभूता पच्चयो रूपक्खन्धस्स पञ्ञापनाय। फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो वेदनाक्खन्धस्स पञ्ञापनाय। फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो सञ्ञाक्खन्धस्स पञ्ञापनाय। फस्सो हेतु, फस्सो पच्चयो सङ्खारक्खन्धस्स पञ्ञापनाय। नामरूपं खो, भिक्खु, हेतु, नामरूपं पच्चयो विञ्ञाणक्खन्धस्स पञ्ञापनाया’’ति।
८७. ‘‘कथं पन, भन्ते, सक्कायदिट्ठि होती’’ति? ‘‘इध, भिक्खु, अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं रूपस्मिं वा अत्तानं; वेदनं अत्ततो समनुपस्सति वेदनावन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा वेदनं वेदनाय वा अत्तानं; सञ्ञं अत्ततो समनुपस्सति सञ्ञावन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा सञ्ञं सञ्ञाय वा अत्तानं; सङ्खारे अत्ततो समनुपस्सति सङ्खारवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा सङ्खारे सङ्खारेसु वा अत्तानं; विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा विञ्ञाणं विञ्ञाणस्मिं वा अत्तानं। एवं खो , भिक्खु, सक्कायदिट्ठि होती’’ति।
‘‘कथं पन, भन्ते, सक्कायदिट्ठि न होती’’ति? ‘‘इध, भिक्खु, सुतवा अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति न रूपवन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा रूपं न रूपस्मिं वा अत्तानं; न वेदनं अत्ततो समनुपस्सति न वेदनावन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा वेदनं न वेदनाय वा अत्तानं; न सञ्ञं अत्ततो समनुपस्सति न सञ्ञावन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा सञ्ञं न सञ्ञाय वा अत्तानं; न सङ्खारे अत्ततो समनुपस्सति न सङ्खारवन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा सङ्खारे न सङ्खारेसु वा अत्तानं; न विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति न विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं न अत्तनि वा विञ्ञाणं न विञ्ञाणस्मिं वा अत्तानं। एवं खो, भिक्खु, सक्कायदिट्ठि न होती’’ति।
८८. ‘‘को नु खो, भन्ते, रूपे अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं? को सञ्ञाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं? को सङ्खारेसु अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं? को विञ्ञाणे अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरण’’न्ति? ‘‘यं खो, भिक्खु, रूपं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं रूपे अस्सादो। यं रूपं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं रूपे आदीनवो। यो रूपे छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं रूपे निस्सरणं। यं खो यञ्च (स्या॰ कं॰), भिक्खु, वेदनं पटिच्च… सञ्ञं पटिच्च… सङ्खारे पटिच्च… विञ्ञाणं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं विञ्ञाणे अस्सादो। यं विञ्ञाणं अनिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं विञ्ञाणे आदीनवो। यो विञ्ञाणे छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं विञ्ञाणे निस्सरण’’न्ति।
८९. ‘‘कथं पन, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो इमस्मिञ्च सविञ्ञाणके काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहंकारममंकारमानानुसया न होन्ती’’ति? ‘‘यं किञ्चि, भिक्खु, रूपं – अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा – सब्बं रूपं ‘नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता’ति – एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। या काचि वेदना… या काचि सञ्ञा… ये केचि सङ्खारा… यं किञ्चि विञ्ञाणं – अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा – सब्बं विञ्ञाणं ‘नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता’ति – एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय पस्सति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो इमस्मिञ्च सविञ्ञाणके काये बहिद्धा च सब्बनिमित्तेसु अहंकारममंकारमानानुसया न होन्ती’’ति।
९०. अथ खो अञ्ञतरस्स भिक्खुनो एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि – ‘‘इति किर, भो, रूपं अनत्ता, वेदना अनत्ता, सञ्ञा अनत्ता, सङ्खारा अनत्ता, विञ्ञाणं अनत्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं कथमत्तानं (सं॰ नि॰ ३.८२) फुसिस्सन्ती’’ति? अथ खो भगवा तस्स भिक्खुनो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्ञाय भिक्खू आमन्तेसि – ‘‘ठानं खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति यं इधेकच्चो मोघपुरिसो अविद्वा अविज्जागतो तण्हाधिपतेय्येन चेतसा सत्थु सासनं अतिधावितब्बं मञ्ञेय्य – ‘इति किर, भो, रूपं अनत्ता, वेदना अनत्ता, सञ्ञा अनत्ता, सङ्खारा अनत्ता, विञ्ञाणं अनत्ता; अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं फुसिस्सन्ती’ति। पटिविनीता पटिच्च विनीता (सी॰ पी॰), पटिपुच्छामि विनीता (स्या॰ कं॰) खो मे तुम्हे, भिक्खवे , तत्र तत्र धम्मेसु’’।
‘‘तं किं मञ्ञथ, भिक्खवे, रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा’’ति? ‘‘अनिच्चं, भन्ते’’। ‘‘यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा’’ति? ‘‘दुक्खं, भन्ते’’। ‘‘यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं – ‘एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता’’’ति? ‘‘नो हेतं , भन्ते’’। ‘‘तं किं मञ्ञथ, भिक्खवे, वेदना… सञ्ञा… सङ्खारा… विञ्ञाणं निच्चं वा अनिच्चं वा’’ति? ‘‘अनिच्चं, भन्ते’’। ‘‘यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा’’ति? ‘‘दुक्खं, भन्ते’’। ‘‘यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं – ‘एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता’’’ति? ‘‘नो हेतं, भन्ते’’। ‘‘तस्मातिह, भिक्खवे, यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा सब्बं रूपं – ‘नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता’ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। या काचि वेदना… या काचि सञ्ञा… ये केचि सङ्खारा… यं किञ्चि विञ्ञाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा सब्बं विञ्ञाणं – ‘नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता’ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको रूपस्मिम्पि निब्बिन्दति, वेदनायपि निब्बिन्दति, सञ्ञायपि निब्बिन्दति, सङ्खारेसुपि निब्बिन्दति, विञ्ञाणस्मिम्पि निब्बिन्दति; निब्बिन्दं विरज्जति , विरागा विमुच्चति। विमुत्तस्मिं विमुत्तमिति ञाणं होति। ‘खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया’ति पजानाती’’ति।
इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुन्ति। इमस्मिञ्च पन वेय्याकरणस्मिं भञ्ञमाने सट्ठिमत्तानं भिक्खूनं अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिंसूति।
महापुण्णमसुत्तं निट्ठितं नवमं।