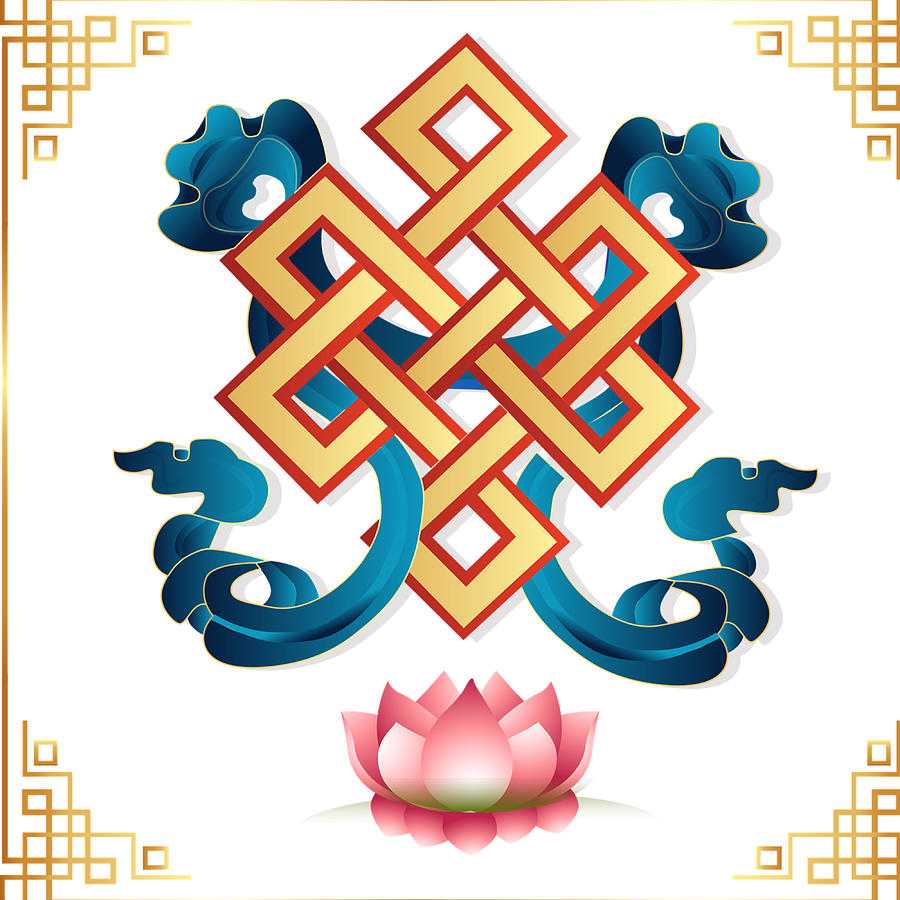
चार आर्यसत्य
भगवान बुद्ध के उपदेशों की सबसे आम और व्यापक रूप से जानी जाने वाली प्रस्तुति उनके पहले उपदेश में दी गई चार आर्य सत्य की शिक्षा है। बुद्ध ने कहा कि ये सत्य मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक सभी जानकारी का सार प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार हाथी के विशाल पदचिह्न में अन्य सभी जानवरों के पदचिह्न समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार चार आर्य सत्य अपनी व्यापकता के कारण सभी कल्याणकारी और लाभकारी शिक्षाओं को अपने भीतर समाहित करते हैं।
जबकि कई व्याख्याकार इन चार सत्य के वास्तविक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अक्सर यह भूल जाते हैं कि इन्हें ‘आर्य सत्य’ क्यों कहा जाता है। दरअसल, ‘आर्य’ शब्द इस बात का खुलासा करता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा को इस विशेष ढांचे में क्यों ढाला और यह शब्द हमें बोध कराता है कि कैसे पूरी धम्म और विनय की शिक्षा एक अनूठे और अपूर्व ध्येय से जुड़ी है।
‘आर्य’ शब्द का प्रयोग बुद्ध ने विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है, जिनका निर्माण उनके उपदेशों के अभ्यास से होता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में इंसानों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा है। एक ओर ‘पुथुज्जन’ हैं, अर्थात वे सामान्य लोग जो अभी भी कलुष और अज्ञानता के आवरण में फंसे हुए हैं। दूसरी ओर ‘आर्य’ हैं, अर्थात वे विशेष व्यक्ति जो अपने आंतरिक चरित्र की महानता से आर्य माने जाते हैं, न कि जन्म, सामाजिक दर्जे या किसी धार्मिक पदवी के कारण।
ये दो श्रेणियाँ पूरी तरह से अलग-अलग और स्थिर नहीं हैं, बल्कि अज्ञानता और अहंकार में जकड़े हुए अंधकारमय दुनिया के इंसान से लेकर पवित्र और ज्ञानवान व्यक्तियों तक, एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी तक का मार्ग दिखाई देता है। इस मार्ग के उच्चतम शिखर पर अर्हंत हैं, जिन्होंने सत्य का इतना गहन अनुभव कर लिया है कि उनके सारे दोषों का अंत हो चुका है और इसी के साथ वे सभी दुखों से मुक्त हो गए हैं।
हालाँकि, यह मार्ग क्रमिक अभ्यास और प्रगति से पार किया जाता है, इसमें हर एक कदम समान रूप से नहीं होता। एक विशेष बिंदु पर, जो दुनिया के साधारण इंसान और एक आर्य के बीच का विभाजन है, एक छलांग लगानी पड़ती है। यह छलांग चार आर्य सत्यों को आत्मसात करने से होती है। इस कारण से बुद्ध द्वारा प्रकट किए गए चार सत्य आर्य कहलाते हैं। जब हम इन सत्यों को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हम साधारण इंसान के दर्जे से निकलकर आर्यों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, और इस विशिष्ट दृष्टि के साथ बुद्ध के शिष्य समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं।
सत्यों की इस गहरी समझ से पहले, चाहे हम कितनी भी आध्यात्मिक गुणों से संपन्न क्यों न हों, हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। हमारी साधारण इंसान के रूप में अर्जित पुण्य क्षीण हो सकता है, जिससे हम जीवन के चक्र में ऊपर-नीचे होते रहते हैं। लेकिन एक बार जब हमने सत्यों को समझ लिया, तो हम इस दुनिया के साधारण जनों की श्रेणी से उठकर आर्यों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। तब सत्य की दृष्टि हमारे सामने प्रकट होती है और भले ही अंतिम लक्ष्य अभी प्राप्त न हुआ हो, लेकिन मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है।
चार आर्य सत्यों का यह पूर्ण अनुभव हमारे जीवन में चार मुख्य कार्यों को सामने लाता है:
पहला आर्य सत्य - दुख: इसे पूरी तरह से समझना होता है। आर्यजन जीवन की धारा में बहने के बजाय इसके सार को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हमें भी अपने जीवन पर गहराई से चिंतन करना होगा, और बुद्ध द्वारा बताए गए सभी दुखों के स्वरूप को समझना होगा।
दूसरा आर्य सत्य - दुख का कारण: इसे त्यागना होता है। आर्यजन अपनी अशुद्धियों को जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम भी यदि आर्य बनना चाहते हैं, तो अपनी तृष्णा और कलुष का सामना करना सीखना होगा और इन्हें धीरे-धीरे त्यागना होगा।
तीसरा आर्य सत्य - दुख का निरोध: इसे साकार करना होता है। यद्यपि निर्वाण का अनुभव केवल आर्य ही कर सकते हैं, हम सभी अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझ सकते हैं और सभी अस्थायी चीज़ों से मुक्ति की आकांक्षा को अपने जीवन का ध्येय बना सकते हैं।
चौथा आर्य सत्य - आर्य अष्टांगिक मार्ग: इसे विकसित करना होता है। बुद्ध के मार्गदर्शन से हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान और निर्वाण की ओर ले जाता है।
इन सत्यों का गहन अनुसंधान ही हमें आर्य बनने का रास्ता दिखाता है। जब हमने इन्हें समझ लिया, तब जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है - और वह है दुख का अंत, पूर्ण मुक्ति, और अर्हंतत्व की प्राप्ति।
संसार के भवचक्र को चार आर्यसत्यों के निगाहों से देखने पर अविद्या और तृष्णा विलुप्त हो जाती है। इसलिए बुद्ध इन्हें लोकुत्तर सम्यकदृष्टि की श्रेणी में रखते है। ये आर्यसत्य कर्म के प्रश्नों को उसी तनाव-व्याकुलता पर केंद्रित करते हैं, जो लोगों को अपने जीवन में सीधे दिखायी दें, प्रासंगिक लगे, और उनके अनुभवों के केंद्र में हो। जब बोधिसत्व को अपने पूर्वजन्म याद आए, तो उनकी हर यादों में उस जीवन में हुआ सुख-दुख का अनुभव शामिल था। उसी तरह, जब अधिकांश लोग अपनी जिंदगी की बात करते हैं, तो वे भी स्वाभाविक रूप से इन्हीं मुद्दों के आस-पास की बातें करते हैं।
हालाँकि चार आर्यसत्य केवल सुख-दुःख की कहानियों तक सीमित नहीं हैं। वे उस पर एक ऐसा स्थायी इलाज प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद वह दुःख दुबारा हमारे मत्थे न पड़े। वे हमें इसे समस्या-समाधान के दृष्टिकोण से देखना सिखाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कौशलता बढ़ाने में प्रयासरत हो। ध्यानसाधना करने वाले केवल सतही और निष्क्रिय अवलोकन से इसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। बल्कि उन्हें अधिक संवेदनशील होकर स्मृति, समाधि और प्रज्ञा को विकसित करने की प्रक्रिया में सक्रिय-रूप से भाग लेना आवश्यक हैं। और एक ऐसी व्यावहारिक कौशलता प्राप्त करना आवश्यक है, जो चित्त-घटकों का कारण-कार्य संबंध गहराई से समझ पाएँ। कर्म कौशलता को बढ़ाते हुए चरम स्तर तक ले जाने से ही इस दुष्चक्र को रोकने की विद्या पता चलती है।
निर्वाण ज्ञान
इदप्पच्चयता, पटिच्च समुप्पाद, और चार आर्यसत्य की गहरी समझ ने बुद्ध को एक सर्वोपरि पुरस्कार से सम्मानित किया। और वह था, निर्वाण। निर्वाण उनकी कर्म कौशलता की परिपूर्णता को दर्शाता है। जब कौशलता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो अरचित-अवस्था की ओर ले जाती है, जो लोक-परलोक के अनुभव से परे होता है। और जब वहाँ से इस लोक में लौटा जाता है, तो दिखता है कि यह लोक पूरी तरह से पूर्व-कर्मों के परिणामस्वरूप ही उपजा है। जब नया कर्म जुड़ता नहीं, तो ब्रह्मांड का अनुभव खत्म हो जाता है। तब, इस बात की पुष्टि होती है कि कर्म ही ब्रह्मांड के अनुभव को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रकार, बुद्ध की भी कर्म-कौशलता वर्तमान क्षण पर केंद्रित थी, लेकिन परिणामी संबोधि से पता चला कि उसी में त्रिकाल ज्ञान छिपा है।
कर्म सिद्धांत में आस्था
कर्म बौद्ध धर्म का एक मूलभूत सिद्धान्त है, और इस पर आस्था रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म पर सीख, चाहे कथात्मक रूप में हो या सैद्धान्तिक रूप में, साधना को दिशा और तात्कालिकता देता है। यह संसार कर्म के नियमों से ही संचालित होता है। इन नियमों को समझने से ही सुख और राहत स्थायी-रूप में मिल सकती है। पुण्य हो या पाप, चेतना से बनते हैं, और लोक-परलोक के अनुभव को कायम रखते हैं। इस पर महारत हासिल करने से ही, अंततः कर्मचक्र को थामा जा सकता है।
बौद्ध साधना में “शून्य अवस्था” का बड़ा महत्व है, जिसमें कर्म की प्रक्रियाओं पर बिना सवाल उठाएँ कि “उसके पीछे कोई आत्मा है या नहीं”, उन पर निष्पक्ष और तटस्थ ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान केन्द्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए स्मृति, समाधि और प्रज्ञा को ऊँचे स्तर तक विकसित करना होता है। जब प्रज्ञा पूर्णतः विकसित होकर परिपूर्ण हो जाती है, तब कर्म प्रक्रिया से जुड़े सभी घटकों का विश्लेषण भी अंततः खत्म हो जाता है। तब अंततः प्रज्ञाचक्षु के आगे दो ही अंतिम कर्म बचते हैं — ध्यान देना और विश्लेषण करना। उन दोनों ही बची प्रक्रियाओं का शॉर्ट सर्किट होकर मुक्तिद्वार खुलता है।
कोई व्यक्ति कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे बिना भी बौद्धसाधना के कुछ अंगों को धारण कर सकारात्मक परिणाम पा सकता है। किन्तु, मंजिल पर पहुँच कर साधना खत्म करने के लिए इस सिद्धांत में अडिग विश्वास अनिवार्य है। यह विश्वास धैर्य, प्रतिबद्धता और विवेक को बनाए रखने में मदद करता है, जो समग्र अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण हैं। साधना पथ पर अग्रसर होते हुए, कर्म सिद्धांत के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। क्योंकि उसके परिणाम पुष्टि करते रहते हैं।
कर्म में आस्था उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देता है। एक-ओर लोकीय पुण्य करते हुए, वह सुखी भविष्य की ओर बढ़ता है, जबकि दूसरी-ओर लोकुत्तर मुक्तिसाधना करते हुए, वह सुखी वर्तमान में जीने लगता है। और एक समय आता है जब दोनों ही एक होकर व्यक्ति को त्रिकाल बंधनों से मुक्ति प्रदान कर स्थायी सुख में डुबोते हैं।