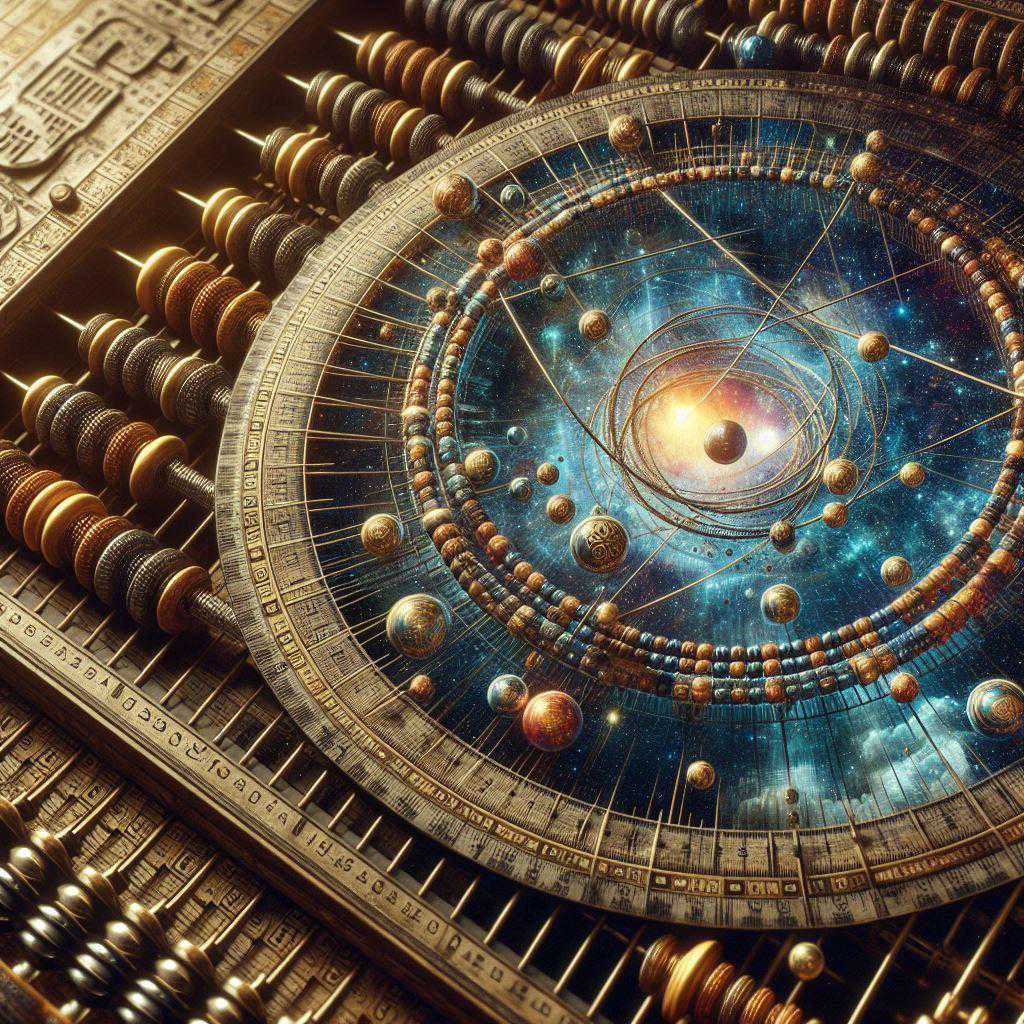
कर्म
- “क्या मानव अपने भाग्य का गुलाम है, या विधाता?”
- “क्या जीवन में दुःख भोगना अनिवार्य है, या वैकल्पिक?”
- “क्या हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं?”
- “क्या हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है?”
ये ऐसे गहरे प्रश्न हैं, जो अनुभव की गहराई से उत्पन्न होते हैं और हमें बार-बार सोचने पर मजबूर करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर न केवल हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को गढ़ते हैं, बल्कि यह भी तय करते हैं कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाते हैं। ये प्रश्न हमारे जीवन के आधार और उद्देश्य की नींव रखते हैं। इसी के साथ, यह भी निर्धारित करते हैं कि हम सुख और शांति की तलाश कहाँ करें — अपने भीतरी अंतर्मन में, बाहरी दुनिया में, या फिर अपने भाग्य को कोसते हुए उससे उम्मीदें छोड़ दें।
इन्हीं बुनियादी प्रश्नों ने सिद्धार्थ गौतम को भी सताया। उन्होंने इस खोज में अपना जीवन दाँव पर लगा दिया, और अंततः मुक्तिमार्ग का बोध किया। उन्हें पता चला कि मानव जीवन सार्थक है — क्योंकि यदि कोई सही दिशा में प्रयास करें, तो वह अपने पीड़ादायी भाग्य से मुक्त हो सकता है। वह संसार के प्रतिबंधों को लाँघ कर, जीवन की सीमाओं से मुक्त होकर, अमर्त्य सुख, शान्ति और राहत को प्राप्त कर सकता है।
इसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप ‘कर्म का सिद्धांत’ प्रकट हुआ, जो बौद्ध धर्म की आधारशिला बना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने भाग्य के गुलाम बनने या विधाता बनने का चुनाव करते हैं।
कर्म की व्याख्या
कर्म का सरल अर्थ है — चेतनापूर्वक किए गए कृत्य, या इरादे से की गई हरकतें। ये कर्म जाने-अनजाने में तनाव पैदा कर सकते हैं या राहत दे सकते हैं, और कभी-कभी इनका मिला-जुला असर भी होता है। इनका प्रभाव हम पर, दूसरों पर, या दुनिया पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ सकता है, या अप्रत्यक्ष रूप से। कर्मों का यह प्रभाव सकारात्मक और लाभदायक हो सकता है, अथवा नकारात्मक और हानिकारक साबित हो सकता है। जैसी चेतना और जितना प्रभाव हो, उसी के अनुसार कर्म का परिणाम उपजता है।
यह परिणाम तुरंत महसूस हो सकता है, कुछ समय बाद इसी जीवन में सामने आ सकता है, या फिर अगले जन्मों में प्रकट हो सकता है। कर्म की यह प्रक्रिया जटिल और विस्तृत है, लेकिन सरलता से कहा जाए तो हमारे इरादे और कार्य ही हमारे भविष्य और अनुभवों को आकार देते हैं।
बुद्ध कहते हैं —
“सब्बे सत्ता कम्मस्सका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मप्पटिसरणा। यं कम्मं करिस्सन्ति—कल्याणं वा पापकं वा—तस्स दायादा भविस्सन्ती।”
— अंगुत्तरनिकाय ५:५७ : अभिण्हपच्चवेक्खितब्बठान सुत्त
अर्थात, सभी सत्व अपने कर्म के कर्ता, कर्म के वारिस, कर्म से जन्में, कर्म से बंधें, और कर्म के शरणागत हैं। वे जो भी कर्म करेंगे — कल्याणकारी या पापपूर्ण — उसी के उत्तराधिकारी बनेंगे।
कर्म तीन स्तरों पर होते हैं — (१) शारीरिक क्रियाओं से, (२) वाणी के शब्दों से, और (३) मन के सोच-विचार से। चाहे कर्म दूषित मन से किए गए हों, भले मन से किए गए हों, या भ्रमित अवस्था में हुए हों — हर कर्म का परिणाम उसके अनुसार ही होता है।
यदि कोई बुरा कर्म करता है, तो उसके परिणाम हानिकारक और दुःखदायी होते हैं। इसके विपरीत, भले कर्म का परिणाम लाभदायक और सुखदायी होता है। इस प्रकार, हमारे हर कर्म का एक निश्चित प्रभाव होता है, और हम अपने विचारों, शब्दों, और कार्यों के द्वारा अपने भविष्य को ढालते हैं।
बुद्ध कहते हैं —
"मनोपुब्बङ्गमा धम्मा,
मनोसेट्ठा मनोमया,
मनसा चे पदुट्ठेन,
भासति वा करोति वा,
ततो नं दुक्खमन्वेति,
चक्कंव वहतो पदं!"— धम्मपद यमकवग्ग १
अर्थात,
मन मालिक है!
मन निर्माणकर्ता!
दूषित मन से बोलने या करने पर,
दुःख ऐसे पीछे पड़ता है
— जैसे खींचने वाले (बैल) के पीछे
चक्के पड़ते हैं।
"मनोपुब्बङ्गमा धम्मा,
मनोसेट्ठा मनोमया,
मनसा चे पसन्नेन,
भासति वा करोति वा,
ततो नं सुखमन्वेति,
छायाव अनपायिनी!"— धम्मपद यमकवग्ग २
अर्थात,
मन मालिक है।
मन निर्माणकर्ता है।
उजले मन से बोलने या करने पर
सुख ऐसे पीछे पड़ता है
— जैसे छाया,
जो कभी साथ न छोड़े।
अर्थात, दूषित मन से किए गए कर्म अकुशल होते हैं, जिनका परिणाम कड़वा और पीड़ादायक होता है। जबकि स्वच्छ मन से किए गए कर्म कुशल होते हैं, जिनका फल मीठा और सुखदायी होता है।
मन की दूषितता लोभ, द्वेष, या भ्रम के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें “अकुशल मूल” कहा जाता है। दूसरी ओर, स्वच्छ चित्त वे अवस्थाएँ हैं, जिनमें निर्लोभ, निर्द्वेष, और निर्मोह होते हैं, और इन्हें “कुशल मूल” कहा जाता है।
भगवान ब्राह्मणों को सिखाते हुए पुछते हैं —
“क्या लगता है, कालामों? जब किसी व्यक्ति के भीतर लोभ उपजता हो, तो वह उसके हित के लिए उत्पन्न होगा अथवा अहित के लिए?”
“अहित के लिए, भन्ते!”
“और कोई लालची, लोभ के वशीभूत, लोभचित्त से बेकाबू होकर — जीवहत्या करे, चोरी करे, पराई औरत के पीछे जाए, झूठ बोले, और यह दुसरों से भी करवाए, तो क्या वह उसके दीर्घकालीन अहित और दुःख के लिए होगा?”
“हाँ, भन्ते!”
“और कालामों! जब किसी व्यक्ति के भीतर द्वेष उपजता हो… या भ्रम उपजता हो, तो वह उसके हित के लिए उत्पन्न होगा अथवा अहित के लिए?”
“अहित के लिए, भन्ते!”
“और कोई दुष्ट, द्वेष के वशीभूत, द्वेषचित्त से बेकाबू होकर… या कोई मूढ़, भ्रम के वशीभूत, भ्रमित चित्त से बेकाबू होकर — जीवहत्या करे, चोरी करे, पराई औरत के पीछे जाए, झूठ बोले, और यह दुसरों से भी करवाए, तो क्या वह उसके दीर्घकालीन अहित और दुःख के लिए होगा?”
“हाँ, भन्ते!”
“क्या लगता है, कालामों? यह स्वभाव कुशल हैं अथवा अकुशल?”
“अकुशल, भन्ते!”
“दोषपूर्ण है अथवा निर्दोष?”
“दोषपूर्ण, भन्ते!”
“ज्ञानियों द्वारा निंदित है अथवा प्रशंसित?”
“निंदित, भन्ते!”
“उसे मानने से, उस पर चलने से अहित होता है, दुःख आता है अथवा नहीं? या क्या लगता है?”
“उसे मानने से, उस पर चलने से अहित होता है, भन्ते! दुःख आता है। ऐसा ही हमें लगता है।”
“इसलिए मैं कहता हूँ कि — न सुनी-सुनाई बात मानो, न परंपरागत बात मानो, न अटकलेबाजी मानो, न शास्त्र-ग्रंथों की बात मानो, न तर्कसंगत कारण मानो, न अनुमानित कारण मानो, न समतुल्य परिस्थिति में लागू होती बात मानो, न अपनी धारणा से मेल खाती बात मानो, न संभावित बात मानो, न श्रमण गुरु के सम्मानार्थ मानो। बल्कि, जब तुम्हें स्वयं पता चले कि — ‘यह स्वभाव अकुशल है। यह स्वभाव दोषपूर्ण है। यह स्वभाव ज्ञानियों द्वारा निंदित है। यह स्वभाव मानने से, उस पर चलने से अहित होता है, दुःख आता है’ — तब तुम्हें वह स्वभाव त्याग देना चाहिए।
और कालामों! जब तुम्हें स्वयं पता चले — ‘यह स्वभाव कुशल है। यह स्वभाव निर्दोष है। यह स्वभाव ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है। यह स्वभाव मानने से, उस पर चलने से हित होता है, सुख आता है’ — तब तुम्हें वह स्वभाव धारण कर उसी में रहना चाहिए।
क्या लगता है, कालामों? जब किसी व्यक्ति के भीतर निर्लोभता उपजती हो… निर्द्वेषता उपजती हो… निर्भ्रमता उपजती हो, तो वह उसके हित के लिए उत्पन्न होगी अथवा अहित के लिए?”
“हित के लिए, भन्ते!”
“और कोई निर्लोभी न लोभ के वशीभूत, न लोभचित्त से बेकाबू होकर… [अथवा] कोई निर्द्वेषी न द्वेष के वशीभूत, न द्वेषचित्त से बेकाबू होकर… [अथवा] कोई निर्भ्रमी न भ्रम के वशीभूत, न भ्रमचित्त से बेकाबू होकर — जीवहत्या न करे, चोरी न करे, पराई औरत के पीछे न जाए, झूठ न बोले, और न ही दुसरों से करवाए, तो क्या वह उसके दीर्घकालीन हित और सुख के लिए होगा?”
“हाँ, भन्ते!”
“और क्या लगता है, कालामों? यह स्वभाव कुशल है अथवा अकुशल?”
“कुशल, भन्ते!”
“दोषपूर्ण है अथवा निर्दोष?”
“निर्दोष, भन्ते!”
“ज्ञानियों द्वारा निंदित है अथवा प्रशंसित?”
“प्रशंसित, भन्ते!”
“उसे मानने से, उस पर चलने से हित होता है, सुख आता है अथवा नहीं? या क्या लगता है?”
“उसे मानने से, उस पर चलने से हित होता है, भन्ते! सुख आता है। ऐसा ही हमें लगता है।”
““इसलिए मैं कहता हूँ कि — न सुनी-सुनाई बात मानो, न परंपरागत बात मानो, न अटकलेबाजी मानो, न शास्त्र-ग्रंथों की बात मानो, न तर्कसंगत कारण मानो, न अनुमानित कारण मानो, न समतुल्य परिस्थिति में लागू होती बात मानो, न अपनी धारणा से मेल खाती बात मानो, न संभावित बात मानो, न श्रमण गुरु के सम्मानार्थ मानो। बल्कि, जब तुम्हें स्वयं पता चले कि — ‘यह स्वभाव कुशल है। यह स्वभाव निर्दोष है। यह स्वभाव ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है। यह स्वभाव मानने से, उस पर चलने से हित होता है, सुख आता है’ — तब तुम्हें वह स्वभाव धारण कर उसी में रहना चाहिए।
—अंगुत्तरनिकाय ३:६६ : केसमुत्तिसुत्त
अर्थात, मानव अपने कर्मों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ हमारे पिछले कर्मों का फल हैं, और साथ ही वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होती हैं। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। मानव कर्म करके अपना भाग्य स्वयं रचता है, और परिणाम भुगतता है। उसका जन्म भी कर्म से होता है, और मौत भी। कर्म से वह जीवन में सुख-दुःख का अनुभव करता है। कर्म की गंभीरता से तय होता है कि उनके परिणाम तत्काल समाप्त होंगे, अथवा दीर्घकाल तक चलते रहेंगे। कोई कर्म अनंतकाल तक फल नहीं दे सकता।
कर्म का सिद्धांत यह नहीं कहता कि सब कुछ पूर्व-निर्धारित है। पिछले कर्मों के कारण परिस्थितियाँ ज़रूर उपजती हैं, किन्तु हमारे पास वर्तमान कर्मों को चुनने की स्वतंत्रता है।
यदि आप चलते हुए एक मोड़ पर आएँ, जहाँ से तीन रास्ते निकलते हों, तो आपको उनमें से एक रास्ता चुनना होगा। हो सकता है कि एक भले रास्ते पर घनी छाया प्रदान करते पेड़ हों, शीतल जल की व्यवस्था हो, और सुखद विश्रामगृह हो। दूसरा रास्ता बंजर ऊबड़-खाबड़ इलाके से गुज़रता हो, जहाँ चोर-लुटेरे घात लगाकर बैठे हों। जबकि तीसरा रास्ता जंगल के एकांत से गुज़रता हो।
आप जो रास्ता चुनेंगे, उसके फल भुगतेंगे और उसकी मंज़िल पर पहुँचेंगे। किन्तु, तब भी तीनों रास्तों का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार अलग-अलग होगा।
किन्तु, व्यक्ति की आज की परिस्थिति भी कर्मों के परिणामों की तीव्रता को कम या अधिक कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति भोग-संसार में लिप्त रहता है, तो उसे अपने पूर्व-कर्मों के फल एक विशेष प्रकार से प्राप्त होते हैं। वहीं, यदि वह धर्म का पालन करता है, तो वही कर्म के फल भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। और यदि वह व्यक्ति बुरे कर्मों में डूब चुका हो, तो वही फल उसे एक और अधिक कष्टदायक रूप में मिलते हैं।
इसी प्रकार, भोग-संसार में डूबे व्यक्ति के आज के कर्म भविष्य में एक विशेष ढंग से परिणाम देंगे। जबकि, धर्म का पालन करने वाले या दुष्ट व्यक्ति के वही कर्म भविष्य में भिन्न-भिन्न रूपों में फलित होंगे। कर्मों के प्रभाव का तरीका और अनुभव व्यक्ति के वर्तमान आचरण और मनोदशा पर निर्भर करता है। भगवान उपमा देकर बताते हैं —
जैसे किसी बकरी-चोर के पकड़े जाने पर, कसाई को छूट मिलती है कि वह उसे पीटे, बांधे, काटे या जैसा चाहे करे। उसी तरह, कोई पुरुष निर्धन, ग़रीब, अल्पसंपन्न होता है। इस तरह के बकरी-चोर के पकड़े जाने पर, कसाई को छूट मिलती है कि वह उसे पीटे, बांधे, काटे या जैसा चाहे करे।
किन्तु, किसी दूसरे बकरी-चोर के पकड़े जाने पर कसाई को छूट नहीं होती कि वह उसे पीटे, बांधे, काटे या जैसा चाहे करे। उसी तरह, कोई पुरुष महाधनी, महासंपत्तिशाली एवं महाभोगसंपदा का स्वामी, राजा अथवा राजमंत्री होता है। इस तरह के बकरी-चोर के पकड़े जाने पर कसाई को छूट नहीं होती है। अधिकतम वह यही कर सकता है कि हृदय के आगे हाथ जोड़कर याचना करें: “साहब, कृपा कर मेरी बकरी या उसकी कीमत ही दे दीजिए!”
उसी तरह, कोई व्यक्ति काया में अविकसित रहता है, शील में अविकसित रहता है, चित्त में अविकसित रहता है, तथा अंतर्ज्ञान में अविकसित रहता है — संकीर्ण सोच, संकुचित हृदय वाला व्यक्ति, जो पीड़ित रहता हो। इस तरह के व्यक्ति का छोटा-सा पापकर्म उसे नर्क ले जाता है।
जबकि कोई व्यक्ति काया में सुविकसित रहता है, शील में सुविकसित रहता है, चित्त में सुविकसित रहता है, तथा अन्तर्ज्ञान में सुविकसित रहता है — खुले मन, उदार हृदय वाला व्यक्ति, जो ‘विस्तृत, विशाल, असीम मानस’ से रहता हो। इस तरह के व्यक्ति का छोटा-सा पापकर्म उसे इसी जीवन में मात्र क्षणभर महसूस होता है।
—अंगुत्तरनिकाय ३:१०१ : लोणकपल्लसुत्त
कर्म केवल सजा या इनाम नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है जो कारण और प्रभाव पर आधारित है। इसलिए बुद्ध बताते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए, अच्छे कर्मों को धरण करना चाहिए, और चित्त को स्वच्छ करते रहना चाहिए। जिससे हमें, दूसरों को, या सभी को दीर्घकालीन लाभ होगा।
कर्म का सिद्धांत पूर्णतः समझना सरल नहीं है। समय की धारा में उपजे विविध कर्मों के विविध परिणाम जानना जटिल कार्य है। इसलिए, भगवान उसे सरल बनाकर कहते हैं —
"सब्बपापस्स अकरणं,
कुसलस्स उपसम्पदा,
सचित्तपरियोदपनं,
एतं बुद्धान सासनं।"— धम्मपद बुद्धवग्गो १८३
अर्थात,
कुशलता को धारण करना,
अपने चित्त को स्वच्छ करना
— यही बुद्धों की शिक्षा है।