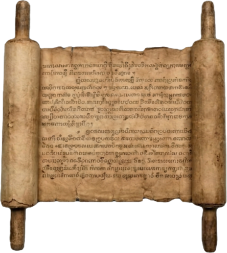
पायासि की बहस
सूत्र परिचय
आयुष्मान कुमार कश्यप भिक्षुसंघ के चुनिन्दा प्रमुख भिक्षुओं में से एक, सुभाषितों में अग्र थे। यह ऐसा इकलौता सूत्र है, जो जैन साहित्य के “पाएसि-कहाणयं सूत्र” से काफी मेल खाता है। उस जैन सूत्र में भी श्रावस्ती के उत्तर-पूर्व में स्थित सेतव्या नगर के राजा “पाएसि” और “केसिन” के बीच एक समान संवाद है। यह कहना कठिन है कि इन दोनों महान श्रमण परंपराओं में से कौन-सा सूत्र प्रामाणिक है, लेकिन यह निश्चित है कि यह सूत्र बहुत रोचक है, यादगार उपमाओं और बोध-कथाओं से भरा हुआ है।
पायासि अपनी आँखों से प्राणियों के जीव और परलोक को देखकर आश्वस्त होना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने राजकीय अधिकारों का दुरुपयोग किया। वह पकड़े गए अपराधियों पर अत्यंत हिंसक और क्रूर प्रयोग करता था, ताकि परलोक के रहस्यों को समझ सके। ऐसे भयावह प्रयोगों की कहानियाँ आजकल के कुछ उन्नत देशों में भी सुनने को मिलती हैं, जहाँ मानव और प्राणी जीवन के प्रति कोई संवेदना नहीं होती।
लेकिन भन्ते कुमार कश्यप ने बड़ी करुणा से पायासि को इन खतरनाक प्रयोगों से बाहर निकाला, और उसे सम्यक दृष्टि में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, पायासि की कठोरता और अज्ञानता उसके धार्मिक जीवन में भी बनी रही, और परलोक में उसे बहुत बड़ी सीख मिली। पायासि ने अपने परलोक के अनुभवों को भन्ते लोगों के साथ आकर साझा किया, और इसके परिणामस्वरूप कई उपासक और उपासिकाएँ अब दान-पुण्य के कार्यों को और अधिक समझदारी और सही तरीके से करने लगी हैं।
हिन्दी
ऐसा मैंने सुना — एक समय आयुष्मान कुमार कश्यप कोसल राज्य में पाँच-सौ भिक्षुओं के विशाल भिक्षुसंघ के साथ भ्रमण करते हुए सेतब्या [=श्वेताम्बी, जो श्रावस्ती के उत्तर-पूर्व में बसा है] नामक कोसल नगर में पहुँचे। तब आयुष्मान कुमार कश्यप सेतब्या की उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन में आकर विहार करने लगे।
उस समय, पायासि राजन्य [=मुखिया] सेतब्या में रहता था, जो एक घनी आबादी वाला इलाका था, और घास, लकड़ी, जल और धन-धान्य से संपन्न था। राजा प्रसेनजित कोसल ने राज-उपहार के तौर पर सेतब्या की राजसत्ता पायासि राजन्य को सौंपी हुई थी।
१. पायासि राजन्य
उस समय, पायासि राजन्य को इस प्रकार की बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी—"[मरणोपरांत] परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए [“ओपपातिक”] सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।"
और, सेतब्या के ब्राह्मणों और गृहस्थों ने सुना, “यह सच है, श्रीमान! श्रमण गौतम के श्रावक श्रमण कुमार कश्यप कोसल राज्य में पाँच-सौ भिक्षुओं के विशाल भिक्षुसंघ के साथ भ्रमण करते हुए हमारे सेतब्या में आ पहुँचे हैं, और सेतब्या की उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन में विहार कर रहे हैं। और उन श्रमण कुमार कश्यप के बारे में ऐसी यशकीर्ति फैली है कि ‘वे पंडित है, अनुभवी है, मेधावी है, बहुत धम्म सुने है, सटीक उत्तर देते है, अत्यंत प्रतिभाशाली है, और परिपक्व अरहंत है। और ऐसे अर्हन्तों का दर्शन वाकई शुभ होता है।”
तब सेतब्या के ब्राह्मण और गृहस्थ, अलग-अलग गुटों में झुंड बनाकर, सेतब्या से निकलकर उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन की ओर चल पड़े। उस समय पायासि राजन्य दिन में झपकी लेने के लिए महल के ऊपरी कक्ष में गया था। उसने सेतब्यावासी ब्राह्मणों और गृहस्थों को, अलग-अलग गुटों में झुंड बनाकर, सेतब्या से निकलकर उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन की ओर जाते देखा। ऐसा देखकर उसने सचिव से कहा, “सचिव जी, ये सेतब्यावासी ब्राह्मण और गृहस्थ, अलग-अलग गुटों में झुंड बनाकर, सेतब्या से निकलकर उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन की ओर क्यों जा रहे हैं?”
“ऐसा है, श्रीमान, कि श्रमण गौतम के श्रावक श्रमण कुमार कश्यप कोसल राज्य में पाँच-सौ भिक्षुओं के विशाल भिक्षुसंघ के साथ भ्रमण करते हुए हमारे सेतब्या में आ पहुँचे हैं, और सेतब्या की उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन में विहार कर रहे हैं। और उन श्रमण कुमार कश्यप के बारे में ऐसी यशकीर्ति फैली है कि ‘वे पंडित है, अनुभवी है, मेधावी है, बहुत धम्म सुने है, सटीक उत्तर देते है, अत्यंत प्रतिभाशाली है, और परिपक्व अरहंत है। उन्ही श्रमण कुमार कश्यप का दर्शन लेने के लिए ये सेतब्यावासी ब्राह्मण और गृहस्थ, अलग-अलग गुटों में झुंड बनाकर, सेतब्या से निकलकर उत्तर-दिशा में सिंसपा-वन की ओर जा रहे हैं।”
“तब सचिव जी, उन सेतब्यावासी ब्राह्मणों और गृहस्थों के पास जाओ, और उन्हें कहो—‘श्रीमानों, पायासि राजन्य कहता है कि थोड़ा ठहर जाएँ, ताकि वे भी श्रमण कुमार कश्यप का दर्शन लेने के लिए साथ आ पाएँ।’ [मुझे जाना चाहिए] इसके पहले कि श्रमण कुमार कश्यप इन मूर्ख और अनुभव-हीन ब्राह्मणों और गृहस्थों को यकीन दिला दे कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’ क्योंकि, सचिव जी, दरअसल परलोक तो होता नहीं है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते नहीं हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।”
“ठीक है, श्रीमान!” सचिव ने उत्तर दिया, और उन सेतब्यावासी ब्राह्मणों और गृहस्थों के पास गया। और उन्हें कहा—“श्रीमानों, थोड़ा ठहर जाएँ, ताकि पायासि राजन्य भी श्रमण कुमार कश्यप का दर्शन लेने के लिए साथ आ पाएँ।”
तब, पायासि राजन्य, सेतब्यावासी ब्राह्मणों और गृहस्थों के घिरा हुआ, सिंसपा-वन में आयुष्मान कुमार कश्यप के पास गया, और जाकर हाल-चाल लिया, और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप कर एक ओर बैठ गया। कुछ सेतब्यावासी ब्राह्मणों और गृहस्थों ने आयुष्मान कुमार कश्यप को अभिवादन किया, और एक-ओर बैठ गए। कुछ ब्राह्मणों और गृहस्थों ने आयुष्मान कुमार कश्यप से नम्रतापूर्ण वार्तालाप किया, और एक-ओर बैठ गए। कुछ ब्राह्मणों और गृहस्थों ने हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध वंदन किया, और एक-ओर बैठ गए। कोई ब्राह्मणों और गृहस्थों ने आयुष्मान कुमार कश्यप को अपना नाम-गोत्र बताया, और एक-ओर बैठ गए। और कोई ब्राह्मण और गृहस्थ चुपचाप ही एक-ओर बैठ गए।
२. नास्तिक-वाद
एक ओर बैठकर पायासि राजन्य ने आयुष्मान कुमार कश्यप से कहा, “श्रीमान कश्यप, मेरी ऐसी धारणा है, ऐसी दृष्टि है कि—‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“राजन्य, काश मैं ऐसी धारणा, ऐसी दृष्टि के बारे में न कभी देखूँ, न कभी सुनूँ। कैसे कोई ऐसा कह सकता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.१ चाँद और सूरज की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप से ही प्रतिप्रश्न करता हूँ। जैसे आप को ठीक लगे, वैसा उत्तर दें। तो, क्या लगता है, राजन्य? क्या चाँद और सूरज इस लोक में हैं, या किसी दूसरे [पर]लोक में? वे देवता हैं या मनुष्य?”
“श्रीमान कश्यप, चाँद और सूरज किसी दूसरे लोक में हैं। और, वे देवता हैं, मनुष्य नहीं।”
“इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(१) “ऐसा है, श्रीमान कश्यप, कि मेरे कुछ मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार करते हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातें करते हैं, लालची और दुर्भावनापूर्ण होकर मिथ्यादृष्टि भी धारण करते हैं [=दस अकुशल]। कुछ समय पश्चात, वे बीमार पड़ते हैं, किसी दर्दभरे गंभीर रोग से पीड़ित। और, जब मुझे पता चलता है कि ‘वे अपनी बीमारी से ठीक नहीं होंगे’, तब मैं उनके पास जाकर कहता हूँ, “श्रीमान, कई श्रमण-ब्राह्मणों की ऐसी धारणा, ऐसी दृष्टि हैं कि ‘जो जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार करते हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातें करते हैं, लालची, दुर्भावनापूर्ण, और मिथ्यादृष्टि धारण करते हैं, वे मरणोपरांत काया छूटने पर नीचे यातनालोक में दुर्गति होकर नर्क में उपजते हैं। आप भी, श्रीमान, जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार करते रहे है, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातें करते रहे है, लालची, दुर्भावनापूर्ण, और मिथ्यादृष्टि धारण करते रहे है। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों की बात सच्ची है, तो श्रीमान, मरणोपरांत काया छूटने पर नीचे यातनालोक में दुर्गति होकर, आप नर्क में उपजेंगे। यदि वाकई ऐसा हो, श्रीमान, कि मरणोपरांत काया छूटने पर नीचे यातनालोक में दुर्गति होकर, आप नर्क में उपजे, तो मुझे आकर बताएं कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’ मुझे, श्रीमान, आप पर श्रद्धा है, विश्वास है। जो श्रीमान ने देख लिया, मानो मैंने स्वयं देख लिया।’
वे मुझे साधुकार देते [=हामी भरते] हैं, किन्तु आज तक न कोई मेरे पास आया, न ही किसी ने दूत ही भेजा। इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.२ चोर उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप से प्रतिप्रश्न करता हूँ। जैसे आप को ठीक लगे, वैसा उत्तर दें। क्या लगता है, राजन्य, यदि आप के पुरुष किसी चोर या अपराधी को पकड़कर पेश करें, ‘महाशय, यह अपराधी चोर है। जैसी आपकी इच्छा हो, उसे वैसा दंड दें।’
तब, आप कहे, ‘ठीक है, श्रीमानों। इस पुरुष की बाहों को पीछे कर रूखी रस्सी से कसकर बांध दो। और उसका सिर मुंडवा कर तेज नगाड़े की आवाज में गली-गली, मार्ग-मार्ग घुमाकर दक्षिण-द्वार से बाहर निकाल, नगर के दक्षिण में वध-स्थल पर ले जाकर उसका सिर काट दो।’
“बहुत अच्छा!” पुरुष आप को उत्तर देकर, उस अपराधी चोर की बाहों को पीछे कर रूखी रस्सी से कसकर बांधकर, उसका सिर मुंडवा कर, तेज नगाड़े की आवाज में गली-गली, मार्ग-मार्ग घुमाकर दक्षिण-द्वार से बाहर निकाल, नगर के दक्षिण में वध-स्थल पर ले जाते हैं। तब, क्या चोर के जल्लादों को कहने पर कुछ मिलेगा, “कृपा करिए, श्रीमान जल्लादों। इस अमुक-अमुक गाँव में, या इस अमुक-अमुक नगर में मेरे कुछ मित्र-सहचारी या रिश्तेदार-संबंधी रहते हैं। क्या आप रुकेंगे, जब तक मैं उनसे मिलकर आता हूँ?” अथवा, उसके बड़बड़ाने रहने पर भी क्या जल्लाद उसका सिर नहीं काट देंगे?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, उसके बड़बड़ाने रहने पर भी जल्लाद उसका सिर काट ही देंगे।”
“राजन्य, जब चोर के मानव होने पर भी वह जल्लाद मानवों द्वारा सुना नहीं जाएगा, तब आपके जो मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार करते रहे है, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातें करते रहे है, लालची, दुर्भावनापूर्ण, और मिथ्यादृष्टि धारण करते हैं, वे मरणोपरांत काया छूटने पर नीचे यातनालोक में दुर्गति होकर, नर्क में उपजते हो, उन्हें नर्कपालों से कहने पर भला क्या मिलेगा, “कृपा करिए, श्रीमान नर्कपालों। क्या आप रुकेंगे, जब तक मैं पायासि राजन्य को जाकर बताता हूँ, ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(२) “ऐसा है, श्रीमान कश्यप, कि मेरे कुछ मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार से विरत रहते हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातों से विरत रहते हैं, लालची और दुर्भावनापूर्ण से विरत होकर सम्यक-दृष्टि धारण करते हैं [=दस कुशल]। कुछ समय पश्चात, वे बीमार पड़ते हैं, किसी दर्दभरे गंभीर रोग से पीड़ित। और, जब मुझे पता चलता है कि ‘वे अपनी बीमारी से ठीक नहीं होंगे’, तब मैं उनके पास जाकर कहता हूँ, “श्रीमान, कई श्रमण-ब्राह्मणों की ऐसी धारणा, ऐसी दृष्टि हैं कि ‘जो जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार से विरत रहते हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातों से विरत रहते हैं, लालची और दुर्भावनापूर्ण से विरत होकर सम्यक-दृष्टि धारण करते हैं, वे मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर स्वर्ग में उपजते हैं। आप भी, श्रीमान, जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार से विरत रहे हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातों से विरत रहे हैं, लालची और दुर्भावनापूर्ण से विरत होकर सम्यक-दृष्टि धारण किया है। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों की बात सच्ची है, तो श्रीमान, मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर, आप स्वर्ग में उपजेंगे। यदि वाकई ऐसा हो, श्रीमान, कि मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर, आप स्वर्ग में उपजे, तो मुझे आकर बताएं कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’ मुझे, श्रीमान, आप पर श्रद्धा है, विश्वास है। जो श्रीमान ने देख लिया, मानो मैंने स्वयं देख लिया।’
वे मुझे साधुकार देते हैं, किन्तु उनमें से भी आज तक न कोई मेरे पास आया, न ही किसी ने दूत ही भेजा। इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.३ मल की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। कल्पना करें, राजन्य, कि एक पुरुष हो, जो सिर तक विष्ठा [गूह, मल] में डूबा हो। तब आप किसी पुरुष को आज्ञा दे, ‘अरे, श्रीमानों, इस पुरुष को विष्ठा से निकालो।’
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष को विष्ठा से निकाले।
तब आप उन्हें कहे, “अरे, श्रीमानों, इस पुरुष के शरीर पर लगी विष्ठा को बाँस के टुकड़ों से अच्छी तरह साफ करो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष के शरीर पर लगी विष्ठा को बाँस के टुकड़ों से अच्छी तरह साफ कर दे।
तब आप उन्हें कहे, “अरे, श्रीमानों, इस पुरुष के शरीर को पीली मिट्टी से तीन-बार उबटन लगा-लगाकर अच्छे से साफ करो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष के शरीर को पीली मिट्टी से तीन-बार उबटन लगा-लगाकर अच्छे से साफ कर दे।
तब आप उन्हें कहे, “अरे, श्रीमानों, इस पुरुष के शरीर को तेल लगाकर तीन-बार महीन स्नान-चूर्ण लगा-लगाकर अच्छे से नहला दो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष के शरीर को तेल लगाकर तीन-बार महीन स्नान-चूर्ण लगा-लगाकर अच्छे से नहला दे।
तब आप उन्हें कहे, “श्रीमानों, अब इस पुरुष की केश और दाढ़ी बना दो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष की केश और दाढ़ी बना दे।
तब आप उन्हें कहे, “श्रीमानों, अब इस पुरुष को महँगी माला, महँगे लेप, और महँगे वस्त्र पहना दो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष को महँगी माला, महँगे लेप, और महँगे वस्त्र पहना दे।
तब आप उन्हें कहे, “श्रीमानों, अब इस पुरुष को महल में ले जाकर, इसकी पाँच काम-भोग से सेवा की व्यवस्था करो।”
“ठीक है।” उत्तर देकर वे उस पुरुष को महल में ले जाकर, उसकी पाँच काम-भोग से सेवा का व्यवस्था करे।
तब क्या लगता है, राजन्य? क्या उस पुरुष को इस तरह अच्छे से नहाने पर, अच्छे से उबटन लगाने पर, अच्छे से केश-दाढ़ी बनाने पर, महँगी मालाएँ, लेप और उजले वस्त्र पहनने पर, महल में जाकर पाँच काम-भोग में लिप्त होकर, अच्छे से सेवित होने पर—फिर से विष्ठा में डूबने की इच्छा होगी?”
“नहीं, श्रीमान कश्यप।”
“क्यों नहीं होगी?”
“क्योंकि, श्रीमान कश्यप, विष्ठा गंदी होती है, गंदगी से बनी होती है, बदबूदार होती है, बदबू से भरी होती है, घिनौनी होती है, घिन से बनी होती है, प्रतिकूल होती है, प्रतिकूलता से बनी होती है।”
“उसी तरह, राजन्य, मानव भी देवताओं के लिए गंदा होता है, गंदगी से बना होता है, बदबूदार होता है, बदबू से भरा होता है, घिनौना होता है, घिन से बना होता है, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूलता से बना होता है। सौ योजन दूर से ही मानवों की बदबू देवताओं को आने लगती है। तब आपके जो मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या, चोरी और व्यभिचार से विरत रहते हैं, झूठ, फूट डालने वाली, कटु और निरर्थक बातों से विरत रहते हैं, लालची और दुर्भावनापूर्ण से विरत होकर सम्यक-दृष्टि धारण करते हैं, वे मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर स्वर्ग में उपजते हो, क्या वे आकर आपको बताएँगे, ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं’?
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(३) “ऐसा है, श्रीमान कश्यप, कि मेरे कुछ मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या से विरत, चोरी से विरत, व्यभिचार से विरत, झूठ बोलने से विरत, और शराब मद्य आदि मदहोश करने वाले नशेपते से विरत रहते हैं [=पञ्चशील]। कुछ समय पश्चात, वे बीमार पड़ते हैं, किसी दर्दभरे गंभीर रोग से पीड़ित। और, जब मुझे पता चलता है कि ‘वे अपनी बीमारी से ठीक नहीं होंगे’, तब मैं उनके पास जाकर कहता हूँ, “श्रीमान, कई श्रमण-ब्राह्मणों की ऐसी धारणा, ऐसी दृष्टि हैं कि ‘जो जीवहत्या से विरत, चोरी से विरत, व्यभिचार से विरत, झूठ बोलने से विरत, और शराब मद्य आदि मदहोश करने वाले नशेपते से विरत रहते हैं, वे मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर स्वर्ग में उपजते हैं। आप भी, श्रीमान, जीवहत्या से विरत, चोरी से विरत, व्यभिचार से विरत, झूठ बोलने से विरत, और शराब मद्य आदि मदहोश करने वाले नशेपते से विरत रहे हैं। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों की बात सच्ची है, तो श्रीमान, मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर, आप स्वर्ग में उपजेंगे। यदि वाकई ऐसा हो, श्रीमान, कि मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर, आप स्वर्ग में उपजे, तो मुझे आकर बताएं कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’ मुझे, श्रीमान, आप पर श्रद्धा है, विश्वास है। जो श्रीमान ने देख लिया, मानो मैंने स्वयं देख लिया।’
वे मुझे साधुकार देते हैं, किन्तु उनमें से भी आज तक न कोई मेरे पास आया, न ही किसी ने दूत ही भेजा। इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.४ तैतीस देवताओं की उपमा
“ठीक है, राजन्य, तब मैं आप से प्रतिप्रश्न करता हूँ। जैसे आप को ठीक लगे, वैसा उत्तर दें। ऐसा है, राजन्य, कि मानवों के सौ-वर्ष तैतीस देवताओं के लिए एक दिन-रात के बराबर है। ऐसे तीस दिन-रात का एक महिना होता है, और ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष। ऐसे एक हजार दिव्य वर्ष [=३ करोड़ ६० लाख मानव वर्ष] तैतीस देवताओं की आयु होती है।
अब, राजन्य, आपके जो मित्र-सहचारी और रिश्तेदार-संबंधी जीवहत्या से विरत, चोरी से विरत, व्यभिचार से विरत, झूठ बोलने से विरत, और शराब मद्य आदि मदहोश करने वाले नशेपते से विरत रहने पर, मरणोपरांत काया छूटने पर सद्गति होकर तैतीस देवलोक में उपजते होंगे, यदि उन्हें लगे कि, ‘मैं पहले दो-तीन दिन-रात पाँच दिव्य कामभोग में लिप्त होकर उसका सेवन कर लूँ, तब जाकर पायासि राजन्य को बताऊंगा कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’ तो क्या वे आकर, आपको बता पाएँगे?”
“नहीं, श्रीमान कश्यप! क्योंकि तब तक मैं बहुत पहले ही मर चुका रहूँगा। किन्तु, श्रीमान कश्यप, आप को किसने बता दिया कि ‘तैतीस देवता होते हैं’, या ‘तैतीस देवताओं की इतनी दीर्घायु होती है?’ मुझे श्रीमान कश्यप पर विश्वास नहीं है कि ‘तैतीस देवता होते हैं’, या ‘तैतीस देवताओं की इतनी दीर्घायु होती है।’”
२.५ जन्म से अंधे की उपमा
“कल्पना करें, राजन्य, कि कोई जन्म से अंधा पुरुष न काला रूप देखता है, न उजला रूप देखता है, न नीला रूप देखता है, न पीला रूप देखता है, न लाल रूप देखता है, न गुलाबी देखता है, न सम-विषम देखता है, न तारें देखता है, न चाँद-सूरज देखता है। वे कहेंगे, “न काले-उजले रूप होते हैं, और न ही कोई काले-उजले रूप देख सकता है। न नीले-पीले रूप होते हैं, और न ही कोई नीले-पीले रूप देख सकता है। न लाल-गुलाबी रूप होते हैं, और न ही कोई लाल-गुलाबी रूप देख सकता है। न सम-विषम होता हैं, न ही कोई सम-विषम देख सकता है। न तारे होते हैं, और न ही कोई तारे देख सकता है। न चाँद-सूरज होता है, और न ही कोई चाँद-सूरज देख सकता है। क्योंकि उन्हें मैं नहीं जानता, नहीं देखता, इसलिए वे होते ही नहीं हैं।” तो, राजन्य, क्या उनका ऐसा कहना सही हैं?”
“नहीं, श्रीमान कश्यप। काले-उजले रूप होते हैं, और काले-उजले रूप देखे जाते हैं। नीले-पीले रूप होते हैं, और नीले-पीले रूप देखे जाते हैं। लाल-गुलाबी रूप होते हैं, और लाल-गुलाबी रूप देखे जाते हैं। सम-विषम होते हैं, और सम-विषम देखे जाते हैं। तारे होते हैं, और तारे देखे जाते हैं। और, चाँद-सूरज होते हैं, और चाँद-सूरज देखे भी जाते हैं। क्योंकि उन्हें मैं नहीं जानता, नहीं देखता, इसलिए वे होते ही नहीं हैं।” उनका ऐसा कहना सही नहीं हैं।”
“उसी जन्म से अंधे की तरह, राजन्य, आप मुझे लगते है, जब आप मुझे कहते है कि “मुझे श्रीमान कश्यप पर विश्वास नहीं है कि ‘तैतीस देवता होते हैं’, या ‘तैतीस देवताओं की इतनी दीर्घायु होती है।’ जैसे आप को लगता है, राजन्य, वैसे माँसल-चक्षु [=शारीरिक आँख] से परलोक नहीं देखा जाता हैं। बल्कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण होते हैं जो निर्जन अरण्य में रहते हैं, दूर एकांतवास में रहते हैं, जो बिना लापरवाह हुए तत्पर और दृढ़-निश्चयी होकर विहार करते हैं। वे अपने दिव्य-चक्षु को निर्मल करते हैं, और अपने मनुष्योत्तर विमल दिव्य-चक्षु से यह लोक देखते हैं, परलोक देखते हैं, स्वयं से प्रकट होते सत्व देखते हैं। इस तरह, राजन्य, परलोक को देखा जाता है। जैसे आप को लगता है, वैसे माँसल-चक्षु से परलोक नहीं देखा जाता हैं।
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(४) “ऐसा है, श्रीमान कश्यप, कि मैं ऐसे श्रमण-ब्राह्मणों को देखता हूँ जो शीलवान और कल्याणधर्मी [=कल्याणकारी स्वभाव के] हैं, जो जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, जो सुखी रहना चाहते हैं, दुःखों से दूर हटते हैं। तब मुझे लगता है, “यदि इन शीलवान और कल्याणधर्मी श्रमण-ब्राह्मणों महाशय जानते हैं कि ‘मरने के बाद श्रेष्ठ [फल] होगा!’ तब उन्हें विष खा लेना चाहिए, शस्त्र भोंक देना चाहिए, फाँसी लगाकर मर जाना चाहिए, खाई से कूद जाना चाहिए। या उन शीलवान और कल्याणधर्मी श्रमण-ब्राह्मण महाशयों को ऐसा लगता नहीं होगा कि ‘मरने के बाद श्रेष्ठ होगा!’ इसलिए, वे जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, सुखी रहना चाहते हैं, दुःखों से दूर हटते हैं। इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.६ गर्भवती की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात हैं, राजन्य, किसी ब्राह्मण की दो पत्नियाँ थी। एक को दस या बारह वर्ष का पुत्र था, दूसरी गर्भवती थी। अब, वह ब्राह्मण मर गया। तब उस युवा-ब्राह्मण पुत्र ने अपनी सौतेली-माँ से कहा, “श्रीमति जी, जितना भी धन, धान्य, चाँदी, और स्वर्ण है, सब मेरा है! तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे पिता की विरासत सौंप दो।”
ऐसा कहे जाने पर, उस ब्राह्मणी ने युवा-ब्राह्मण से कहा, “प्रिय, मेरे जन्म देने तक रुक जाओ। यदि लड़का हुआ तो एक हिस्सा उसका भी होगा। और यदि लड़की हुई तो तुम्हारे उपभोग के लिए ही होगी।”
दूसरी बार, उस युवा-ब्राह्मण ने अपनी सौतेली-माँ से कहा, “नहीं, श्रीमति जी। जितना भी धन, धान्य, चाँदी, और स्वर्ण है, सब मेरा है! तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे पिता की विरासत सौंप दो।”
ऐसा कहे जाने पर, फिर उस ब्राह्मणी ने युवा-ब्राह्मण से कहा, “प्रिय, मेरे जन्म देने तक रुक जाओ। यदि लड़का हुआ तो एक हिस्सा उसका भी होगा। और यदि लड़की हुई तो तुम्हारे उपभोग के लिए ही होगी।”
तब तीसरी बार, उस युवा-ब्राह्मण ने अपनी सौतेली-माँ से कहा, “नहीं, श्रीमति जी। जितना भी धन, धान्य, चाँदी, और स्वर्ण है, सब मेरा है! तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे पिता की विरासत सौंप दो।”
तब, उस ब्राह्मणी ने तेज़ शस्त्र लेकर भीतरी कक्ष में गयी, और अपना पेट फाड़ दिया, [सोचते हुए,] “अभी जन्म देकर देखना चाहिए, लड़का है या लड़की?” उसने स्वयं के जीवन के साथ-साथ अपनी गर्भ-संपत्ति को भी नष्ट कर दिया।
जैसे, अनुचित तरह से विरासत चाहती उस मूर्ख और अनुभवहीन स्त्री का विनाश हो गया, उसी तरह, राजन्य, अनुचित तरह से परलोक ढूँढते आप जैसे मूर्ख और अनुभव-हीन का भी विनाश होगा। कोई शीलवान और कल्याणधर्मी श्रमण-ब्राह्मण अपने बिना-पके [फल] को [जबरन] नहीं पकाते हैं, बल्कि वे उसके पकने तक रुकते हैं। क्योंकि, राजन्य, जो शीलवान और कल्याणधर्मी श्रमण-ब्राह्मण विद्वान होते हैं, उनका जीवन अर्थपूर्ण होता है। जितने दीर्घकाल तक ऐसे शीलवान और कल्याणधर्मी श्रमण-ब्राह्मण जीवित रहते हैं, तब तक बहुत पुण्य करते हैं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, इस दुनिया पर उपकार करते हुए, देव और मानव के कल्याण, हित और सुख के लिए कार्यरत रहते हैं।
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(५) “जब ऐसा होता हैं, श्रीमान कश्यप, कि मेरे पुरुष किसी चोर या अपराधी को पकड़कर मेरे सामने पेश करते हैं, [कहते हुए,] “स्वामी, यह अपराधी चोर है। जैसी आपकी इच्छा हो, उसे वैसा दंड दें।”
तब मैं कहता हूँ, “ठीक है, श्रीमानों। इस पुरुष को जिंदा ही एक बड़े हंडे में डाल, गीले चमड़े से मुँह बंद कर, गीली मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाकर चूल्हे पर रखकर आग लगा दो।”
“ठीक है।” उत्तर देते हुए, वे उस पुरुष को जिंदा ही एक बड़े हंडे में डाल, गीले चमड़े से मुँह बंद कर, गीली मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाकर चूल्हे पर रखकर आग लगा देते हैं। जब मुझे लगता है कि ‘पुरुष मर गया होगा’, तब हंडे को उतार कर धीरे से मुँह खोलकर देखता हूँ कि ‘काश उसके जीव को निकलते हुए देखूँ।’ किन्तु मैंने कभी किसी जीव को निकलते हुए नहीं देखा। इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.७ स्वप्न की उपमा
“ठीक है, राजन्य। मैं आप से प्रतिप्रश्न करता हूँ। जैसे आप को लगे, वैसा उत्तर दे। क्या आप को याद है, कभी दिन में सोते हुए स्वप्न देखना, जिसमें रमणीय उद्यान, रमणीय वनउद्यान, रमणीय भूमिउद्यान, या रमणीय पुष्करणी-उद्यान दिखा हो?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप। मुझे दिन में सोते हुए ऐसा स्वप्न देखना याद है, जिसमें रमणीय उद्यान, रमणीय वनउद्यान, रमणीय भूमिउद्यान, या रमणीय पुष्करणी-उद्यान दिखा था।”
“क्या उस समय आप की रक्षा कुबड़े, नाटे, बौने, और बच्चियाँ कर रही थी?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप। उस समय मेरी रक्षा कुबड़े, नाटे, बौने, और बच्चियाँ कर रही थी।”
“क्या उन्होंने आपके जीव को प्रवेश करते या निकलते हुए देखा?”
“नहीं, श्रीमान कश्यप।”
“जब, राजन्य, वे आपके जीवित रहते हुए भी आपके जीव को प्रवेश करते या निकलते हुए नहीं देख सकते, तब भला आप कैसे किसी के मरने पर उसके जीव को प्रवेश करते या निकलते हुए देख सकते है?
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(६) “जब ऐसा होता हैं, श्रीमान कश्यप, कि मेरे पुरुष किसी चोर या अपराधी को पकड़कर मेरे सामने पेश करते हैं, [कहते हुए,] “स्वामी, यह अपराधी चोर है। जैसी आपकी इच्छा हो, उसे वैसा दंड दें।”
तब मैं कहता हूँ, “ठीक है, श्रीमानों। इस पुरुष को जिंदा रख तराजू पर तौल दो। फिर उसे रस्सी से गला घोटकर मार दो, और फिर तराजू पर तौल दो।
“ठीक है” उत्तर देते हुए वे उस पुरुष को जिंदा रख तराजू पर तौलते हैं। फिर उसे रस्सी से गला घोटकर मारने पर फिर तराजू पर तौलते हैं। जब तक जीवित रहे, तब तक वे तुलना में अधिक हल्के होते हैं, मृदु होते हैं, लचीले होते हैं। किन्तु, मरने पर वे तुलना में अधिक भारी, कठोर और सख्त हो जाते हैं।
इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.८ तप्त लौहगोले की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। कल्पना करे कि कोई पुरुष दिन भर तपाकर जलते, धधकते, चमकते लौहगोले को तराजू पर तौलता है। फिर कुछ समय पश्चात शीतल हो जाने पर फिर तराजू पर तौलता है। तो, कब वह लौहगोला तुलना में अधिक हल्का, मृदु, और लचीला होगा—जब वह जलता, धधकता, चमकता हो, अथवा जब शीतल हो चुका हो?”
“श्रीमान कश्यप, जब तक वह लौहगोला अग्नि के साथ और वायु के साथ, जलता, धधकता, चमकता होगा, तब वह तुलना में अधिक हल्का, मृदु, और लचीला होगा। किन्तु, जब वह लौहगोला न अग्नि के साथ, न ही वायु के साथ हो, बल्कि शीतल होकर बुझ चुका हो, तब वह तुलना में अधिक भारी, कठोर और सख्त हो जाएगा।”
उसी तरह, राजन्य, जब तक यह काया आयु के साथ, ऊष्मा के साथ, चैतन्य के साथ होती है, तब वह तुलना में अधिक हल्की, मृदु, और लचीली होती है। किन्तु, जब यह काया न आयु के साथ, न ऊष्मा के साथ, और न ही चैतन्य के साथ होती है, तब वह तुलना में अधिक भारी, कठोर और सख्त हो जाती है।
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(७) “जब ऐसा होता हैं, श्रीमान कश्यप, कि मेरे पुरुष किसी चोर या अपराधी को पकड़कर मेरे सामने पेश करते हैं, [कहते हुए,] “स्वामी, यह अपराधी चोर है। जैसी आपकी इच्छा हो, उसे वैसा दंड दें।”
तब मैं कहता हूँ, “ठीक है, श्रीमानों। इस पुरुष की त्वचा, चर्म, माँस, नसें, हड्डियाँ, अस्थिमज्जा को बिना चोट पहुँचाए इसकी जान ले लो, ताकि हम उसका जीव निकलते हुए देखे।”
“ठीक है”, उत्तर देकर वे उस पुरुष की त्वचा, चर्म, माँस, नसें, हड्डियाँ, अस्थिमज्जा को बिना चोट पहुँचाए उसकी जान लेने लगते हैं। जब वह मरने पर आ जाता है, तब मैं उन्हें कहता हूँ, “श्रीमानों, इस पुरुष को सीधा लिटा दो, ताकि हम उसका जीव निकलते हुए देखे।”
तब वे उस पुरुष को सीधा लिटाते हैं। किन्तु, मैं उसका जीव निकलते हुए नहीं देखता हूँ। तब मैं उन्हें कहता हूँ, “अब, श्रीमानों, इस पुरुष को उल्टा लिटा दो… दायी करवट लिटा दो… बायी करवट लिटा दो… सीधा खड़ा कर दो… उल्टा लटका दो… हाथ से मारो… पत्थर से मारो… डंडे से मारो… शस्त्र से मारो… अच्छे से हिलाओ-डुलाओ, ताकि हम उसका जीव निकलते हुए देखे।”
“ठीक है”, उत्तर देकर वे उस पुरुष को उल्टा लिटाते हैं… दायी करवट लिटाते हैं… बायी करवट लिटाते हैं… सीधा खड़ा करते हैं… उल्टा लटकाते हैं… हाथ से मारते हैं… पत्थर से मारते हैं… डंडे से मारते हैं… शस्त्र से मारते हैं… अच्छे से हिलाते-डुलाते हैं। किन्तु, मैं उसका जीव निकलते हुए नहीं देखता हूँ। उसके लिए आँखें होती हैं, रूप होते हैं, किन्तु वह उस आयाम पर कोई अनुभूति नहीं करता है। उसके लिए कान होते हैं, आवाज़े होती हैं, किन्तु वह उस आयाम पर कोई अनुभूति नहीं करता है। उसके लिए नाक होती हैं, गंध होती हैं, किन्तु वह उस आयाम पर कोई अनुभूति नहीं करता है। उसके लिए जीभ होती हैं, रस होते हैं, किन्तु वह उस आयाम पर कोई अनुभूति नहीं करता है। उसके लिए काया होती हैं, संस्पर्श होते हैं, किन्तु वह उस आयाम पर कोई अनुभूति नहीं करता है।
इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.९ शंख की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, किसी शंखधारी ने अपना शंख लेकर दूर-दराज के इलाके में गया। वह किसी गाँव में गया और गाँव के बीच खड़ा होकर अपने शंख का तीन बार ज़ोर से नाद किया। और, तब उसने अपना शंख नीचे भूमि पर रखकर एक ओर बैठ गया।
तब, राजन्य, उस सीमांत दूर-दराज के इलाके के लोगों को लगा, “हाय, किसका ऐसा आवाज है, जो इतना आकर्षक, इतना कामुक, इतना मोहक, [मन को] इतना बांधने वाला, इतना मदहोश करने वाला है!”
तब उन्होंने एकत्र होकर शंखधारी से कहा, “अरे, किसका ऐसा आवाज है, जो इतना आकर्षक, इतना कामुक, इतना मोहक, इतना बांधने वाला, इतना मदहोश करने वाला है!”
“यह आवाज, श्रीमानों, जिसे शंख कहते हैं, उससे निकला है, जो इतना आकर्षक, इतना कामुक, इतना मोहक, इतना बांधने वाला, इतना मदहोश करने वाला है!”
तब वे लोग उस शंख को सीधा लिटाते हैं, [कहते हुए,] “बोलो, श्रीमान शंख! बोलो, श्रीमान शंख!” उस शंख ने आवाज नहीं किया। तब वे लोग उस शंख को उल्टा लिटाते हैं… दायी करवट लिटाते हैं… बायी करवट लिटाते हैं… सीधा खड़ा करते हैं… उल्टा लटकाते हैं… हाथ से मारते हैं… पत्थर से मारते हैं… डंडे से मारते हैं… शस्त्र से मारते हैं… अच्छे से हिलाते-डुलाते हैं, [कहते हुए,] “बोलो, श्रीमान शंख! बोलो, श्रीमान शंख!” उस शंख ने आवाज नहीं किया।
तब, राजन्य, उस शंखधारी को लगा, “बड़े मूर्ख हैं इस सीमांत इलाके के लोग! भला कौन इतने अनुचित तरह से शंख का आवाज ढूँढता है?”
तब, उसने लोगों को दिखाते हुए शंख उठाया और तीन बार ज़ोर से बजाया, और तब उसे लेकर चल पड़ा। तब, राजन्य, उस सीमांत इलाके के लोगों को लगा, “ओह, लगता है कि जिसे शंख कहते हैं, जब वह पुरुष के साथ, मेहनत के साथ, और वायु के साथ होता है, तभी वह शंख आवाज करता है। किन्तु, जब शंख न पुरुष के साथ, न मेहनत के साथ, और न ही वायु के साथ हो, तब वह शंख आवाज नहीं करता है।
उसी तरह, राजन्य, जब यह काया आयु के साथ, ऊष्मा के साथ, चैतन्य के साथ होती है, तभी यह आगे बढ़ती है, लौट आती है, खड़ी होती है, बैठती है, या लेटती है, और आँखों से रूप देखती है, कानों से आवाज सुनती है, नाक से गंघ सूँघती है, जीभ से रस चखती है, काया से संस्पर्श अनुभव करती है, और मन से स्वभाव समझती है। किन्तु, जब यह काया न आयु के साथ, न ऊष्मा के साथ, न ही चैतन्य के साथ होती है, तब यह न आगे बढ़ती है, न लौट आती है, न खड़ी होती है, न बैठती है, न ही लेटती है, और न आँखों से रूप देखती है, न कानों से आवाज सुनती है, न नाक से गंघ सूँघती है, न जीभ से रस चखती है, न काया से संस्पर्श अनुभव करती है, और न ही मन से स्वभाव समझती है।
इस तरह, राजन्य, आप को समझना चाहिए कि ‘परलोक होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम होते हैं।’”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, तब भी मुझे लगता है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किन्तु, राजन्य, क्या आप के पास और कोई तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप कहते हैं कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप, मैं तर्क के आधार पर कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
“किस तरह, राजन्य?”
(८) “जब ऐसा होता हैं, श्रीमान कश्यप, कि मेरे पुरुष किसी चोर या अपराधी को पकड़कर मेरे सामने पेश करते हैं, [कहते हुए,] “स्वामी, यह अपराधी चोर है। जैसी आपकी इच्छा हो, उसे वैसा दंड दें।”
तब मैं कहता हूँ, “ठीक है, श्रीमानों, इस पुरुष की त्वचा काटकर निकालो। ताकि हमें इसका जीव दिखायी दे।”
“ठीक है।” उत्तर देते हुए वे उस पुरुष की त्वचा काटकर निकालते हैं। किन्तु, हमें उसका जीव नहीं दिखायी देता हैं।
तब मैं कहता हूँ, “ठीक है, श्रीमानों, इस पुरुष का चर्म… माँस… नसें… हड्डियाँ… अस्थिमज्जा काटकर निकालो। ताकि हमें इसका जीव दिखायी दे।”
“ठीक है।” उत्तर देते हुए वे उस पुरुष का चर्म… माँस… नसें… हड्डियाँ… अस्थिमज्जा काटकर निकालते हैं। किन्तु, हमें उसका जीव नहीं दिखायी देता हैं।
इस तर्क के आधार पर, श्रीमान कश्यप, मैं कहता हूँ कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’”
२.१० अग्निक जटाधारी की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, कोई अग्निक [=अग्नि की उपासना और पुजा करने वाला] जटाधारी [साधू] जंगली इलाके में पर्णकुटी [=पत्तियों से बनी कुटी] में रहता था। तब वहाँ किसी दूर-दराज के इलाके से एक [व्यापारियों का] कारवाँ आया। वह उस अग्निक जटाधारी के आश्रम के पास एक रात रुका और फिर चला गया।
तब, राजन्य, उस अग्निक जटाधारी को लगा, “क्यों न मैं उस कारवाँ की जगह पर जाऊँ, ताकि वहाँ कोई मेरे काम की चीज मिल जाएँ?” तब वह अग्निक जटाधारी उस कारवाँ की जगह पर गया। वहाँ जाने पर उसे पीछे छोड़ा एक नन्हा, सीधा लेटा हुआ, मतिमंद बच्चा दिखा। देखकर उसे लगा, “यह तो मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मानव बना यह मेरे देखते मर जाए। क्यों न मैं इस बच्चे को अपने आश्रम ले जाऊँ, और उसे पालकर बड़ा करूँ?”
तब उस अग्निक जटाधारी ने उस बच्चे को अपने आश्रम ले गया, और उसे पालकर बड़ा किया। जब वह बच्चा दस या बारह वर्ष का हुआ, तब अग्निक जटाधारी को देहात जाने का कोई काम पड़ा। तब उसने बच्चे से कहा, “प्रिय, मेरी देहात जाने की इच्छा है। तब तक, प्रिय, अग्नि की सेवा करना। उस अग्नि को बुझने मत देना। यदि अग्नि बुझ जाए, तो यह कुल्हाड़ी है, यह लकड़ियाँ हैं, ये दोनों अरणी भी साथ हैं। अग्नि उत्पन्न कर फिर से अग्नि की सेवा करना।” इस तरह, वह अग्निक जटाधारी बच्चे को अनुशासन कर देहात चला गया।
तब, खेल में लगे रहने से अग्नि बुझ गयी। उस बच्चे को लगा, “मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि ‘प्रिय, अग्नि की सेवा करना। उस अग्नि को बुझने मत देना। यदि अग्नि बुझ जाए, तो यह कुल्हाड़ी है, यह लकड़ियाँ हैं, ये दोनों अरणी भी साथ हैं। अग्नि उत्पन्न कर फिर से अग्नि की सेवा करना।’ क्यों न मैं अग्नि को उत्पन्न कर फिर से अग्नि की सेवा करूँ?”
तब उस बच्चे ने [कुल्हाड़ी से] अरणी के दो टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए, चार टुकड़े कर दिए, पाँच टुकड़े कर दिए, दस टुकड़े कर दिए, सौ टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को कूट डाला, ओखल में डालकर पीस डाला, और उसे पवन में उड़ा दिया, [सोचते हुए,] “इस तरह अग्नि उत्पन्न होगी!” किन्तु, अग्नि उत्पन्न नहीं हुई।
तब, अग्निक जटाधारी ने देहात में अपना काम खत्म किया और अपने आश्रम में लौटा। आश्रम में जाकर बच्चे से कहा, “प्रिय, अग्नि बुझी तो नहीं?”
“पिताजी, मैं खेल में लगे रहने से अग्नि बुझ गयी। मुझे लगा, “आप ने मुझसे कहा था कि ‘प्रिय, अग्नि की सेवा करना…” तब मैंने [कुल्हाड़ी से] अरणी के दो टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर दिए… सौ टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों को कूट डाला, ओखल में डालकर पीस डाला, और उसे पवन में उड़ा दिया, [सोचते हुए,] “इस तरह अग्नि उत्पन्न होगी!” किन्तु, अग्नि उत्पन्न नहीं हुई।”
तब, उस अग्निक जटाधारी को लगा, “बड़ा मूर्ख है यह बच्चा! कोई कितने अनुचित तरीके से अग्नि ढूँढ सकता है?”
तब उसने बच्चे को दिखाते हुए अरणी को उठाकर अग्नि उत्पन्न की, और बच्चे से कहा, “इस तरह, प्रिय, अग्नि उत्पन्न करते हैं। उस मूर्ख और अनुभवहीन अनुचित तरह से नहीं, जिस तरह तुम अग्नि जलाना ढूँढ रहे थे।”
ठीक उसी तरह, राजन्य, आप भी मूर्ख और अनुभवहीन होकर अनुचित तरह से परलोक ढूँढ रहे हैं। यह पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दीजिए, राजन्य! त्याग दीजिए इस पापी मिथ्या-धारणा को! अपने लिए दीर्घकाल तक अहित और दुःख मत खड़ा होने दो।”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, किन्तु मैं तब भी इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग नहीं सकता। कोसलराज प्रसेनजित के साथ-साथ कई अन्य राजा भी जानते हैं कि ‘पायासि राजन्य की ऐसी धारणा है, ऐसी दृष्टि है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’’ यदि मैं इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दूँ, तो लोग कहेंगे, “कितना मूर्ख और अनुभवहीन है पायासि राजन्य, जो मिथ्या में पड़ा हुआ था!” इसलिए मैं क्रोधित रहते हुए भी इसी [धारणा] को ढोता रहूँगा! घृणित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! तिरस्कारित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा!”
२.११ दो कारवाँओं की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, एक हजार गाड़ियों का विशाल कारवाँ पूर्व राज्यों के इलाके से पश्चिम राज्यों के इलाके में जा रहे थे। वे जहाँ-जहाँ जाते, वहाँ के सब घास, लकड़ियाँ, जल और हरियाली व्यय हो जाती। उस समय उस कारवाँ के दो मालिक थे, दोनों पाँच-पाँच सौ गाड़ियों के मालिक।
उन दोनों को लगा, “यह एक हजार गाड़ियों का विशाल कारवाँ है। हम जहाँ-जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के सब घास, लकड़ियाँ, जल और हरियाली व्यय हो जाती है। क्यों न हम इसे दो में विभाजित कर दे—एक में पाँच सौ गाडियाँ, और दूसरे में पाँच सौ गाडियाँ।”
तब दोनों ने उसे दो में विभाजित कर दिया—एक में पाँच सौ गाडियाँ, और दूसरे में पाँच सौ गाडियाँ। एक मालिक ने बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल लेकर कारवाँ आगे बढ़ाया। दो-तीन दिन बीतने पर उसने एक काले पुरुष को सामने से आते देखा, जिसकी आँखें लाल थी, जो तीर-धनुष लिए, कुमुद की माला पहले, भीगे वस्त्र और भीगे केश के साथ, कीचड़ लगे चक्कों वाले सुंदर रथ पर सवार था। देखकर बोला, “श्रीमान, कहाँ से आ रहे है?”
“अमुक इलाके से।”
“कहाँ जा रहे है?”
“अमुक नाम के इलाके में।”
“श्रीमान, क्या रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है?”
“हाँ, श्रीमान, रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है। मार्ग जल से भर गया है, और आगे बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल है। श्रीमान, अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दो। हल्का होकर तुम्हारा कारवाँ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेगा। खींचने वाले [जानवरों] को मत थकाओ।”
तब, उस कारवाँ के मालिक ने अपने कारवाँ को संबोधित किया, “यह पुरुष कहता है कि ‘रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है। मार्ग जल से भर गया है, और आगे बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल है। श्रीमान, अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दो। हल्का होकर तुम्हारा कारवाँ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेगा। खींचने वाले को मत थकाओ।’ तब, श्रीमानों, पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दो। हल्का कर के कारवाँ आगे बढ़ाते हैं।”
“ठीक है, श्रीमान।” उत्तर देकर कारवाँ के लोगों ने अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दिया। और, हल्का कर के कारवाँ आगे बढ़ाया।
किन्तु, पहले कारवाँ-स्थल पर उन्हें कोई घास, लकड़ी या जल नहीं दिखा। दूसरे कारवाँ-स्थल पर भी… तीसरे कारवाँ-स्थल पर भी… चौथे कारवाँ-स्थल पर भी… पाँचवे कारवाँ-स्थल पर भी… छठे कारवाँ-स्थल पर भी… और, सातवे कारवाँ-स्थल पर भी उन्हें कोई घास, लकड़ी या जल नहीं दिखा। वे सभी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तबाही में गिर पड़े। उस कारवाँ के जितने भी मनुष्य और पशु थे, सभी को यक्षों और अमनुष्यों ने खा लिया। वहाँ केवल हड्डियाँ ही रह गयी।
और, उधर जब दूसरे कारवाँ के मालिक को लगा, “पहले कारवाँ को निकले बहुत दिन बीत गए”, तब उसने बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल लेकर कारवाँ आगे बढ़ाया। दो-तीन दिन बीतने पर उसने भी एक काले पुरुष को सामने से आते देखा, जिसकी आँखें लाल थी, जो तीर-धनुष लिए, कुमुद की माला पहले, भीगे वस्त्र और भीगे केश के साथ, कीचड़ लगे चक्कों वाले सुंदर रथ पर सवार था। देखकर बोला, “श्रीमान, कहाँ से आ रहे है?”
“अमुक इलाके से।”
“कहाँ जा रहे है?”
“अमुक नाम के इलाके में।”
“श्रीमान, क्या रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है?”
“हाँ, श्रीमान, रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है। मार्ग जल से भर गया है, और आगे बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल है। श्रीमान, अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दो। हल्का होकर तुम्हारा कारवाँ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेगा। खींचने वाले को मत थकाओ।”
तब, उस कारवाँ के मालिक ने अपने कारवाँ को संबोधित किया, “यह पुरुष कहता है कि ‘रेगिस्तान में आगे महामेघ वर्षा हुई है। मार्ग जल से भर गया है, और आगे बहुत-सी घास, लकड़ियाँ और जल है। श्रीमान, अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल फेंक दो। हल्का होकर तुम्हारा कारवाँ जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेगा। खींचने वाले को मत थकाओ।’ किन्तु, श्रीमानों, यह पुरुष हमारा मित्र भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। हम कैसे उस पर विश्वास कर लें? हमें अपनी पुरानी घास, लकड़ियाँ और जल नहीं फेंकना चाहिए। बल्कि अपना सामान लेकर ही कारवाँ आगे बढ़ाते हैं।”
“ठीक है, श्रीमान।” उत्तर देकर कारवाँ के लोगों ने मालिक की सुनी, और अपना पुराना सामान लेकर कारवाँ आगे बढ़ाया।
तब, पहले कारवाँ-स्थल पर उन्हें कोई घास, लकड़ी या जल नहीं दिखा। दूसरे कारवाँ-स्थल पर भी… तीसरे कारवाँ-स्थल पर भी… चौथे कारवाँ-स्थल पर भी… पाँचवे कारवाँ-स्थल पर भी… छठे कारवाँ-स्थल पर भी… और, सातवे कारवाँ-स्थल पर भी उन्हें कोई घास, लकड़ी या जल नहीं दिखा। वहाँ उन्हें पहले कारवाँ की दुर्भाग्यपूर्ण तबाही दिख पड़ी। और उन्होंने पहले कारवाँ के जितने भी मनुष्य और पशु थे, उनकी बची हड्डियाँ देखी, जिन सभी को यक्षों और अमनुष्यों ने खा लिया था।
तब, उस कारवाँ के मालिक ने अपने कारवाँ को संबोधित किया, “इस कारवाँ की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तबाही हुई! जैसे मूर्ख मालिक वाले कारवाँओं के साथ होता ही है। तब, श्रीमानों, अपने गाड़ियों के जो भी सस्ते सामान हैं, उन्हें यही फेंक दो। और इस कारवाँ के जो भी महँगे सामान हैं, उन्हें लो।”
“ठीक है, श्रीमान।” उत्तर देकर कारवाँ के लोगों ने मालिक की सुनी, और अपनी गाड़ियों के सस्ते सामान वही फेंक दिए। और पहले कारवाँ के महँगे सामान लेकर कारवाँ आगे बढ़ाया। और, उन्होंने रेगिस्तान पार कर लिया। जैसे समझदार मालिक वाले कारवाँओं के साथ होता ही है।
ठीक उसी तरह, राजन्य, आप भी मूर्ख और अनुभवहीन होकर अनुचित तरह से परलोक ढूँढ रहे हैं। यह पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दीजिए, राजन्य! त्याग दीजिए इस पापी मिथ्या-धारणा को! अपने लिए दीर्घकाल तक अहित और दुःख मत खड़ा होने दो।”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, किन्तु मैं तब भी इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग नहीं सकता। कोसलराज प्रसेनजित के साथ-साथ कई अन्य राजा भी जानते हैं कि ‘पायासि राजन्य की ऐसी धारणा है, ऐसी दृष्टि है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’’ यदि मैं इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दूँ, तो लोग कहेंगे, “कितना मूर्ख और अनुभवहीन है पायासि राजन्य, जो मिथ्या में पड़ा हुआ था!” इसलिए मैं क्रोधित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! घृणित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! तिरस्कारित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा!”
२.१२ विष्ठा की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक और उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, कोई सुवर-पालक पुरुष अपने गाँव से किसी दूसरे गाँव गया। वहाँ उसने सूखी विष्ठा [गूह, मल] का ढ़ेर फेंका हुआ देखा। देखकर उसे लगा, “यह सूखी विष्ठा का ढ़ेर फेंका हुआ है, जो मेरे सुवरों का खाद्य है। क्यों न मैं इस सूखी विष्ठा को ढोकर ले चलूँ?”
तब उसने अपना बाहरी वस्त्र फैलाया, उसमें सूखी विष्ठा के ढ़ेर को एकत्र किया, और गठरी बांधकर सिर पर उठाकर चल पड़ा। रास्ते में बड़ी अकाल-वर्षा होने लगी। और, वह उस चूति और टपकती विष्ठा से [सिर से लेकर] नाखूनों तक पूर्ण लथपथ होकर ढ़ोते चलते रहा।
उसे देखकर लोगों ने कहा, “अरे भाई! पगला गए हो? बहक गए हो? कैसे चूति और टपकती विष्ठा से नाखूनों तक पूर्ण लथपथ होकर ढ़ोते चल सकते हो?”
“तुम ही पगला गए हो! तुम ही बहक गए हो! यह तो मेरे सुवरों का भोजन है।”
ठीक उसी तरह, राजन्य, मुझे आप भी विष्ठा ढ़ोते हुए ही लग रहे है। त्याग दीजिए इस पापी मिथ्या-धारणा को, राजन्य! छोड़ दीजिए, इस पापी मिथ्या-धारणा को! अपने लिए दीर्घकाल तक अहित और दुःख मत खड़ा होने दो।”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, किन्तु मैं तब भी इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग नहीं सकता। कोसलराज प्रसेनजित के साथ-साथ कई अन्य राजा भी जानते हैं कि ‘पायासि राजन्य की ऐसी धारणा है, ऐसी दृष्टि है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’’ यदि मैं इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दूँ, तो लोग कहेंगे, “कितना मूर्ख और अनुभवहीन है पायासि राजन्य, जो मिथ्या में पड़ा हुआ था!” इसलिए मैं क्रोधित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! घृणित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! तिरस्कारित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा!”
२.१३ जुवारी की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक और उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, दो जुवारी जुवा खेलते थे। उनमें से एक जुवारी हार-जीतकर पासे को निगल जाता था। दूसरे जुवारी ने उसे हार-जीतकर पासे को निगलते हुए देखा। देखकर उस जुवारी से कहा, “अरे, मित्र! तुमने तो सब कुछ जीत लिया। अभी पासे को मुझे दो। मैं फेकुंगा!”
“ठीक है, मित्र!” उत्तर देकर पहले जुवारी ने उसे पासा सौंपा। तब, दूसरे जुवारी ने उस पासे को विष में डुबाया और पहले जुवारी से कहा, “आओ, मित्र! अब खेलते हैं जुवा!”
“ठीक है, मित्र!” पहले जुवारी ने उत्तर दिया। तब, वे दूसरी बार उस पासे से खेलने लगे। और, दूसरी बार भी पहले जुवारी ने हार-जीतकर पासे को निगल लिया। तब दूसरे जुवारी ने उसे उस पासे को निगलते हुए देखा और कहा:
निगलते पुरुष को समझ न आया।
निगल रे, पापी धूर्त, निगल जा!
पश्चात तेरा कड़वा होगा!”
ठीक उसी तरह, राजन्य, मुझे आप उस जुवारी जैसे ही लग रहे है। त्याग दीजिए इस पापी मिथ्या-धारणा को, राजन्य! छोड़ दीजिए, इस पापी मिथ्या-धारणा को! अपने लिए दीर्घकाल तक अहित और दुःख मत खड़ा होने दो।”
“भले ही श्रीमान कश्यप ऐसा कहे, किन्तु मैं तब भी इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग नहीं सकता। कोसलराज प्रसेनजित के साथ-साथ कई अन्य राजा भी जानते हैं कि ‘पायासि राजन्य की ऐसी धारणा है, ऐसी दृष्टि है कि ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’’ यदि मैं इस पापी मिथ्या-धारणा को त्याग दूँ, तो लोग कहेंगे, “कितना मूर्ख और अनुभवहीन है पायासि राजन्य, जो मिथ्या में पड़ा हुआ था!” इसलिए मैं क्रोधित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! घृणित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा! तिरस्कारित रहते हुए भी इसी को ढोता रहूँगा!”
२.१४ सन की उपमा
“ठीक है, राजन्य, मैं आप को एक और उपमा देता हूँ। क्योंकि उपमा से कितने ही समझदार लोग बात का अर्थ समझ जाते हैं। बहुत पहले की बात है, राजन्य, दूर कोई राज्य खड़ा [समृद्ध] हुआ। तब एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, “आओ मित्र! उस राज्य में जाए। कम ही दिनों में कुछ धन कमा लाएँगे।”
“ठीक है, मित्र!” दूसरे मित्र ने उत्तर दिया। तब वे दोनों दूर के उस राज्य में गए। वहाँ किसी निर्जन गाँव में जाने पर, उन्हें सन [=जूट] का ढ़ेर पड़ा मिला। देखकर एक मित्र से दूसरे मित्र से कहा, “मित्र, यहाँ सन का ढ़ेर फेंका पड़ा है। ठीक है, मित्र, तुम इस सन का गठरी बांध लो, मैं भी इस सन की गठरी बांधता हूँ। दोनों ही इस सन की गठरियाँ ढ़ोते चलेंगे।”
“ठीक है, मित्र!” दूसरे मित्र ने उत्तर दिया। तब उन दोनों ने सन की गठरियाँ बांधकर ढ़ोते हुए किसी दूसरे निर्जन गाँव में गए। वहाँ उन्होंने सन के सूत का ढ़ेर पड़ा मिला। देखकर एक मित्र से दूसरे मित्र से कहा, “मित्र, जिसके लिए सन चाहिए, उसी सन-सूत का ढ़ेर यहाँ फेंका पड़ा है। ठीक है, मित्र, तुम अपने सन का ढ़ेर फेंक दो, मैं भी अपने सन का ढ़ेर फेंकता हूँ। दोनों ही इस सन-सूत का ढ़ेर ढ़ोते चलेंगे।”
“देखो, मित्र, मैं इस सन की गठरी को दूर से ढ़ोते ला रहा हूँ जो अच्छे से बंधी है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। 1 तुम समझ जाओ।”
तब, पहले मित्र ने सन की गठरी फेंककर सन-सूत की गठरी बांधी, और तब दोनों किसी दूसरे निर्जन गाँव में गए। वहाँ उन्होंने सन के वस्त्रों का ढ़ेर पड़ा मिला। देखकर एक मित्र से दूसरे मित्र से कहा, “मित्र, जिसके लिए सन-सूत चाहिए, उसी सन-वस्त्रों का ढ़ेर यहाँ फेंका पड़ा है। ठीक है, मित्र, तुम अपने सन का ढ़ेर फेंक दो, मैं भी अपने सन-सूत का ढ़ेर फेंकता हूँ। दोनों ही इस सन-वस्त्रों का ढ़ेर ढ़ोते चलेंगे।”
“देखो, मित्र, मैं इस सन की गठरी को दूर से ढ़ोते ला रहा हूँ जो अच्छे से बंधी है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। तुम समझ जाओ।”
तब, पहले मित्र ने सन-सूत की गठरी फेंककर सन-वस्त्रों की गठरी बांधी, और तब दोनों किसी दूसरे निर्जन गाँव में गए। वहाँ उन्होंने क्षौम [=अलसी का सन] का ढ़ेर… क्षौम-सूत का ढ़ेर… क्षौम-वस्त्रों का ढ़ेर… कपास का ढ़ेर… कपास-सूत का ढ़ेर… कपास-वस्त्रों का ढ़ेर… लोहे का ढ़ेर… तांबे का ढ़ेर… टिन का ढ़ेर… सीसे का ढ़ेर… चाँदी का ढ़ेर… स्वर्ण का ढ़ेर पड़ा मिला। देखकर एक मित्र से दूसरे मित्र से कहा, “मित्र, जिसके लिए सन, या सन-सूत, या सन-वस्त्र, या क्षौम, या क्षौम-सूत, या क्षौम-वस्त्र, या कपास, या कपास-सूत्र, या कपास-वस्त्र, या लोहा, या तांबा, या टिन, या सीसा, या चाँदी चाहिए, उसी स्वर्ण का ढ़ेर यहाँ फेंका पड़ा है। ठीक है, मित्र, तुम अपना सन का ढ़ेर फेंक दो, मैं भी अपने चाँदी का ढ़ेर फेंकता हूँ। दोनों ही इस स्वर्ण का ढ़ेर ढ़ोते चलेंगे।”
“देखो, मित्र, मैं इस सन की गठरी को दूर से ढ़ोते ला रहा हूँ जो अच्छे से बंधी है। मेरे लिए यही पर्याप्त है। तुम समझ जाओ।”
तब, पहले मित्र ने चाँदी की गठरी फेंककर स्वर्ण की गठरी बांधी, और तब दोनों अपने गाँव लौट गए। जब एक मित्र सन की गठरी लेकर घर गया, तो उसके माता-पिता ने उसका अभिनंदन नहीं किया, उसकी पत्नी और संतानों ने उसका अभिनंदन नहीं किया, उसके मित्रों और सहचारियों ने उसका अभिनंदन नहीं किया। उसके कारण उसे या किसी को सुख और हर्ष महसूस नहीं हुआ।
जबकि एक मित्र स्वर्ण की गठरी लेकर घर गया, तो उसके माता-पिता ने उसका अभिनंदन किया, उसकी पत्नी और संतानों ने उसका अभिनंदन किया, उसके मित्रों और सहचारियों ने उसका अभिनंदन किया। उस कारण उसे और सभी को बहुत सुख और हर्ष महसूस हुआ।
ठीक उसी तरह, राजन्य, मुझे आप उस सन की गठरी ढ़ोते जैसे ही लग रहे है। त्याग दीजिए इस पापी मिथ्या-धारणा को, राजन्य! छोड़ दीजिए, इस पापी मिथ्या-धारणा को! अपने लिए दीर्घकाल तक अहित और दुःख मत खड़ा होने दो।”
३. शरण जाना
“श्रीमान कश्यप, मैं आपकी पहली उपमा से ही हर्षित और प्रसन्न हो गया था। किन्तु मैंने इन भाँति-भाँति के प्रश्नोत्तरों को सुनने की इच्छा से ही श्रीमान कश्यप के विपरीत बातें कह रहा था। अतिउत्तम, श्रीमान कश्यप! अतिउत्तम, श्रीमान कश्यप! जैसे कोई पलटे को सीधा करे, छिपे को खोल दे, भटके को मार्ग दिखाए, या अँधेरे में दीप जलाकर दिखाए, ताकि तेज आँखों वाला स्पष्ट देख पाए—उसी तरह कश्यप गुरुजी ने धम्म को अनेक तरह से स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ! धम्म की और संघ की भी! कश्यप गुरुजी मुझे आज से लेकर प्राण रहने तक शरणागत उपासक धारण करें!
श्रीमान कश्यप, मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। मुझे निर्देश करे, कश्यप गुरुजी, जो मेरे दीर्घकाल के हित और सुख के लिए हो।”
४. यज्ञ कथा
“राजन्य, जिस यज्ञ में गायों की हत्या की जाती है, बकरियों की हत्या की जाती है, भेड़ों की हत्या की जाती है, मुर्गियों की हत्या की जाती है, सुवरों की हत्या की जाती है, विविध प्रकार के किसी अन्य प्राणियों को मौत के घाट उतारा जाता है, और जिसका आयोजक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कार्य, मिथ्या आजीविका, मिथ्या स्मृति, और मिथ्या समाधि को ग्रहण किए होता है, इस तरह के यज्ञ का, राजन्य, न महाफलदायी होता है, न महापुरस्कारी होता है, न महाउजला होता है, और न ही महाविस्तारी होता है।
जैसे, राजन्य, कोई किसान बीज और हल लेकर जंगल में प्रवेश करे। और वहाँ बुरे [=बंजर] क्षेत्र में, बुरे भूमि में, ठूँठ [=stump] और कँटीली झाड़ियों से भरे जगह पर ऐसे बीज बोये, जो टूट चुके हो, सड़ चुके हो, सूख चुके हो, बंजर हो चुके हो, अच्छे से न जमे हो। और आवश्यक समय होने पर देवता भी वर्षा न कराएँ। तब क्या वे बीज अंकुरित हो, वृद्धि और विपुलता प्राप्त करेंगे? और क्या उस किसान को भरपूर फल प्राप्त होंगे?”
“नहीं, श्रीमान कश्यप।”
“ठीक उसी तरह, राजन्य, जिस यज्ञ में गायों की हत्या की जाती है, बकरियों की हत्या की जाती है, भेड़ों की हत्या की जाती है, मुर्गियों की हत्या की जाती है, सुवरों की हत्या की जाती है, विविध प्रकार के किसी अन्य प्राणियों को मौत के घाट उतारा जाता है, और जिसका आयोजक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वचन, मिथ्या कार्य, मिथ्या आजीविका, मिथ्या स्मृति, और मिथ्या समाधि को ग्रहण किए होता है, इस तरह के यज्ञ का, राजन्य, न महाफलदायी होता है, न महापुरस्कारी होता है, न महाउजला होता है, और न ही महाविस्तारी होता है।
जैसे, राजन्य, कोई बीज और हल लेकर जंगल में प्रवेश करे। और अच्छे [=उपजाऊ] क्षेत्र में, अच्छी भूमि में, ठूँठ और कँटीली झाड़ियों से रहित जगह पर ऐसे बीज बोये, जो टूटे न हो, सड़े न हो, सूखे न हो, बंजर न हो, अच्छे से जमे हो। और आवश्यक समय होने पर देवता भी वर्षा कराएँ। तब क्या वे बीज अंकुरित हो, वृद्धि और विपुलता प्राप्त करेंगे? और क्या उस किसान को भरपूर फल प्राप्त होंगे?”
“हाँ, श्रीमान कश्यप।”
“ठीक उसी तरह, राजन्य, जिस यज्ञ में गायों की हत्या नहीं की जाती, बकरियों की हत्या नहीं की जाती, भेड़ों की हत्या नहीं की जाती, मुर्गियों की हत्या नहीं की जाती, सुवरों की हत्या नहीं की जाती, विविध प्रकार के किसी अन्य प्राणियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता, और जिसका आयोजक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि को ग्रहण किए होता है, इस तरह के यज्ञ का, राजन्य, महाफलदायी होता है, महापुरस्कारी होता है, महाउजला होता है, और महाविस्तारी होता है।
५. युवा-ब्राह्मण उत्तर
तब पायासि राजन्य ने श्रमण, ब्राह्मण, ग़रीब, घुमक्कड़, कंगाल तथा भिखारियों के लिए दान का आयोजन किया। और उस दान में वह ऐसा भोजन देता था जिसमें टूटे चावल की खिचड़ी, अचार के साथ दी जाएँ, और गठीलें किनारे वाले रूखे वस्त्र देता था। तब उस दान आयोजन का अधीक्षक ‘उत्तर’ नामक युवा-ब्राह्मण था, जो दान देते हुए उद्देश्य कहता था, “इस दान से मेरा और पायासि राजन्य का साथ इसी लोक तक रहे, परलोक में नहीं।”
पायासि राजन्य ने सुना कि युवा-ब्राह्मण उत्तर दान देते हुए उद्देश्य कहता है, ‘इस दान से मेरा और पायासि राजन्य का साथ इसी लोक तक रहे, परलोक में नहीं।’ तब पायासि राजन्य ने उत्तर युवा-ब्राह्मण को आमंत्रित कर कहा, “क्या यह सच है, प्रिय उत्तर, कि तुम दान देते हुए उद्देश्य कहते हो, ‘इस दान से मेरा और पायासि राजन्य का साथ इसी लोक तक रहे, परलोक में नहीं?’
“हाँ, श्रीमान!”
“किंतु, प्रिय उत्तर, क्यों तुम दान देते हुए उद्देश्य कहते हो कि ‘इस दान से मेरा और पायासि राजन्य का साथ इसी लोक तक रहे, परलोक में नहीं’? क्या हम पुण्य करते लोग उस दान के फल की आशा भी न रखें?”
“श्रीमान, उस दान में ऐसा भोजन दिया जाता हैं, टूटे चावल की खिचड़ी, अचार के साथ, जिस भोजन को खाना तो दूर, आप पैर से भी नहीं छुएँगे। उस दान में गठिलें किनारे वाले इतने रूखे वस्त्र दिए जाते हैं, जिसे पहनना तो दूर, आप पैर से भी नहीं छुएँगे। श्रीमान हमारे लिए प्रिय और पसंदीदा है। कैसे हम प्रिय और पसंदीदा को अनचाहे से जोड़ दें?”
“तब, प्रिय उत्तर, जैसा भोजन मैं करता हूँ, वैसा ही भोजन बांटने का इंतज़ाम करो। और जैसे वस्त्र मैं पहनता हूँ, वैसे ही वस्त्र बांटने का इंतज़ाम करो।”
“ठीक है, श्रीमान!” उत्तर देकर युवा-ब्राह्मण उत्तर ने ऐसा भोजन दान देने का इंतज़ाम किया, जैसे भोजन पायासि राजन्य करता था। और ऐसे वस्त्र दान देने का इंतज़ाम किया, जैसे वस्त्र पायासि राजन्य पहनता था।
तब पायासि राजन्य बिना ध्यान रखते हुए दान देने से, बिना स्वयं के हाथों से दान देने से, बिना सहानुभूति चित्त से दान देने से, ऐसे दान देने से कि मानो फेंक रहे हो, मरणोपरांत काया छूटने पर चार महाराजा देवताओं में रिक्त ‘शिरीष महल’ में उत्पन्न हुआ। जबकि युवा-ब्राह्मण उत्तर ध्यान रखते हुए दान देने से, स्वयं के हाथों से दान देने से, सहानुभूति चित्त से दान देने से मरणोपरांत काया छूटने पर तैतीस देवलोक में उत्पन्न हुआ।
६. देवपुत्र पायासि
तब, उस समय, आयुष्मान गवम्पति अक्सर दिन के समय ध्यान करने के लिए उस रिक्त शिरीष महल में जाते थे। तब, देवपुत्र पायासि आयुष्मान गवम्पति के पास गया, और अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। आयुष्मान गवम्पति ने एक ओर खड़े देवपुत्र पायासि से कहा, “आप कौन है, मित्र?”
“भन्ते, मैं पायासि राजन्य हूँ।”
“क्या आप ही की ऐसी धारणा थी, ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं’?”
“यह सच है, भन्ते, मेरी ही ऐसी धारणा थी, ‘परलोक नहीं होता है, स्वयं से प्रकट हुए सत्व नहीं होते हैं, भले और बुरे कर्मों के फल-परिणाम नहीं होते हैं।’ किन्तु मैं आर्य कुमार कश्यप के द्वारा उस पापी मिथ्या-धारणा से हटाया गया।”
“किन्तु मित्र, जो तुम्हारे दान को बाँटता था, उत्तर नामक युवा-ब्राह्मण, वह कहाँ उत्पन्न हुआ?”
“भन्ते, युवा-ब्राह्मण उत्तर ध्यान रखते हुए दान देने से, स्वयं के हाथों से दान देने से, सहानुभूति चित्त से दान देने से मरणोपरांत काया छूटने पर तैतीस देवलोक में उत्पन्न हुआ। जबकि मैं बिना ध्यान रखते हुए दान देने से, बिना स्वयं के हाथों से दान देने से, बिना सहानुभूति चित्त से दान देने से, ऐसे दान देने से कि मानो फेंक रहे हो, मरणोपरांत काया छूटने पर चार महाराजा देवताओं में इस रिक्त ‘शिरीष महल’ में उत्पन्न हुआ।
भन्ते गवम्पति, जब आप मानवलोक जाए, यह घोषणा करे कि ‘ध्यान रखते हुए दान दें, स्वयं के हाथों से दान दें, सहानुभूति चित्त से दान दें, ऐसे मत दें जैसे फेंक रहे हो। पायासि राजन्य बिना ध्यान रखते हुए दान देने से, बिना स्वयं के हाथों से दान देने से, बिना सहानुभूति चित्त से दान देने से, ऐसे दान देने से कि मानो फेंक रहे हो, मरणोपरांत काया छूटने पर चार महाराजा देवताओं में रिक्त शिरीष महल में उत्पन्न हुआ। जबकि युवा-ब्राह्मण उत्तर ध्यान रखते हुए दान देने से, स्वयं के हाथों से दान देने से, सहानुभूति चित्त से दान देने से मरणोपरांत काया छूटने पर [ऊँचे] तैतीस देवलोक में उत्पन्न हुआ।’”
तब, भन्ते गवम्पति मानवलोक गए और यह घोषणा की कि ‘ध्यान रखते हुए दान दें, स्वयं के हाथों से दान दें, सहानुभूति चित्त से दान दें, ऐसे मत दें जैसे फेंक रहे हो। पायासि राजन्य बिना ध्यान रखते हुए दान देने से, बिना स्वयं के हाथों से दान देने से, बिना सहानुभूति चित्त से दान देने से, ऐसे दान देने से कि मानो फेंक रहे हो, मरणोपरांत काया छूटने पर चार महाराजा देवताओं में रिक्त शिरीष महल में उत्पन्न हुआ। जबकि युवा-ब्राह्मण उत्तर ध्यान रखते हुए दान देने से, स्वयं के हाथों से दान देने से, सहानुभूति चित्त से दान देने से मरणोपरांत काया छूटने पर [ऊँचे] तैतीस देवलोक में उत्पन्न हुआ।’
सुत्त समाप्त।
|| महावर्ग समाप्त ||
-
इसे अँग्रेजी में “Sunk Cost Fallacy” कहते हैं। लोग अपने जीवन में किसी बात पर इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत समय, ऊर्जा, और भावनाएँ लगायी होती हैं। भले ही आगे चलकर वह मार्ग सही साबित न हो, लेकिन उसमें हो चुके निवेश के कारण अब उसे छोड़ना सरल नहीं लगता। उदाहरण के लिए, कोई फिल्म देखने जाए और लगे कि फिल्म खराब है। लेकिन टिकट के पैसे पहले ही दे दिए हो, तो फिल्म को बीच में छोड़ने के बजाय पूरी देख लेता है। इस तरह, वह पैसे के साथ-साथ अपना समय और मूड भी बर्बाद करता है। इसके बजाय, हमें जब भी पुराने निर्णय की गलती का बोध हो, और नयी दिशा प्रकट हो, तो यह समझना चाहिए कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। बहता पानी जीवन देता है, और रुका पानी सड़ते जाता है। समय-समय पर अपनी पुरानी गलतियों का बोध होना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को नयी सम्यक दिशा दे। ↩︎
पालि
४०६. एवं मे सुतं – एकं समयं आयस्मा कुमारकस्सपो कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन सेतब्या नाम कोसलानं नगरं तदवसरि। तत्र सुदं आयस्मा कुमारकस्सपो सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं सिंसपावने [सीसपावने (स्या॰)]। तेन खो पन समयेन पायासि राजञ्ञो सेतब्यं अज्झावसति सत्तुस्सदं सतिणकट्ठोदकं सधञ्ञं राजभोग्गं रञ्ञा पसेनदिना कोसलेन दिन्नं राजदायं ब्रह्मदेय्यं।
पायासिराजञ्ञवत्थु
४०७. तेन खो पन समयेन पायासिस्स राजञ्ञस्स एवरूपं पापकं दिट्ठिगतं उप्पन्नं होति – ‘‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं [सुकटक्कटानं (सी॰ पी॰)] कम्मानं फलं विपाको’’ति। अस्सोसुं खो सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका – ‘‘समणो खलु भो कुमारकस्सपो समणस्स गोतमस्स सावको कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सेतब्यं अनुप्पत्तो सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं सिंसपावने। तं खो पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो [बुद्धो (स्या॰ क॰)] चेव अरहा च। साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होती’’’ति। अथ खो सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतब्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन सिंसपावनं [येन सिंसपावनं, तेनुपसङ्कमन्ति (सी॰ पी॰)]।
४०८. तेन खो पन समयेन पायासि राजञ्ञो उपरिपासादे दिवासेय्यं उपगतो होति। अद्दसा खो पायासि राजञ्ञो सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके सेतब्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूते उत्तरेनमुखे गच्छन्ते येन सिंसपावनं [येन सिंसपावनं, तेनुपसङ्कमन्ते (सी॰ पी॰)], दिस्वा खत्तं आमन्तेसि – ‘‘किं नु खो, भो खत्ते, सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतब्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूता उत्तरेनमुखा गच्छन्ति येन सिंसपावन’’न्ति [एत्थ पन सब्बत्थपि एवमेव दिस्सति, नत्थि पाठन्तरं]?
‘‘अत्थि खो, भो, समणो कुमारकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सेतब्यं अनुप्पत्तो सेतब्यायं विहरति उत्तरेन सेतब्यं सिंसपावने। तं खो पन भवन्तं कुमारकस्सपं एवं कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गतो – ‘पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो चेव अरहा चा’ति [अरहा च (स्या॰ क॰)]। तमेते [तमेनं ते (सी॰ क॰), तमेनं (पी॰)] भवन्तं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमन्ती’’ति। ‘‘तेन हि, भो खत्ते, येन सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके एवं वदेहि – ‘पायासि, भो, राजञ्ञो एवमाह – आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासिपि राजञ्ञो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती’ति। पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके बाले अब्यत्ते सञ्ञापेति – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति। नत्थि हि, भो खत्ते, परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति। ‘‘एवं भो’’ति खो सो खत्ता पायासिस्स राजञ्ञस्स पटिस्सुत्वा येन सेतब्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा सेतब्यके ब्राह्मणगहपतिके एतदवोच – ‘‘पायासि, भो, राजञ्ञो एवमाह, आगमेन्तु किर भवन्तो, पायासिपि राजञ्ञो समणं कुमारकस्सपं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती’’ति।
४०९. अथ खो पायासि राजञ्ञो सेतब्यकेहि ब्राह्मणगहपतिकेहि परिवुतो येन सिंसपावनं येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता कुमारकस्सपेन सद्धिं सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। सेतब्यकापि खो ब्राह्मणगहपतिका अप्पेकच्चे आयस्मन्तं कुमारकस्सपं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु; अप्पेकच्चे आयस्मता कुमारकस्सपेन सद्धिं सम्मोदिंसु; सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। अप्पेकच्चे येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनञ्जलिं पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। अप्पेकच्चे नामगोत्तं सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। अप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्तं निसीदिंसु।
नत्थिकवादो
४१०. एकमन्तं निसिन्नो खो पायासि राजञ्ञो आयस्मन्तं कुमारकस्सपं एतदवोच – ‘‘अहञ्हि, भो कस्सप, एवंवादी एवंदिट्ठी – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘नाहं, राजञ्ञ, एवंवादिं एवंदिट्ठिं अद्दसं वा अस्सोसिं वा। कथञ्हि नाम एवं वदेय्य – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति?
चन्दिमसूरियउपमा
४११. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं ब्याकरेय्यासि। तं किं मञ्ञसि, राजञ्ञ, इमे चन्दिमसूरिया इमस्मिं वा लोके परस्मिं वा, देवा वा ते मनुस्सा वा’’ति? ‘‘इमे, भो कस्सप, चन्दिमसूरिया परस्मिं लोके, न इमस्मिं; देवा ते न मनुस्सा’’ति। ‘‘इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति।
४१२. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो, येन ते परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति? ‘‘अत्थि, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘यथा कथं विय, राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्झालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी। ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाळ्हगिलाना। यदाहं जानामि – ‘न दानिमे इमम्हा आबाधा वुट्ठहिस्सन्ती’ति त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि – ‘सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्ठिनो – ये ते पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्झालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ती’ति। भवन्तो खो पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्झालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी। सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सन्ति। सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्याथ, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका, यं भवन्तेहि दिट्ठं, यथा सामं दिट्ठं एवमेतं भविस्सती’ति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति, न पन दूतं पहिणन्ति। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
चोरउपमा
४१३. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं ब्याकरेय्यासि। तं किं मञ्ञसि, राजञ्ञ, इध ते पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेय्युं – ‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि, तं दण्डं पणेही’ति। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं दळ्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गाळ्हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा [कारेत्वा (स्या॰ क॰)] खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं [रथियाय रथियं (बहूसू)] सिङ्घाटकेन सिङ्घाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आघातने सीसं छिन्दथा’ति। ते ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं दळ्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गाळ्हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिङ्घाटकेन सिङ्घाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आघातने निसीदापेय्युं। लभेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेसु – ‘आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मिं मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा ञातिसालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा आगच्छामी’ति, उदाहु विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्यु’’न्ति? ‘‘न हि सो, भो कस्सप, चोरो लभेय्य चोरघातेसु – ‘आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता अमुकस्मिं मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा ञातिसालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा आगच्छामी’ति। अथ खो नं विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्यु’’न्ति। ‘‘सो हि नाम, राजञ्ञ, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेसु चोरघातेसु न लभिस्सति – ‘आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मिं मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा ञातिसालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा आगच्छामी’ति। किं पन ते मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्झालू ब्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी, ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना लभिस्सन्ति निरयपालेसु – ‘आगमेन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजञ्ञस्स गन्त्वा आरोचेम – ‘‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति? इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४१४. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो येन ते परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति? ‘‘अत्थि, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘यथा कथं विय, राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्झालू अब्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी। ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाळ्हगिलाना। यदाहं जानामि – ‘न दानिमे इमम्हा आबाधा वुट्ठहिस्सन्ती’ति त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि – ‘सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्ठिनो – ये ते पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्झालू अब्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्तीति। भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्झालू अब्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी। सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जिस्सन्ति। सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जेय्याथ, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका, यं भवन्तेहि दिट्ठं, यथा सामं दिट्ठं एवमेतं भविस्सती’ति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति, न पन दूतं पहिणन्ति। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
गूथकूपपुरिसउपमा
४१५. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे [उपमायपिधेकच्चे (सी॰ स्या॰), उपमायपिइधेकच्चे (पी॰)] विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, राजञ्ञ, पुरिसो गूथकूपे ससीसकं [ससीसको (स्या॰)] निमुग्गो अस्स। अथ त्वं पुरिसे आणापेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तं पुरिसं तम्हा गूथकूपा उद्धरथा’ति। ते ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं तम्हा गूथकूपा उद्धरेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स काया वेळुपेसिकाहि गूथं सुनिम्मज्जितं निम्मज्जथा’ति। ते ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तस्स पुरिसस्स काया वेळुपेसिकाहि गूथं सुनिम्मज्जितं निम्मज्जेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स कायं पण्डुमत्तिकाय तिक्खत्तुं सुब्बट्टितं उब्बट्टेथा’ति [सुप्पट्टितं उप्पट्टेथाति (क॰)]। ते तस्स पुरिसस्स कायं पण्डुमत्तिकाय तिक्खत्तुं सुब्बट्टितं उब्बट्टेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तं पुरिसं तेलेन अब्भञ्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्खत्तुं सुप्पधोतं करोथा’ति। ते तं पुरिसं तेलेन अब्भञ्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्खत्तुं सुप्पधोतं करेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्पेथा’ति। ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्पेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स महग्घञ्च मालं महग्घञ्च विलेपनं महग्घानि च वत्थानि उपहरथा’ति। ते तस्स पुरिसस्स महग्घञ्च मालं महग्घञ्च विलेपनं महग्घानि च वत्थानि उपहरेय्युं। ते त्वं एवं वदेय्यासि – ‘तेन हि, भो, तं पुरिसं पासादं आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि उपट्ठापेथा’ति। ते तं पुरिसं पासादं आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि उपट्ठापेय्युं।
‘‘तं किं मञ्ञसि, राजञ्ञ, अपि नु तस्स पुरिसस्स सुन्हातस्स सुविलित्तस्स सुकप्पितकेसमस्सुस्स आमुक्कमालाभरणस्स ओदातवत्थवसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्गीभूतस्स परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मिं गूथकूपे निमुज्जितुकामता [निमुज्जितुकाम्यता (स्या॰ क॰)] अस्सा’’ति? ‘‘नो हिदं, भो कस्सप’’। ‘‘तं किस्स हेतु’’? ‘‘असुचि, भो कस्सप, गूथकूपो असुचि चेव असुचिसङ्खातो च दुग्गन्धो च दुग्गन्धसङ्खातो च जेगुच्छो च जेगुच्छसङ्खातो च पटिकूलो च पटिकूलसङ्खातो चा’’ति। ‘‘एवमेव खो, राजञ्ञ, मनुस्सा देवानं असुची चेव असुचिसङ्खाता च, दुग्गन्धा च दुग्गन्धसङ्खाता च, जेगुच्छा च जेगुच्छसङ्खाता च, पटिकूला च पटिकूलसङ्खाता च। योजनसतं खो, राजञ्ञ, मनुस्सगन्धो देवे उब्बाधति। किं पन ते मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्झालू अब्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना ते आगन्त्वा आरोचेस्सन्ति – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति? इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४१६. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो …पे॰… ‘‘अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… ``यथा कथं विय, राजञ्ञाति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना पटिविरता, ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाळ्हगिलाना। यदाहं जानामि – ‘न दानिमे इमम्हा आबाधा वुट्ठहिस्सन्ती’ति त्याहं उपसङ्कमित्वा एवं वदामि – ‘सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्ठिनो – ये ते पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति देवानं तावतिंसानं सहब्यतन्ति। भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना पटिविरता। सचे तेसं भवतं समणब्राह्मणानं सच्चं वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जिस्सन्ति, देवानं तावतिंसानं सहब्यतं। सचे, भो, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जेय्याथ देवानं तावतिंसानं सहब्यतं, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ – `इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाकोति। भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका, यं भवन्तेहि दिट्ठं, यथा सामं दिट्ठं एवमेतं भविस्सतीति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति, न पन दूतं पहिणन्ति। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
तावतिंसदेवउपमा
४१७. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि; यथा ते खमेय्य, तथा नं ब्याकरेय्यासि। यं खो पन, राजञ्ञ, मानुस्सकं वस्ससतं, देवानं तावतिंसानं एसो एको रत्तिन्दिवो [रत्तिदिवो (क॰)], ताय रत्तिया तिंसरत्तियो मासो, तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिब्बं वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं आयुप्पमाणं। ये ते मित्तामच्चा ञातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिंसानं सहब्यतं। सचे पन तेसं एवं भविस्सति – ‘याव मयं द्वे वा तीणि वा रत्तिन्दिवा दिब्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता परिचारेम, अथ मयं पायासिस्स राजञ्ञस्स गन्त्वा आरोचेय्याम – ‘‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति। अपि नु ते आगन्त्वा आरोचेय्युं – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति? ‘‘नो हिदं, भो कस्सप। अपि हि मयं, भो कस्सप, चिरं कालङ्कतापि भवेय्याम। को पनेतं भोतो कस्सपस्स आरोचेति – ‘अत्थि देवा तावतिंसा’ति वा ‘एवंदीघायुका देवा तावतिंसा’ति वा। न मयं भोतो कस्सपस्स सद्दहाम – ‘अत्थि देवा तावतिंसा’ति वा ‘एवंदीघायुका देवा तावतिंसा’ति वा’’ति।
जच्चन्धउपमा
४१८. ‘‘सेय्यथापि, राजञ्ञ, जच्चन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्ह – सुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानि [मञ्जेट्ठकानि (स्या॰)] रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मञ्जिट्ठकानि रूपानि, न पस्सेय्य समविसमं, न पस्सेय्य तारकानि रूपानि, न पस्सेय्य चन्दिमसूरिये। सो एवं वदेय्य – ‘नत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, नत्थि कण्हसुक्कानं रूपानं दस्सावी। नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकानं रूपानं दस्सावी। नत्थि पीतकानि रूपानि, नत्थि पीतकानं रूपानं दस्सावी। नत्थि लोहितकानि रूपानि, नत्थि लोहितकानं रूपानं दस्सावी। नत्थि मञ्जिट्ठकानि रूपानि, नत्थि मञ्जिट्ठकानं रूपानं दस्सावी। नत्थि समविसमं, नत्थि समविसमस्स दस्सावी। नत्थि तारकानि रूपानि, नत्थि तारकानं रूपानं दस्सावी। नत्थि चन्दिमसूरिया, नत्थि चन्दिमसूरियानं दस्सावी। अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नत्थी’ति। सम्मा नु खो सो, राजञ्ञ, वदमानो वदेय्या’’ति? ‘‘नो हिदं, भो कस्सप। अत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, अत्थि कण्हसुक्कानं रूपानं दस्सावी। अत्थि नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलकानं रूपानं दस्सावी…पे॰… अत्थि समविसमं, अत्थि समविसमस्स दस्सावी। अत्थि तारकानि रूपानि, अत्थि तारकानं रूपानं दस्सावी। अत्थि चन्दिमसूरिया, अत्थि चन्दिमसूरियानं दस्सावी। ‘अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नत्थी’ति। न हि सो, भो कस्सप, सम्मा वदमानो वदेय्या’’ति। ‘‘एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, जच्चन्धूपमो मञ्ञे पटिभासि यं मं त्वं एवं वदेसि’’।
‘‘को पनेतं भोतो कस्सपस्स आरोचेति – ‘अत्थि देवा तावतिंसा’’ति वा, ‘एवंदीघायुका देवा तावतिंसा’ति वा? न मयं भोतो कस्सपस्स सद्दहाम – ‘अत्थि देवा तावतिंसा’ति वा ‘एवंदीघायुका देवा तावतिंसा’ति वा’’ति। ‘‘न खो, राजञ्ञ, एवं परो लोको दट्ठब्बो, यथा त्वं मञ्ञसि इमिना मंसचक्खुना। ये खो ते राजञ्ञ समणब्राह्मणा अरञ्ञवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता दिब्बचक्खुं विसोधेन्ति। ते दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन इमं चेव लोकं पस्सन्ति परञ्च सत्ते च ओपपातिके। एवञ्च खो, राजञ्ञ, परो लोको दट्ठब्बो; नत्वेव यथा त्वं मञ्ञसि इमिना मंसचक्खुना। इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४१९. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो…पे॰… अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… यथा कथं विय, राजञ्ञा’’ति? ‘‘इधाहं, भो कस्सप, पस्सामि समणब्राह्मणे सीलवन्ते कल्याणधम्मे जीवितुकामे अमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले। तस्स मय्हं, भो कस्सप, एवं होति – सचे खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा एवं जानेय्युं – ‘इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सती’ति। इदानिमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा विसं वा खादेय्युं, सत्थं वा आहरेय्युं, उब्बन्धित्वा वा कालङ्करेय्युं, पपाते वा पपतेय्युं। यस्मा च खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा न एवं जानन्ति – ‘इतो नो मतानं सेय्यो भविस्सती’ति, तस्मा इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामा अमरितुकामा सुखकामा दुक्खपटिकूला अत्तानं न मारेन्ति [( ) नत्थि (स्या॰ पी॰)]। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
गब्भिनीउपमा
४२०. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, अञ्ञतरस्स ब्राह्मणस्स द्वे पजापतियो अहेसुं। एकिस्सा पुत्तो अहोसि दसवस्सुद्देसिको वा द्वादसवस्सुद्देसिको वा, एका गब्भिनी उपविजञ्ञा। अथ खो सो ब्राह्मणो कालमकासि। अथ खो सो माणवको मातुसपत्तिं [मातुसपतिं (स्या॰)] एतदवोच – ‘यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा जातरूपं वा, सब्बं तं मय्हं; नत्थि तुय्हेत्थ किञ्चि। पितु मे [पितु मे सन्तको (स्या॰)] भोति, दायज्जं निय्यादेही’ति [नीय्यातेहीति (सी॰ पी॰)]। एवं वुत्ते सा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच – ‘आगमेहि ताव, तात, याव विजायामि। सचे कुमारको भविस्सति, तस्सपि एकदेसो भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति, सापि ते ओपभोग्गा [उपभोग्गा (स्या॰)] भविस्सती’ति। दुतियम्पि खो सो माणवको मातुसपत्तिं एतदवोच – ‘यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा जातरूपं वा, सब्बं तं मय्हं; नत्थि तुय्हेत्थ किञ्चि। पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यादेही’ति। दुतियम्पि खो सा ब्राह्मणी तं माणवकं एतदवोच – ‘आगमेहि ताव, तात, याव विजायामि। सचे कुमारको भविस्सति, तस्सपि एकदेसो भविस्सति; सचे कुमारिका भविस्सति सापि ते ओपभोग्गा [उपभोग्गा (स्या॰)] भविस्सती’ति। ततियम्पि खो सो माणवको मातुसपत्तिं एतदवोच – ‘यमिदं, भोति, धनं वा धञ्ञं वा रजतं वा जातरूपं वा, सब्बं तं मय्हं; नत्थि तुय्हेत्थ किञ्चि। पितु मे, भोति, दायज्जं निय्यादेही’ति।
‘‘अथ खो सा ब्राह्मणी सत्थं गहेत्वा ओवरकं पविसित्वा उदरं ओपादेसि [उप्पातेसि (स्या॰)] – ‘याव विजायामि यदि वा कुमारको यदि वा कुमारिका’ति। सा अत्तानं चेव जीवितञ्च गब्भञ्च सापतेय्यञ्च विनासेसि। यथा तं बाला अब्यत्ता अनयब्यसनं आपन्ना अयोनिसो दायज्जं गवेसन्ती, एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, बालो अब्यत्तो अनयब्यसनं आपज्जिस्ससि अयोनिसो परलोकं गवेसन्तो; सेय्यथापि सा ब्राह्मणी बाला अब्यत्ता अनयब्यसनं आपन्ना अयोनिसो दायज्जं गवेसन्ती। न खो, राजञ्ञ, समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा अपक्कं परिपाचेन्ति; अपि च परिपाकं आगमेन्ति। पण्डितानं अत्थो हि, राजञ्ञ, समणब्राह्मणानं सीलवन्तानं कल्याणधम्मानं जीवितेन। यथा यथा खो, राजञ्ञ, समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं तिट्ठन्ति, तथा तथा बहुं पुञ्ञं पसवन्ति, बहुजनहिताय च पटिपज्जन्ति बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४२१. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो…पे॰… अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… यथा कथं विय, राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेन्ति – ‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि, तं दण्डं पणेही’ति। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तंयेव कुम्भिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा अल्लेन चम्मेन ओनन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं [बहलविलेपनं (स्या॰ क॰)] करित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्गिं देथा’ति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तंयेव कुम्भिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा अल्लेन चम्मेन ओनन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं आरोपेत्वा अग्गिं देन्ति। यदा मयं जानाम ‘कालङ्कतो सो पुरिसो’ति, अथ नं कुम्भिं ओरोपेत्वा उब्भिन्दित्वा मुखं विवरित्वा सणिकं निल्लोकेम [विलोकेम (स्या॰)] – ‘अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा’ति। नेवस्स मयं जीवं निक्खमन्तं पस्साम। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
सुपिनकउपमा
४२२. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, तञ्ञेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं ब्याकरेय्यासि। अभिजानासि नो त्वं, राजञ्ञ, दिवा सेय्यं उपगतो सुपिनकं पस्सिता आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यक’’न्ति? ‘‘अभिजानामहं, भो कस्सप, दिवासेय्यं उपगतो सुपिनकं पस्सिता आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यक’’न्ति। ‘‘रक्खन्ति तं तम्हि समये खुज्जापि वामनकापि वेलासिकापि [चेलाविकापि (स्या॰), केळायिकापि (सी॰)] कोमारिकापी’’ति? ‘‘एवं, भो कस्सप, रक्खन्ति मं तम्हि समये खुज्जापि वामनकापि वेलासिकापि [चेलाविकापि (स्या॰), केळायिकापि (सी॰)] कोमारिकापी’’ति। ‘‘अपि नु ता तुय्हं जीवं पस्सन्ति पविसन्तं वा निक्खमन्तं वा’’ति? ‘‘नो हिदं, भो कस्सप’’। ‘‘ता हि नाम, राजञ्ञ, तुय्हं जीवन्तस्स जीवन्तियो जीवं न पस्सिस्सन्ति पविसन्तं वा निक्खमन्तं वा। किं पन त्वं कालङ्कतस्स जीवं पस्सिस्ससि पविसन्तं वा निक्खमन्तं वा। इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४२३. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो…पे॰… ‘‘अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… यथा कथं विय राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेन्ति – ‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि, तं दण्डं पणेही’ति। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तंयेव तुलाय तुलेत्वा जियाय अनस्सासकं मारेत्वा पुनदेव तुलाय तुलेथा’ति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तंयेव तुलाय तुलेत्वा जियाय अनस्सासकं मारेत्वा पुनदेव तुलाय तुलेन्ति। यदा सो जीवति, तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्मञ्ञतरो च। यदा पन सो कालङ्कतो होति तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो च अकम्मञ्ञतरो च। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
सन्तत्तअयोगुळउपमा
४२४. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, राजञ्ञ, पुरिसो दिवसं सन्तत्तं अयोगुळं आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं तुलाय तुलेय्य। तमेनं अपरेन समयेन सीतं निब्बुतं तुलाय तुलेय्य। कदा नु खो सो अयोगुळो लहुतरो वा होति मुदुतरो वा कम्मञ्ञतरो वा, यदा वा आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, यदा वा सीतो निब्बुतो’’ति? ‘‘यदा सो, भो कस्सप, अयोगुळो तेजोसहगतो च होति वायोसहगतो च आदित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्मञ्ञतरो च। यदा पन सो अयोगुळो नेव तेजोसहगतो होति न वायोसहगतो सीतो निब्बुतो, तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो च अकम्मञ्ञतरो चा’’ति। ‘‘एवमेव खो, राजञ्ञ, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो च विञ्ञाणसहगतो च, तदा लहुतरो च होति मुदुतरो च कम्मञ्ञतरो च। यदा पनायं कायो नेव आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्ञाणसहगतो तदा गरुतरो च होति पत्थिन्नतरो च अकम्मञ्ञतरो च। इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
४२५. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो…पे॰… अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… यथा कथं विय राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेन्ति – ‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि, तं दण्डं पणेही’ति। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं अनुपहच्च छविञ्च चम्मञ्च मंसञ्च न्हारुञ्च अट्ठिञ्च अट्ठिमिञ्जञ्च जीविता वोरोपेथ, अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा’ति। ते मे ‘साधू’ति पटिस्सुत्वा तं पुरिसं अनुपहच्च छविञ्च…पे॰… जीविता वोरोपेन्ति। यदा सो आमतो होति, त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं उत्तानं निपातेथ, अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा’ति। ते तं पुरिसं उत्तानं निपातेन्ति। नेवस्स मयं जीवं निक्खमन्तं पस्साम। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं अवकुज्जं निपातेथ… पस्सेन निपातेथ… दुतियेन पस्सेन निपातेथ… उद्धं ठपेथ… ओमुद्धकं ठपेथ… पाणिना आकोटेथ… लेड्डुना आकोटेथ… दण्डेन आकोटेथ… सत्थेन आकोटेथ… ओधुनाथ सन्धुनाथ निद्धुनाथ, अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा’ति। ते तं पुरिसं ओधुनन्ति सन्धुनन्ति निद्धुनन्ति। नेवस्स मयं जीवं निक्खमन्तं पस्साम। तस्स तदेव चक्खु होति ते रूपा, तञ्चायतनं नप्पटिसंवेदेति। तदेव सोतं होति ते सद्दा, तञ्चायतनं नप्पटिसंवेदेति। तदेव घानं होति ते गन्धा, तञ्चायतनं नप्पटिसंवेदेति। साव जिव्हा होति ते रसा, तञ्चायतनं नप्पटिसंवेदेति। स्वेव कायो होति ते फोट्ठब्बा, तञ्चायतनं नप्पटिसंवेदेति। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
सङ्खधमउपमा
४२६. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, अञ्ञतरो सङ्खधमो सङ्खं आदाय पच्चन्तिमं जनपदं अगमासि। सो येन अञ्ञतरो गामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मज्झे गामस्स ठितो तिक्खत्तुं सङ्खं उपलापेत्वा सङ्खं भूमियं निक्खिपित्वा एकमन्तं निसीदि। अथ खो, राजञ्ञ, तेसं पच्चन्तजनपदानं [पच्चन्तजानं (सी॰)] मनुस्सानं एतदहोसि – ‘अम्भो कस्स नु खो [एतदहोसि ‘‘किस्स दुखो (पी॰)] एसो सद्दो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो’ति। सन्निपतित्वा तं सङ्खधमं एतदवोचुं – ‘अम्भो, कस्स नु खो एसो सद्दो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो’ति। ‘एसो खो, भो, सङ्खो नाम यस्सेसो सद्दो एवंरजनीयो एवंकमनीयो एवंमदनीयो एवंबन्धनीयो एवंमुच्छनीयो’ति। ते तं सङ्खं उत्तानं निपातेसुं – ‘वदेहि, भो सङ्ख, वदेहि, भो सङ्खा’ति। नेव सो सङ्खो सद्दमकासि। ते तं सङ्खं अवकुज्जं निपातेसुं, पस्सेन निपातेसुं, दुतियेन पस्सेन निपातेसुं, उद्धं ठपेसुं, ओमुद्धकं ठपेसुं, पाणिना आकोटेसुं, लेड्डुना आकोटेसुं, दण्डेन आकोटेसुं, सत्थेन आकोटेसुं, ओधुनिंसु सन्धुनिंसु निद्धुनिंसु – ‘वदेहि, भो सङ्ख, वदेहि, भो सङ्खा’ति। नेव सो सङ्खो सद्दमकासि।
‘‘अथ खो, राजञ्ञ, तस्स सङ्खधमस्स एतदहोसि – ‘याव बाला इमे पच्चन्तजनपदामनुस्सा, कथञ्हि नाम अयोनिसो सङ्खसद्दं गवेसिस्सन्ती’ति। तेसं पेक्खमानानं सङ्खं गहेत्वा तिक्खत्तुं सङ्खं उपलापेत्वा सङ्खं आदाय पक्कामि। अथ खो, राजञ्ञ, तेसं पच्चन्तजनपदानं मनुस्सानं एतदहोसि – ‘यदा किर, भो, अयं सङ्खो नाम पुरिससहगतो च होति वायामसहगतो [वायोसहगतो (स्या॰)] च वायुसहगतो च, तदायं सङ्खो सद्दं करोति, यदा पनायं सङ्खो नेव पुरिससहगतो होति न वायामसहगतो न वायुसहगतो, नायं सङ्खो सद्दं करोती’ति। एवमेव खो, राजञ्ञ, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो च विञ्ञाणसहगतो च, तदा अभिक्कमतिपि पटिक्कमतिपि तिट्ठतिपि निसीदतिपि सेय्यम्पि कप्पेति, चक्खुनापि रूपं पस्सति, सोतेनपि सद्दं सुणाति, घानेनपि गन्धं घायति, जिव्हायपि रसं सायति, कायेनपि फोट्ठब्बं फुसति, मनसापि धम्मं विजानाति। यदा पनायं कायो नेव आयुसहगतो होति, न उस्मासहगतो, न विञ्ञाणसहगतो, तदा नेव अभिक्कमति न पटिक्कमति न तिट्ठति न निसीदति न सेय्यं कप्पेति, चक्खुनापि रूपं न पस्सति, सोतेनपि सद्दं न सुणाति, घानेनपि गन्धं न घायति, जिव्हायपि रसं न सायति, कायेनपि फोट्ठब्बं न फुसति, मनसापि धम्मं न विजानाति। इमिनापि खो ते, राजञ्ञ, परियायेन एवं होतु – ‘इतिपि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति [विपाकोति, पठमभाणवारं (स्या॰)]।
४२७. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति। ‘‘अत्थि पन, राजञ्ञ, परियायो…पे॰… अत्थि, भो कस्सप, परियायो…पे॰… यथा कथं विय राजञ्ञा’’ति? ‘‘इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा दस्सेन्ति – ‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि, तं दण्डं पणेही’ति। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ, अप्पेव नामस्स जीवं पस्सेय्यामा’ति। ते तस्स पुरिसस्स छविं छिन्दन्ति। नेवस्स मयं जीवं पस्साम। त्याहं एवं वदामि – ‘तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्मं छिन्दथ, मंसं छिन्दथ, न्हारुं छिन्दथ, अट्ठिं छिन्दथ, अट्ठिमिञ्जं छिन्दथ, अप्पेव नामस्स जीवं पस्सेय्यामा’ति। ते तस्स पुरिसस्स अट्ठिमिञ्जं छिन्दन्ति, नेवस्स मयं जीवं पस्सेय्याम। अयम्पि खो, भो कस्सप, परियायो, येन मे परियायेन एवं होति – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति।
अग्गिकजटिलउपमा
४२८. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, अञ्ञतरो अग्गिको जटिलो अरञ्ञायतने पण्णकुटिया सम्मति [वसति (सी॰ पी॰)]। अथ खो, राजञ्ञ, अञ्ञतरो जनपदे सत्थो [सत्थो जनपदपदेसा (सी॰), जनपदो सत्थवासो (स्या॰), जनपदपदेसो (पी॰)] वुट्ठासि। अथ खो सो सत्थो [सत्थवासो (स्या॰)] तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स अस्समस्स सामन्ता एकरत्तिं वसित्वा पक्कामि। अथ खो, राजञ्ञ, तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि – ‘यंनूनाहं येन सो सत्थवासो तेनुपसङ्कमेय्यं, अप्पेव नामेत्थ किञ्चि उपकरणं अधिगच्छेय्य’न्ति। अथ खो सो अग्गिको जटिलो कालस्सेव वुट्ठाय येन सो सत्थवासो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा अद्दस तस्मिं सत्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यकं छड्डितं। दिस्वानस्स एतदहोसि – ‘न खो मे तं पतिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो कालङ्करेय्य; यंनूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा आपादेय्यं पोसेय्यं वड्ढेय्य’न्ति। अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं अस्समं नेत्वा आपादेसि पोसेसि वड्ढेसि। यदा सो दारको दसवस्सुद्देसिको वा होति [अहोसि (?)] द्वादसवस्सुद्देसिको वा, अथ खो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे कञ्चिदेव करणीयं उप्पज्जि। अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं एतदवोच – ‘इच्छामहं, तात, जनपदं [नगरं (क॰)] गन्तुं; अग्गिं, तात, परिचरेय्यासि। मा च ते अग्गि निब्बायि। सचे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अयं वासी इमानि कट्ठानि इदं अरणिसहितं, अग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्यासी’ति। अथ खो सो अग्गिको जटिलो तं दारकं एवं अनुसासित्वा जनपदं अगमासि। तस्स खिड्डापसुतस्स अग्गि निब्बायि।
‘‘अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि – ‘पिता खो मं एवं अवच – ‘‘अग्गिं, तात, परिचरेय्यासि। मा च ते अग्गि निब्बायि। सचे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अयं वासी इमानि कट्ठानि इदं अरणिसहितं, अग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्यासी’’ति। यंनूनाहं अग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्य’न्ति। अथ खो सो दारको अरणिसहितं वासिया तच्छि – ‘अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्य’न्ति। नेव सो अग्गिं अधिगच्छि। अरणिसहितं द्विधा फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा [वीसतिधा (स्या॰)] फालेसि, सकलिकं सकलिकं अकासि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले कोट्टेसि, उदुक्खले कोट्टेत्वा महावाते ओपुनि [ओफुनि (स्या॰ क॰)] – ‘अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्य’न्ति। नेव सो अग्गिं अधिगच्छि।
‘‘अथ खो सो अग्गिको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं दारकं एतदवोच – ‘कच्चि ते, तात, अग्गि न निब्बुतो’ति? ‘इध मे, तात, खिड्डापसुतस्स अग्गि निब्बायि। तस्स मे एतदहोसि – ‘‘पिता खो मं एवं अवच अग्गिं, तात, परिचरेय्यासि। मा च ते, तात, अग्गि निब्बायि। सचे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अयं वासी इमानि कट्ठानि इदं अरणिसहितं, अग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्यासीति। यंनूनाहं अग्गिं निब्बत्तेत्वा अग्गिं परिचरेय्य’’न्ति। अथ ख्वाहं, तात, अरणिसहितं वासिया तच्छिं – ‘‘अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्य’’न्ति। नेवाहं अग्गिं अधिगच्छिं। अरणिसहितं द्विधा फालेसिं, तिधा फालेसिं, चतुधा फालेसिं, पञ्चधा फालेसिं, दसधा फालेसिं, सतधा फालेसिं, सकलिकं सकलिकं अकासिं, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले कोट्टेसिं, उदुक्खले कोट्टेत्वा महावाते ओपुनिं – ‘‘अप्पेव नाम अग्गिं अधिगच्छेय्य’’न्ति। नेवाहं अग्गिं अधिगच्छि’’’न्ति। अथ खो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स एतदहोसि – ‘याव बालो अयं दारको अब्यत्तो, कथञ्हि नाम अयोनिसो अग्गिं गवेसिस्सती’ति। तस्स पेक्खमानस्स अरणिसहितं गहेत्वा अग्गिं निब्बत्तेत्वा तं दारकं एतदवोच – ‘एवं खो, तात, अग्गि निब्बत्तेतब्बो। न त्वेव यथा त्वं बालो अब्यत्तो अयोनिसो अग्गिं गवेसी’ति। एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, बालो अब्यत्तो अयोनिसो परलोकं गवेसिस्ससि। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं, पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं, मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया’’ति।
४२९. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्कोमि इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितुं। राजापि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानोपि – ‘पायासि राजञ्ञो एवंवादी एवंदिट्ठी – ‘‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो – ‘याव बालो पायासि राजञ्ञो अब्यत्तो दुग्गहितगाही’ति। कोपेनपि नं हरिस्सामि, मक्खेनपि नं हरिस्सामि, पलासेनपि नं हरिस्सामी’’ति।
द्वे सत्थवाहउपमा
४३०. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, महासकटसत्थो सकटसहस्सं पुरत्थिमा जनपदा पच्छिमं जनपदं अगमासि। सो येन येन गच्छि, खिप्पंयेव परियादियति तिणकट्ठोदकं हरितकपण्णं। तस्मिं खो पन सत्थे द्वे सत्थवाहा अहेसुं एको पञ्चन्नं सकटसतानं, एको पञ्चन्नं सकटसतानं। अथ खो तेसं सत्थवाहानं एतदहोसि – ‘अयं खो महासकटसत्थो सकटसहस्सं; ते मयं येन येन गच्छाम, खिप्पमेव परियादियति तिणकट्ठोदकं हरितकपण्णं। यंनून मयं इमं सत्थं द्विधा विभजेय्याम – एकतो पञ्च सकटसतानि एकतो पञ्च सकटसतानी’ति। ते तं सत्थं द्विधा विभजिंसु [विभजेसुं (क॰)] एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्च सकटसतानि। एको सत्थवाहो बहुं तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च आरोपेत्वा सत्थं पयापेसि [पायापेसि (सी॰ पी॰)]। द्वीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो अद्दस पुरिसं काळं लोहितक्खं [लोहितक्खिं (स्या॰)] सन्नद्धकलापं [आसन्नद्धकलापं (स्या॰)] कुमुदमालिं अल्लवत्थं अल्लकेसं कद्दममक्खितेहि चक्केहि भद्रेन रथेन पटिपथं आगच्छन्तं’, दिस्वा एतदवोच – ‘कुतो, भो, आगच्छसी’ति? ‘अमुकम्हा जनपदा’ति। ‘कुहिं गमिस्ससी’ति? ‘अमुकं नाम जनपद’न्ति। ‘कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो’ति? ‘एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो, आसित्तोदकानि वटुमानि, बहु तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च। छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था’ति।
‘‘अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि – ‘अयं, भो, पुरिसो एवमाह – ‘‘पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो, आसित्तोदकानि वटुमानि, बहु तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च। छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था’’ति। छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सत्थं पयापेथा’ति। ‘एवं, भो’ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा छड्डेत्वा पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि लहुभारेहि सकटेहि सत्थं पयापेसुं। ते पठमेपि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा कट्ठं वा उदकं वा। दुतियेपि सत्थवासे… ततियेपि सत्थवासे… चतुत्थेपि सत्थवासे… पञ्चमेपि सत्थवासे… छट्ठेपि सत्थवासे… सत्तमेपि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा कट्ठं वा उदकं वा। सब्बेव अनयब्यसनं आपज्जिंसु। ये च तस्मिं सत्थे अहेसुं मनुस्सा वा पसू वा, सब्बे सो यक्खो अमनुस्सो भक्खेसि। अट्ठिकानेव सेसानि।
‘‘यदा अञ्ञासि दुतियो सत्थवाहो – ‘बहुनिक्खन्तो खो, भो, दानि सो सत्थो’ति बहुं तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च आरोपेत्वा सत्थं पयापेसि। द्वीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो अद्दस पुरिसं काळं लोहितक्खं सन्नद्धकलापं कुमुदमालिं अल्लवत्थं अल्लकेसं कद्दममक्खितेहि चक्केहि भद्रेन रथेन पटिपथं आगच्छन्तं, दिस्वा एतदवोच – ‘कुतो, भो, आगच्छसी’ति? ‘अमुकम्हा जनपदा’ति। ‘कुहिं गमिस्ससी’ति? ‘अमुकं नाम जनपद’न्ति। ‘कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो’ति? ‘एवं, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो। आसित्तोदकानि वटुमानि, बहु तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च। छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था’ति।
‘‘अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि – ‘अयं, भो, ‘‘पुरिसो एवमाह – पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो, आसित्तोदकानि वटुमानि, बहु तिणञ्च कट्ठञ्च उदकञ्च। छड्डेथ, भो, पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघं सीघं गच्छथ; मा योग्गानि किलमित्था’’ति। अयं भो पुरिसो नेव अम्हाकं मित्तो, न ञातिसालोहितो, कथं मयं इमस्स सद्धाय गमिस्साम। न वो छड्डेतब्बानि पुराणानि तिणानि कट्ठानि उदकानि, यथाभतेन भण्डेन सत्थं पयापेथ। न नो पुराणं छड्डेस्सामा’ति। ‘एवं, भो’ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यथाभतेन भण्डेन सत्थं पयापेसुं। ते पठमेपि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा कट्ठं वा उदकं वा। दुतियेपि सत्थवासे… ततियेपि सत्थवासे… चतुत्थेपि सत्थवासे… पञ्चमेपि सत्थवासे… छट्ठेपि सत्थवासे… सत्तमेपि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा कट्ठं वा उदकं वा। तञ्च सत्थं अद्दसंसु अनयब्यसनं आपन्नं। ये च तस्मिं सत्थेपि अहेसुं मनुस्सा वा पसू वा, तेसञ्च अट्ठिकानेव अद्दसंसु तेन यक्खेन अमनुस्सेन भक्खितानं।
‘‘अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि – ‘अयं खो, भो, सत्थो अनयब्यसनं आपन्नो, यथा तं तेन बालेन सत्थवाहेन परिणायकेन। तेन हि, भो, यानम्हाकं सत्थे अप्पसारानि पणियानि, तानि छड्डेत्वा, यानि इमस्मिं सत्थे महासारानि पणियानि, तानि आदियथा’ति। ‘एवं, भो’ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यानि सकस्मिं सत्थे अप्पसारानि पणियानि, तानि छड्डेत्वा यानि तस्मिं सत्थे महासारानि पणियानि, तानि आदियित्वा सोत्थिना तं कन्तारं नित्थरिंसु, यथा तं पण्डितेन सत्थवाहेन परिणायकेन। एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, बालो अब्यत्तो अनयब्यसनं आपज्जिस्ससि अयोनिसो परलोकं गवेसन्तो सेय्यथापि सो पुरिमो सत्थवाहो। येपि तव [ते (क॰)] सोतब्बं सद्धातब्बं [सद्दहातब्बं (पी॰ क॰)] मञ्ञिस्सन्ति, तेपि अनयब्यसनं आपज्जिस्सन्ति, सेय्यथापि ते सत्थिका। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया’’ति।
४३१. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्कोमि इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितुं। राजापि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानोपि – ‘पायासि राजञ्ञो एवंवादी एवंदिट्ठी – ‘‘इतिपि नत्थि परो लोको…पे॰… विपाको’’’ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो – ‘याव बालो पायासि राजञ्ञो, अब्यत्तो दुग्गहितगाही’ति। कोपेनपि नं हरिस्सामि, मक्खेनपि नं हरिस्सामि, पलासेनपि नं हरिस्सामी’’ति।
गूथभारिकउपमा
४३२. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि। उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, अञ्ञतरो सूकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा अञ्ञं गामं अगमासि। तत्थ अद्दस पहूतं सुक्खगूथं छड्डितं। दिस्वानस्स एतदहोसि – ‘अयं खो पहुतो सुक्खगूथो छड्डितो, मम च सूकरभत्तं [सूकरानं भक्खो (स्या॰)]; यंनूनाहं इतो सुक्खगूथं हरेय्य’न्ति। सो उत्तरासङ्गं पत्थरित्वा पहूतं सुक्खगूथं आकिरित्वा भण्डिकं बन्धित्वा सीसे उब्बाहेत्वा [उच्चारोपेत्वा (क॰ सी॰ क॰)] अगमासि। तस्स अन्तरामग्गे महाअकालमेघो पावस्सि। सो उग्घरन्तं पग्घरन्तं याव अग्गनखा गूथेन मक्खितो गूथभारं आदाय अगमासि। तमेनं मनुस्सा दिस्वा एवमाहंसु – ‘कच्चि नो त्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि विचेतो, कथञ्हि नाम उग्घरन्तं पग्घरन्तं याव अग्गनखा गूथेन मक्खितो गूथभारं हरिस्ससी’ति। ‘तुम्हे ख्वेत्थ, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता, तथा हि पन मे सूकरभत्त’न्ति। एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, गूथभारिकूपमो [गूथहारिकूपमो (सी॰ पी॰)] मञ्ञे पटिभासि। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया’’ति।
४३३. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्कोमि इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितुं। राजापि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानोपि – ‘पायासि राजञ्ञो एवंवादी एवंदिट्ठी – ‘‘इतिपि नत्थि परो लोको…पे॰… विपाको’’ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो – ‘याव बालो पायासि राजञ्ञो अब्यत्तो दुग्गहितगाही’ति। कोपेनपि नं हरिस्सामि, मक्खेनपि नं हरिस्सामि, पलासेनपि नं हरिस्सामी’’ति।
अक्खधुत्तकउपमा
४३४. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, द्वे अक्खधुत्ता अक्खेहि दिब्बिंसु। एको अक्खधुत्तो आगतागतं कलिं गिलति। अद्दसा खो दुतियो अक्खधुत्तो तं अक्खधुत्तं आगतागतं कलिं गिलन्तं, दिस्वा तं अक्खधुत्तं एतदवोच – ‘त्वं खो, सम्म, एकन्तिकेन जिनासि, देहि मे, सम्म, अक्खे पजोहिस्सामी’ति। ‘एवं सम्मा’ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स अक्खे पादासि। अथ खो सो अक्खधुत्तो अक्खे विसेन परिभावेत्वा तं अक्खधुत्तं एतदवोच – ‘एहि खो, सम्म, अक्खेहि दिब्बिस्सामा’ति। ‘एवं सम्मा’ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स पच्चस्सोसि। दुतियम्पि खो ते अक्खधुत्ता अक्खेहि दिब्बिंसु। दुतियम्पि खो सो अक्खधुत्तो आगतागतं कलिं गिलति। अद्दसा खो दुतियो अक्खधुत्तो तं अक्खधुत्तं दुतियम्पि आगतागतं कलिं गिलन्तं, दिस्वा तं अक्खधुत्तं एतदवोच –
‘‘लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्खं पुरिसो न बुज्झति।
गिल रे गिल पापधुत्तक [गिलि रे पापधुत्तक (क॰)], पच्छा ते कटुकं भविस्सतीति॥
‘‘एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, अक्खधुत्तकूपमो मञ्ञे पटिभासि। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया’’ति।
४३५. ‘‘किञ्चापि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सक्कोमि इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितुं। राजापि मं पसेनदि कोसलो जानाति तिरोराजानोपि – ‘पायासि राजञ्ञो एवंवादी एवंदिट्ठी – ‘‘इतिपि नत्थि परो लोको…पे॰… विपाको’’ति। सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो – ‘याव बालो पायासि राजञ्ञो अब्यत्तो दुग्गहितगाही’ति। कोपेनपि नं हरिस्सामि, मक्खेनपि नं हरिस्सामि, पलासेनपि नं हरिस्सामी’’ति।
साणभारिकउपमा
४३६. ‘‘तेन हि, राजञ्ञ, उपमं ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे विञ्ञू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति। भूतपुब्बं, राजञ्ञ, अञ्ञतरो जनपदो वुट्ठासि। अथ खो सहायको सहायकं आमन्तेसि – ‘आयाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपसङ्कमिस्साम, अप्पेव नामेत्थ किञ्चि धनं अधिगच्छेय्यामा’ति। ‘एवं सम्मा’ति खो सहायको सहायकस्स पच्चस्सोसि। ते येन सो जनपदो, येन अञ्ञतरं गामपट्टं [गामपज्जं (स्या॰), गामपत्तं (सी॰)] तेनुपसङ्कमिंसु, तत्थ अद्दसंसु पहूतं साणं छड्डितं, दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि – ‘इदं खो, सम्म, पहूतं साणं छड्डितं, तेन हि, सम्म, त्वञ्च साणभारं बन्ध, अहञ्च साणभारं बन्धिस्सामि, उभो साणभारं आदाय गमिस्सामा’ति। ‘एवं सम्मा’ति खो सहायको सहायकस्स पटिस्सुत्वा साणभारं बन्धित्वा ते उभो साणभारं आदाय येन अञ्ञतरं गामपट्टं तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ अद्दसंसु पहूतं साणसुत्तं छड्डितं, दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि – ‘यस्स खो, सम्म, अत्थाय इच्छेय्याम साणं, इदं पहूतं साणसुत्तं छड्डितं। तेन हि, सम्म, त्वञ्च साणभारं छड्डेहि, अहञ्च साणभारं छड्डेस्सामि, उभो साणसुत्तभारं आदाय गमिस्सामा’ति। ‘अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च, अलं मे त्वं पजानाही’ति। अथ खो सो सहायको साणभारं छड्डेत्वा साणसुत्तभारं आदियि।
‘‘ते येन अञ्ञतरं गामपट्टं तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ अद्दसंसु पहूता साणियो छड्डिता, दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि – ‘यस्स खो, सम्म, अत्थाय इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा, इमा पहूता साणियो छड्डिता। तेन हि, सम्म, त्वञ्च साणभारं छड्डेहि, अहञ्च साणसुत्तभारं छड्डेस्सामि, उभो साणिभारं आदाय गमिस्सामा’ति। ‘अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च, अलं मे, त्वं पजानाही’ति। अथ खो सो सहायको साणसुत्तभारं छड्डेत्वा साणिभारं आदियि।
‘‘ते येन अञ्ञतरं गामपट्टं तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ अद्दसंसु पहूतं खोमं छड्डितं, दिस्वा…पे॰… पहूतं खोमसुत्तं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं खोमदुस्सं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं कप्पासं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं कप्पासिकसुत्तं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं कप्पासिकदुस्सं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं अयं [अयसं (स्या॰)] छड्डितं, दिस्वा… पहूतं लोहं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं तिपुं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं सीसं छड्डितं, दिस्वा… पहूतं सज्झं [सज्झुं (सी॰ स्या॰ पी॰)] छड्डितं, दिस्वा… पहूतं सुवण्णं छड्डितं, दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि – ‘यस्स खो, सम्म, अत्थाय इच्छेय्याम साणं वा साणसुत्तं वा साणियो वा खोमं वा खोमसुत्तं वा खोमदुस्सं वा कप्पासं वा कप्पासिकसुत्तं वा कप्पासिकदुस्सं वा अयं वा लोहं वा तिपुं वा सीसं वा सज्झं वा, इदं पहूतं सुवण्णं छड्डितं। तेन हि, सम्म, त्वञ्च साणभारं छड्डेहि, अहञ्च सज्झभारं [सज्झुभारं (सी॰ स्या॰ पी॰)] छड्डेस्सामि, उभो सुवण्णभारं आदाय गमिस्सामा’ति। ‘अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च, अलं मे त्वं पजानाही’ति। अथ खो सो सहायको सज्झभारं छड्डेत्वा सुवण्णभारं आदियि।
‘‘ते येन सको गामो तेनुपसङ्कमिंसु। तत्थ यो सो सहायको साणभारं आदाय अगमासि, तस्स नेव मातापितरो अभिनन्दिंसु, न पुत्तदारा अभिनन्दिंसु, न मित्तामच्चा अभिनन्दिंसु, न च ततोनिदानं सुखं सोमनस्सं अधिगच्छि। यो पन सो सहायको सुवण्णभारं आदाय अगमासि, तस्स मातापितरोपि अभिनन्दिंसु, पुत्तदारापि अभिनन्दिंसु, मित्तामच्चापि अभिनन्दिंसु, ततोनिदानञ्च सुखं सोमनस्सं अधिगच्छि। ‘‘एवमेव खो त्वं, राजञ्ञ, साणभारिकूपमो मञ्ञे पटिभासि। पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ञ, पापकं दिट्ठिगतं। मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया’’ति।
सरणगमनं
४३७. ‘‘पुरिमेनेव अहं ओपम्मेन भोतो कस्सपस्स अत्तमनो अभिरद्धो। अपि चाहं इमानि विचित्रानि पञ्हापटिभानानि सोतुकामो एवाहं भवन्तं कस्सपं पच्चनीकं कातब्बं अमञ्ञिस्सं। अभिक्कन्तं, भो कस्सप, अभिक्कन्तं, भो कस्सप। सेय्यथापि, भो कस्सप, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूळ्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य ‘चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती’ति एवमेवं भोता कस्सपेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भो कस्सप, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि, धम्मञ्च, भिक्खुसङ्घञ्च। उपासकं मं भवं कस्सपो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं।
‘‘इच्छामि चाहं, भो कस्सप, महायञ्ञं यजितुं, अनुसासतु मं भवं कस्सपो, यं ममस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया’’ति।
यञ्ञकथा
४३८. ‘‘यथारूपे खो, राजञ्ञ, यञ्ञे गावो वा हञ्ञन्ति अजेळका वा हञ्ञन्ति, कुक्कुटसूकरा वा हञ्ञन्ति, विविधा वा पाणा संघातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिट्ठी मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ञ, यञ्ञो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो। सेय्यथापि, राजञ्ञ, कस्सको बीजनङ्गलं आदाय वनं पविसेय्य। सो तत्थ दुक्खेत्ते दुब्भूमे अविहतखाणुकण्टके बीजानि पतिट्ठापेय्य खण्डानि पूतीनि वातातपहतानि असारदानि असुखसयितानि। देवो च न कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य। अपि नु तानि बीजानि वुद्धिं विरूळ्हिं [विरुळ्हिं (मोग्गलाने)] वेपुल्लं आपज्जेय्युं, कस्सको वा विपुलं फलं अधिगच्छेय्या’’ति? ‘‘नो हिदं [न एवं (स्या॰ क॰)] भो कस्सप’’। ‘‘एवमेव खो, राजञ्ञ, यथारूपे यञ्ञे गावो वा हञ्ञन्ति, अजेळका वा हञ्ञन्ति, कुक्कुटसूकरा वा हञ्ञन्ति, विविधा वा पाणा संघातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिट्ठी मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ञ, यञ्ञो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो।
‘‘यथारूपे च खो, राजञ्ञ, यञ्ञे नेव गावो हञ्ञन्ति, न अजेळका हञ्ञन्ति, न कुक्कुटसूकरा हञ्ञन्ति, न विविधा वा पाणा संघातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति सम्मादिट्ठी सम्मासङ्कप्पा सम्मावाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ञ, यञ्ञो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो। सेय्यथापि, राजञ्ञ, कस्सको बीजनङ्गलं आदाय वनं पविसेय्य। सो तत्थ सुखेत्ते सुभूमे सुविहतखाणुकण्टके बीजानि पतिट्ठपेय्य अखण्डानि अपूतीनि अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि। देवो च कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य। अपि नु तानि बीजानि वुद्धिं विरूळ्हिं वेपुल्लं आपज्जेय्युं, कस्सको वा विपुलं फलं अधिगच्छेय्या’’ति? ‘‘एवं, भो कस्सप’’। ‘‘एवमेव खो, राजञ्ञ, यथारूपे यञ्ञे नेव गावो हञ्ञन्ति, न अजेळका हञ्ञन्ति, न कुक्कुटसूकरा हञ्ञन्ति, न विविधा वा पाणा संघातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति सम्मादिट्ठी सम्मासङ्कप्पा सम्मावाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ञ, यञ्ञो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो’’ति।
उत्तरमाणववत्थु
४३९. अथ खो पायासि राजञ्ञो दानं पट्ठपेसि समणब्राह्मणकपणद्धिकवणिब्बकयाचकानं। तस्मिं खो पन दाने एवरूपं भोजनं दीयति कणाजकं बिलङ्गदुतियं, धोरकानि [थोरकानि (सी॰ पी॰), चोरकानि (स्या॰)] च वत्थानि गुळवालकानि [गुळगाळकानि (क॰)]। तस्मिं खो पन दाने उत्तरो नाम माणवो वावटो [ब्यावटो (सी॰ पी॰)] अहोसि। सो दानं दत्वा एवं अनुद्दिसति – ‘‘इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्ञमेव इमस्मिं लोके समागच्छिं, मा परस्मि’’न्ति। अस्सोसि खो पायासि राजञ्ञो – ‘‘उत्तरो किर माणवो दानं दत्वा एवं अनुद्दिसति – ‘इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्ञमेव इमस्मिं लोके समागच्छिं, मा परस्मि’’’न्ति। अथ खो पायासि राजञ्ञो उत्तरं माणवं आमन्तापेत्वा एतदवोच – ‘‘सच्चं किर त्वं, तात उत्तर, दानं दत्वा एवं अनुद्दिससि – ‘इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्ञमेव इमस्मिं लोके समागच्छिं, मा परस्मि’’’न्ति? ‘‘एवं, भो’’। ‘‘किस्स पन त्वं, तात उत्तर, दानं दत्वा एवं अनुद्दिससि – ‘इमिनाहं दानेन पायासिं राजञ्ञमेव इमस्मिं लोके समागच्छिं, मा परस्मि’न्ति? ननु मयं, तात उत्तर, पुञ्ञत्थिका दानस्सेव फलं पाटिकङ्खिनो’’ति? ‘‘भोतो खो दाने एवरूपं भोजनं दीयति कणाजकं बिलङ्गदुतियं, यं भवं पादापि [पादासि (क॰)] न इच्छेय्य सम्फुसितुं [छुपितुं (पी॰ क॰)], कुतो भुञ्जितुं, धोरकानि च वत्थानि गुळवालकानि, यानि भवं पादापि [अचित्तिकतं (क॰)] न इच्छेय्य सम्फुसितुं, कुतो परिदहितुं। भवं खो पनम्हाकं पियो मनापो, कथं मयं मनापं अमनापेन संयोजेमा’’ति? ‘‘तेन हि त्वं, तात उत्तर, यादिसाहं भोजनं भुञ्जामि, तादिसं भोजनं पट्ठपेहि। यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि, तादिसानि च वत्थानि पट्ठपेही’’ति। ‘‘एवं, भो’’ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स राजञ्ञस्स पटिस्सुत्वा यादिसं भोजनं पायासि राजञ्ञो भुञ्जति, तादिसं भोजनं पट्ठपेसि। यादिसानि च वत्थानि पायासि राजञ्ञो परिदहति, तादिसानि च वत्थानि पट्ठपेसि।
४४०. अथ खो पायासि राजञ्ञो असक्कच्चं दानं दत्वा असहत्था दानं दत्वा अचित्तीकतं दानं दत्वा अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जि सुञ्ञं सेरीसकं विमानं। यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो। सो सक्कच्चं दानं दत्वा सहत्था दानं दत्वा चित्तीकतं दानं दत्वा अनपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जि देवानं तावतिंसानं सहब्यतं।
पायासिदेवपुत्तो
४४१. तेन खो पन समयेन आयस्मा गवम्पति अभिक्खणं सुञ्ञं सेरीसकं विमानं दिवाविहारं गच्छति। अथ खो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा गवम्पति तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं गवम्पतिं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि। एकमन्तं ठितं खो पायासिं देवपुत्तं आयस्मा गवम्पति एतदवोच – ‘‘कोसि त्वं, आवुसो’’ति? ‘‘अहं, भन्ते, पायासि राजञ्ञो’’ति। ‘‘ननु त्वं, आवुसो, एवंदिट्ठिको अहोसि – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’’’ति? ‘‘सच्चाहं, भन्ते, एवंदिट्ठिको अहोसिं – ‘इतिपि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको’ति। अपि चाहं अय्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिट्ठिगता विवेचितो’’ति। ‘‘यो पन ते, आवुसो, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो, सो कुहिं उपपन्नो’’ति? ‘‘यो मे, भन्ते, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो, सो सक्कच्चं दानं दत्वा सहत्था दानं दत्वा चित्तीकतं दानं दत्वा अनपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यतं। अहं पन, भन्ते, असक्कच्चं दानं दत्वा असहत्था दानं दत्वा अचित्तीकतं दानं दत्वा अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुञ्ञं सेरीसकं विमानं। तेन हि, भन्ते गवम्पति, मनुस्सलोकं गन्त्वा एवमारोचेहि – ‘सक्कच्चं दानं देथ, सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, अनपविद्धं दानं देथ। पायासि राजञ्ञो असक्कच्चं दानं दत्वा असहत्था दानं दत्वा अचित्तीकतं दानं दत्वा अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुञ्ञं सेरीसकं विमानं। यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो, सो सक्कच्चं दानं दत्वा सहत्था दानं दत्वा चित्तीकतं दानं दत्वा अनपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यत’’’न्ति।
अथ खो आयस्मा गवम्पति मनुस्सलोकं आगन्त्वा एवमारोचेसि – ‘‘सक्कच्चं दानं देथ, सहत्था दानं देथ, चित्तीकतं दानं देथ, अनपविद्धं दानं देथ। पायासि राजञ्ञो असक्कच्चं दानं दत्वा असहत्था दानं दत्वा अचित्तीकतं दानं दत्वा अपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपन्नो सुञ्ञं सेरीसकं विमानं। यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो, सो सक्कच्चं दानं दत्वा सहत्था दानं दत्वा चित्तीकतं दानं दत्वा अनपविद्धं दानं दत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्नो देवानं तावतिंसानं सहब्यत’’न्ति।
पायासिसुत्तं निट्ठितं दसमं।
महावग्गो निट्ठितो।
तस्सुद्दानं –
महापदान निदानं, निब्बानञ्च सुदस्सनं।
जनवसभ गोविन्दं, समयं सक्कपञ्हकं।
महासतिपट्ठानञ्च, पायासि दसमं भवे [सतिपट्ठानपायासि, महावग्गस्स सङ्गहो (सी॰ पी॰) सतिपट्ठानपायासि, महावग्गोति वुच्चतीति (स्या॰)]॥
महावग्गपाळि निट्ठिता।